ईलोक चौपाल(मधुमती, अक्टूबर-2017 में प्रकाशित)
डॉ. राजेन्द्र कुमार सिंघवी
गतांक से आगे....
प्रख्यात कवि एवं आलोचक विजेन्द्र ने कला और साहित्य की दृष्टि को रेखांकित करते हुए लिखा कि हमें कला-साहित्य की समृद्ध विरासत को, उनकी उत्कृष्ट परम्पराओं को आत्मसात कर लेना चाहिए। एक लेखक के रूप में हमारा उद्देश्य अपनी विशाल संघर्षशील लोक की सेवा ही होना चाहिए। लोक में कौन शामिल हैं? इसमें मजदूर, किसान, दलित, आदिवासी, सैनिक और निम्न-मध्यवर्ग तक को शामिल किया जा सकता है। ये वे वर्ग हैं जो अपने श्रम से अपने समाज के लिए उत्पादन करते हैं और समाज का निर्माण करते हैं। कविता के साकार रूप की कल्पना करते हुए अनिल पाण्डेय का मंतव्य है कि कविता में बहुत कुछ छुटकर बिखर जाने की यातना लिए एकदम से स्पष्ट कर देने की प्रतिबद्धता और बहुत कुछ को बदल देने की जिद बहुत कम कवि ही रख पाए हैं। यह उन्हीं कवियों में वर्तमान रह सका है जो तिकडमी बाज नहीं है, तुनक मिजाज नहीं है। जो बाहर हैं, अन्दर भी वही हैं। कवि-हृदय में उठ रही दुनिया सही अर्थो में ऐसे कवियों के माध्यम से ही साकार रूप ले पाती है।
हिन्दी की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए बनारस से आशीष त्रिपाठी लिखते हैं- आज हिंदी भूमंडलीकरण की भाषा है। बाजार मनोरंजन, उद्योग और विज्ञापनों की भाषा। पतंजलि जैसे तेजी से बढते व्यापारिक समूह की भाषा। इस सबके पीछे भी अंततः निर्विकल्प एकभाषी हिन्दी जनों को संबोधित करने की व्यापारिक मजबूरियाँ प्रमुख हैं।... हिन्दी दिवस स्थापना करने का दिन नहीं है, एक रचनात्मक संकल्प लेने का दिन है कि हिन्दी भाषी अपनी भाषा और बोलियों से प्यार करे। उसमें हो रहे साहित्य-सृजन और ज्ञान-रचना को आगे बढाएँ।... हिन्दी यानी भाषाओं का संयुक्त परिवार। कोई एक रूप नहीं। अनेक रूप।
<br/>उज्जैन से प्रो. शैलेन्द्र कुमार शर्मा का विचार है कि स्वभाषा के स्थान पर अंग्रेजी हमारी शिक्षा-व्यवस्था की प्रमुख भाषा बनती जा रही है। एक बहुत बडे भ्रम के रूप में अंग्रेजी का ज्ञान शिक्षित और सफल होने का पर्याय माना जा रहा है। सदियों से हमारी संवेदना संस्कृति और ज्ञान-विज्ञान का संवहन करती आ रही भारतीय भाषाओं की निरन्तर उपेक्षा हो रही है। देश के मध्य भाग में हिन्दी के साथ ही व्यापक लोक समुदाय में प्रयुक्त मालवी, निमाडी, बुंदेली, बघेली, छत्तीसगढी तथा जनजातीय क्षेत्रों में प्रचलित भीली, भिलाली, बारेली, सहरिया, गोंडी, वैगा, कोरकू, मुरिया, हल्बी, मुंडा, उरांव जैसी कई मातृभाषाएँ हमारी भाषायी सामर्थ्य के प्रमाण हैं।
केन्द्रीय हिन्दी संस्थान के विदेशी छात्रों को हिन्दी सिखाने वाले एक वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम में ‘गोदान’ के स्थान पर ‘निर्मला’ रखने का मुद्दा ई लोक पर चर्चित रहा। हस्तक्षेप करते हुए बनारस से अमरेन्द्र त्रिपाठी लिखते हैं कि पूरे विवाद में यह बात सिरे से गायब थी कि विदेशी विद्यार्थियों की भाषा संबंधी मुश्किल को ध्यान में रखते हुए ‘गोदान’ की जगह ‘निर्मला’ रखा गया। गोयनका जी की ख्याति प्रेमचंद के विशेषज्ञ के रूप में है, उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश प्रेमचंद साहित्य के विषय में अनुसंधान पर होम किया है। उनके उपाध्यक्ष रहते प्रेमचंद को पाठ्यक्रम से हटा देने की खबर पर कम-से-कम हिन्दी जगत के विद्वानों को तो सहज भरोसा नहीं ही करना चाहिए था।
फतहपुर उ.प्र. से अनूप शुक्ल ने साहित्य के राजधानी केन्द्रित होने का प्रश्न उठाते हुए लिखा कि साहित्य इतना केन्द्रीकृत पहले कभी नहीं था, जितना आज है... आदिकाल और भक्तिकाल के कवि बिखरे हुए थे। उनका बिखराव भौगोलिक भी था और वस्तुगत व भाषागत भी था। उनमें समानता के कुछ बिन्दु भले खोज लिए जाएँ, लेकिन उनके साहित्य में पर्याप्त विविधता थी। संचारहीनता के उस युग में अपनी भौगोलिक विकेन्द्रीयता और भाषागत विविधता के चलते उन्होंने बहुत बडे जनसमुदाय को प्रभावित किया और रचनाओं के माध्यम से अपनी बात लोगों तक पहुँचाने में सफलता प्राप्त की।... दिल्ली के साहित्यिक, सांस्कृतिक की विकेन्द्रीयता पर ही असर नही पडा, बल्कि कहीं न कहीं साहित्य और भाषा की विविधता भी प्रभावित हुई। पहले जो लेखक रचना में अपनी भाषा और अभिव्यक्ति के निजीपन से पहचाने जाते थे, उनमें से अधिकांश भाषा और अभिव्यक्ति के सामान्यीकरण और समानीकरण के शिकार हो गए।... इससे साहित्य की समृद्धि बही या उसका नुकसान हुआ, यह आकलन का विषय है; लेकिन यह जरूर देखा जाना चाहिए कि साहित्य के लोक से कटते जाने, साहित्य के साहित्य पाठकों के कम होते जाने और लेखकों के ही साहित्य का पाठक रह जाने के पीछे साहित्य की इस केन्द्रीयता की कोई भूमिका है या नहीं?
दिल्ली से दिविक रमेश ने हिन्दी में आलोचना की वर्तमान स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा- ‘‘क्या आज हिन्दी में आलोचना है? क्या आलोचना का समय लद गया? क्या आलोचना की जरूरत अब नहीं रही? क्या पाठ ही सर्वोपरि है? दलित, नारी, आदिवासी, प्रवासी आदि से सम्बद्ध साहित्य-विमर्श क्या आलोचना के विकल्प हैं?... आज तो लगने यह भी लगा है कि आलोचना की कोई केन्द्रीय अवधारणा मानो बची ही नहीं है। बहुत-सी अवधारणाएँ एक दूसरे से गुत्थम गुत्था हों रही है। बहस के रूप में चुनौती तो केन्द्रीय साहित्य होने की अवधारणा को भी मिल रही है। धुमका (झारखंड) से सुशील कुमार ने रचनाकारों की महत्वाकांक्षाओं पर टिप्पणी करते हुए लिखा कि लेखक, कवि कलाकार- सबके सब महत्वाकांक्षी होते हैं। वे दुखियों को दुःख नहीं बाँटते, केवल अपनी शौक और शगल को पूरा करते हैं। इसलिए इनसे समाज की तस्वीर नहीं बदलती, न जनता में कोई युगबोध जन्म लेता है।
साहित्य के नोबेल सम्मान जापानी मूल के ब्रिटिश लेखक काजुओ इशिगुरो को उनके उपन्यास ‘द रिमेंस ऑफ द डे’ के लिए दिए जाने पर सवाई सिंह शेखावत ने स्वीडिश अकादमी के सचिव सारा डेनियस की टिप्पणी साझा की है- ‘‘आप जेन ऑस्टिन और फ्रेंज काफ्ता को मिला दें तो संक्षेप में इशिगुरो को पा सकते हैं, लेकिन उन्हें ठीक से पाने के लिए आपको थोडा-सा प्रॉउस्ट को भी मिलाना पडेगा उसके बाद ज्यादा न हिलाएँ तो आप उनके लेखन को पा सकते हैं- स्मृति, समय और आत्म-विमोहा इशिगुरो के लिए जीवन के खुरदरे यथार्थ के बरक्ए जीवन से जुडी वे मानवीय अनुभूतियाँ अधिक वरेण्य हैं, जो हर तरह की विपरीत जीवन स्थितियों में भी जीने का सरंजाम जुटाती है।
ब्लू-व्हेल जैसे खेलों से अबोध बचपन किस प्रकार अवसाद का शिकार हो रहा है? उसे इन्दौर से सुशोभित शक्तावत ने ‘चाचा चौधरी’ जैसे पात्र से तुलना करते हुए लिखा है कि भूमंडलीकरण की कुशाग्रताओं के साथ ढाई दशक में ‘अढाई कोस’ चलने के बाद अंततः शायद हमें समझ आएं कि ‘चाचा चौधरी’ उस कम्प्यूटर से अधिक मेधावी नहीं हो सकते थे, जो युद्धों को एक खेल में तब्दील कर सकता है और आत्मनाश को नीली मछलियों के भुलावों में। फिर भी जिंदगी के कई पहलू ऐसे होते हैं, जिनमें वक्त से पिछड जाना ही बेहतर होता है और यह बात इतनी साफ-सरल है कि ‘साबू’ भी इसे बडी आसानी से समझ सकता है, जिसकी अकल उसके घुटनों में बसती थी।
मथुरा से राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय की विश्वात्मकता का आधार निरूपित करते हुए लिखा है कि अध्ययन-मनन-चिंतन छोटे-छोटे दायरों से बंधा नहीं होता। संकीर्ण नहीं होता है। वहाँ कोई सीमा नहीं होती। स्वदेशो भुवनत्रयं। वह चिन्तक आकाश की भाँति उन्मुक्त होता है! बन्धन नहीं होता। वह किसी के शासन में रहकर चिंतन कर ही नहीं सकता। जैसे कवि के मनोभूमि को मधुमयी भूमिका कहा जाता है, वैसा ही चिंतक के संबंध में कहा जा सकता है। सच तो यह है कि स्वतंत्र चिंतन समाधि जैसी अवस्था में होता है, जिसमें न मैं का अस्तित्व होता है न मेरे जोधपुर से नरेन्द्र मिश्र ने लिखा है कि भारत में गुवाहाटी विश्वविद्यालय एक मात्र संस्थान है, जहाँ हिन्दी का शोधपत्र अंग्रेजी में अनूदित करवाकर पढना पडता है। ऐसी स्थिति में राष्ट्रभाषा का क्या सम्मान रह जाता है? ऐसी घटनाओं के लिए अब हिन्दी-प्रेमियों को संकल्प की आवश्यकता है।
Powered by : Avid Web Solutions
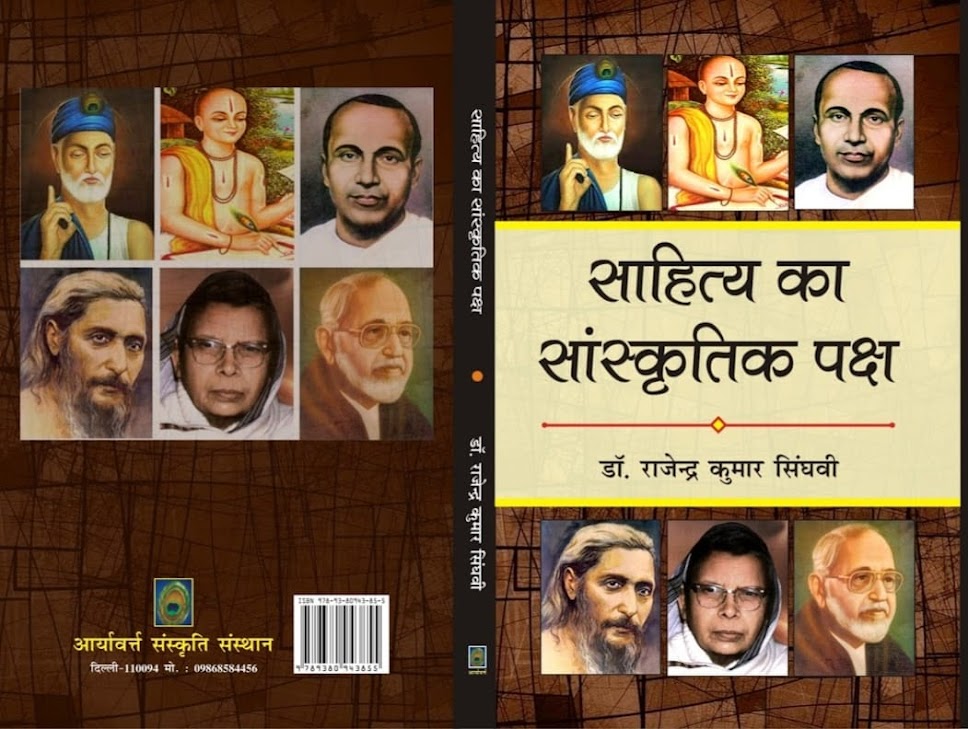
No comments:
Post a Comment