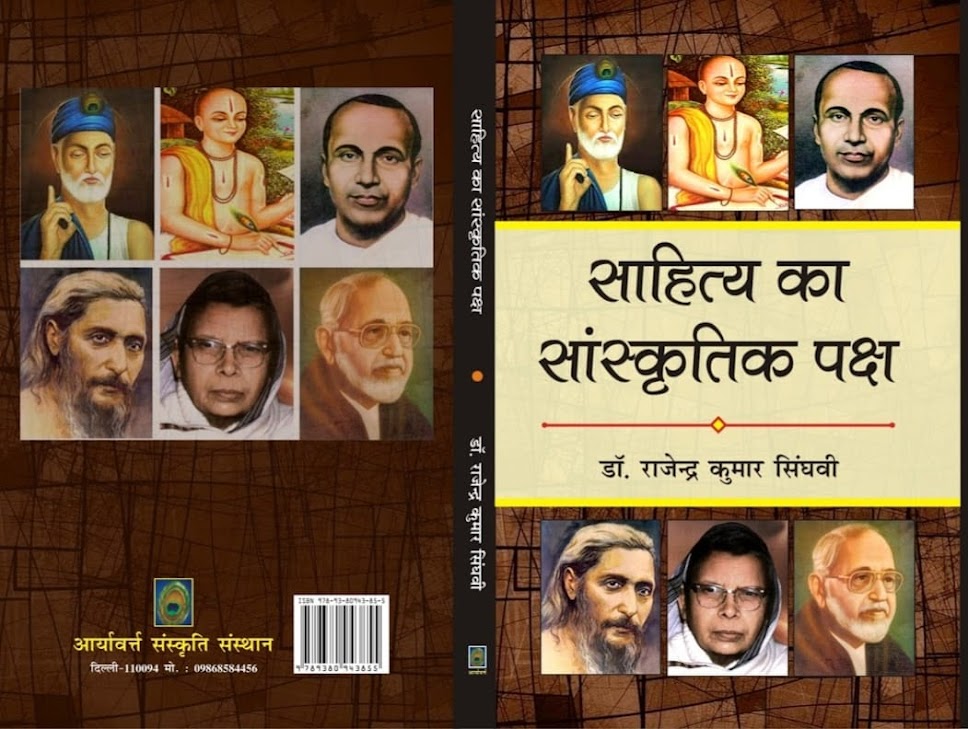राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता में साहित्य की भूमिका
साहित्य-अर्चना, स्मारिका-२०२५ में प्रकाशित
राष्ट्र एक जीवन्त, जाग्रत इकाई है। राष्ट्र स्वयंभू है, सृष्टि की रचना ही इस बात का निर्धारण करती है कि किस राष्ट्र का सृजन, अभ्युदय, पतन अथवा पुनरूत्थान हो, क्योंकि राष्ट्र का भी जीवनोद्देश्य होता है। अतः प्रत्येक राष्ट्र में अस्तित्व बोध होना सहज स्वाभाविक है। राष्ट्र केवल पर्वत-नदी या समतल भूमि नहीं होता, बल्कि उस भूमिखंड में निवास तथा विकास करने वाले मानव-समूह का जीवन अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहता है। राष्ट्र और उसकी संस्कृति मिलकर समूचे विश्व में अपनी पहचान स्थापित करते हैं। राष्ट्र का निजत्व होता है, गुणधर्म होता है, उसकी पहचान, आकृति, अस्मिता और भूगोल होता है। यजुर्वेद में कहा गया कि हम राष्ट्र के पुरोहित हैं। हम भोग में भी त्याग के समान आचरण करते हैं। विश्व के सभी प्राणी सुखी हों, ऐसी उदात्त भावना है। भारतीय संस्कृति अखिल विश्व के समस्त संस्कारों, परम्पराओं, सभ्यता के विभिन्न तत्त्वों, लौकिक, आध्यात्मिक एवं धार्मिक मान्यताओं को समाविष्ट किए हुए हैं। इसलिए मनीषियों ने इसे ‘सा प्रथमा संस्कृति विश्वधारा’ के रूप में बोधित किया है। इसी सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय मनीषा ने राष्ट्र को भी परिभाषित किया है।
विश्व साहित्य की प्रथम पुस्तक, जिसे यूनेस्को ने भी स्वीकार किया है, वह है- ऋग्वेद। उसमें कहा गया है- मनुर्भवः, अर्थात् मनुष्य बनो। मनुष्यता का बोध ही भारतीय संस्कृति का मूल है, जो वर्तमान और भविष्य के लिए भी जरूरी है व रहेगी। हमें यह समझना होगा कि भारतवर्ष पूर्वी-पश्चिमी सभ्यताओं का समूह नहीं, वरन मानवता का संस्कार देने के लिए ईश्वरीय योजनानुरूप इस राष्ट्र का उदय हुआ। भारत की राष्ट्रीय संस्कृति का निर्माण हजारों वर्ष में हुआ है। उसके निर्माण के कई कारक हैं। साहित्य का अवदान उसमें अन्यतम है। अपनी संस्कृति का सीधा संवाद साहित्य से होता है। भारतीय साहित्य की पारस्परिक अन्तःसंबद्धता तथा आधारभूत एकता को प्रतिबिम्बित करने वाले अनेक तत्त्व दृष्टिगोचर होते हैं। हम प्रकृति के सहचर हैं, जिससे हम रस ग्रहण कर जीवन को गति प्रदान करते हैं, दूसरी ओर पश्चिमी दृष्टि की धारणा है कि मनुष्य का प्रकृति पर आधिपत्य है और वह भोग के लिए है। भारतीय परम्परा का ज्ञान हमारे साहित्य ने करवाया। राम, कृष्ण, वाल्मीकि, वेदव्यास का व्यक्तित्व हमारी विरासत में साहित्य की देन है। शरीर नश्वर है, कर्म ही जीवन है, ज्ञान, इच्छा और क्रिया का समन्वय होना चाहिए यह सब हमारे साहित्य में लिखा गया और अपने-अपने समय के अनुकूल लिखा गया। भारतीय राष्ट्रीयता के लिए वन्देमातरम् का उद्घोष, शंकराचार्य का एकात्मभाव, विवेकानंद की विराट दृष्टि ने आने वाली पीढ़ियों को चमत्कृत कर दिशा दी।
भारत की विशालता और विविधता के बावजूद उसे परस्पर जोड़ने में संस्कृत-साहित्य का अन्यतम महत्त्व हैं। वेद, उपनिषद, स्मृति, ब्राह्मण ग्रन्थ, रामायण, महाभारत, चरक, सुश्रुत इत्यादि में सांस्कृतिक चेतना का ऐसा युग-युगीन सेतु बन चुका है, जिसमें पूरा भारत वर्ष एक बना हुआ है। कालिदास का रघुवंश, महाकाव्य, भवभूति और अश्वघोष का साहित्य, माघ और भाष का चिंतन हमारी राष्ट्रीयता संवर्धक है। संस्कृति की इस चेतना को बलवती बनाने में कश्मीर के पंडितों व आचार्यों का सराहनीय महत्त्व है। आचार्य कल्हण द्वारा लिखित राजतरंगिणी इतिहास का महाभारत के बाद पहला ग्रन्थ माना जाता है। इसी प्रकार विल्हण का योगदान कम नहीं है। जिस कश्मीर में आतंक का ताण्डव चक्र रहा है वहां कभी- 8वीं से 12 वीं शती तक प्रत्यभिज्ञा दर्शन का साम्राज्य था, जिसमें शैवोपासना की संस्कृति का उज्ज्वल प्रकाश बिखरता रहता था। इसी काल के दसवीं से ग्यारहवीं शती मे आचार्य अभिनवगुप्त ने ध्वनि में रस और रस में जीवन तलाशने का भगीरथ प्रयास किया था।
विवेकानंद ने 30 वर्ष की उम्र में अपने ज्ञान से दुनिया को विस्मित कर दिया था। उन्होंने 1200 वर्ष बाद शंकराचार्य की परम्परा को संवाहित किया और यह स्पष्ट किया कि मनुष्य श्रेष्ठ है। मनुष्य का अस्तित्व मानवता की पराकाष्ठा है एवं आत्म तत्त्व को पहचानना है। यही कारण है कि पश्चिम के विज्ञान और पूर्व के ज्ञान के समन्वय पर बल देने वाला व्याख्यान भारत को दुनिया में सिरमौर बनाता है। 1913 में गीतांजलि पर टैगोर को नोबेल पुरस्कार मिलता है। मैथिलीशरण गुप्त की भारत-भारती राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जन चेतना को जाग्रत करती है। 1915 में ‘उसने कहा था’ कहानी उस शाश्वत वचन को प्रमाणित करती हैं, जिसमें कहा गया है कि ‘रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई।‘ साकेत का यह कथन विचारणीय है- ‘संदेश नहीं मैं यहाँ स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया।’ यह साहित्य समकाल में लिखा गया, जो हमारी परम्परा से प्रभावित था। 1936 में ‘राम की शक्ति पूजा’ भी अपने अन्दर रामत्व को जगाने का प्रयास है। प्रसाद अथवा दिनकर, अज्ञेय अथवा धर्मवीर भारती सबने उस भारतीय परम्परा को आगे बढ़ाया, जिसके सूत्र वैदिक ऋषियों से प्राप्त हुए थे।
राष्ट्र को सांस्कृतिक दृष्टि से उन्नत बनाने में साहित्य का योगदान अतुल्य है। पं. विद्यानिवास मिश्र ने साहित्य और संस्कृति के अन्तःसम्बन्ध को व्याख्यायित करते हुए लिखा कि इस देश की संस्कृति सीता है, जो धरती से जनक के हल के नोक से पैदा हुई हैं। इस देश की संस्कृति गंगा है, जिन्हें भगीरथ ने अपने परिश्रम से पहाड़ खोदकर निकाला था। इस देश की संस्कृति गौरी है, जिन्होंने अपने प्रियतम को सौन्दर्य से नहीं तम से प्राप्त किया था। इस देश की संस्कृति असंख्य ग्रामीण बन्धु और वनवासी हैं, जो असंख्य बाधाओं को राम की धनुही से तोड़ने का विश्वास रखते है।
भारत के विभिन्न अंचलों में व्याप्त बोलियों का एक विशाल साहित्य है। उस विशाल लोक साहित्य में संस्कृति की अनेक तरंगे प्रस्फुटित हुई हैं। हिन्दी की तमाम उपबोलियों में, पंजाबी जुबान के साहित्य में, बंगला, उड़िया, असमिया, मलयालम, कन्नड़, तेलगु, तमिल भाषाओं में व्याप्त भारतीय संस्कृति के विविध रंगों का आस्वाद एक जैसा है। राजस्थानी लोकगीतों के प्रवाह में संस्कृति का रत्न छिपा है। कहना न होगा कि भारत की इन भाषाओं-उपभाषाओं में संस्कृति की समझ बड़ी समृद्ध है। अनेक भावों की अंतर तरंगे अध्यात्म के महाभाव में मिलकर एक महातरंग को जन्म देती हैं। भाषा-उपभाषा में लिखित और मौखिक साहित्य की लिपि भिन्न-भिन्न हो सकती हैं, उच्चारण में भेद हो सकते हैं, भौगोलिक विभिन्नताएँ हो सकती हैं, कहीं रेगिस्तान, कहीं हरियाली, कहीं मैदान तो कहीं पहाड़ हो सकते है- पर सबका भाव एक ही है।
भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में हिन्दी की राष्ट्रीय-सांस्कृतिक काव्य धारा ने भारत के आत्म-गौरव को जगाने का कार्य किया। इस धारा के कवियों में मैथिलीशरण गुप्त, सोहनलाल द्विवेदी, बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन‘, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्राकुमारी चौहान, रामधारीसिंह दिनकर आदि अनेक कवियों ने राष्ट्रीयता के भावों से संपन्न ऐसा साहित्य रचा कि वे स्वाधीनता आन्दोलन में जन-जागृति के प्रमुख स्रोत बन गए। यह भी उल्लेखनीय है कि स्वाधीनता संग्राम काल के इसी काल खंड में समानांतर रूप से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में असीम मात्रा में स्फुट काव्य भी सृजित हुआ, जिसने सामान्य जन-मानस के देशप्रेम को मुखर स्वर दिया और भारतीय मनीषा को जाग्रत किया।
सोहनलाल द्विवेदी राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के अत्यधिक ओजस्वी कवि रहे हैं। वासवदत्ता, कुणाल, विषपान आदि प्रबंधात्मक रचनाओं के माध्यम से पं. द्विवेदी जी ने अतीत की ओर उन्मुख देश के गौरवशाली इतिहास और भारत की सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय-संघर्ष के लिए प्रेरक स्रोत बनाया। उन्होंने राष्ट्रीयता का मुक्त कंठ से गान किया था। “भैरवी” के विप्लवी गीतों में कवि के प्राण राष्ट्रीय भावना में बहते हुए से दिखाई देते हैं। राष्ट्र की चेतना को संपूर्ण रूप में प्रस्तुत करते हुए कवि ने स्वयं अपने स्वरों को राष्ट्र-प्रेम पर समर्पित कर उत्साह का संचार किया, यथा-
वन्दना के इन स्वरों में, एक स्वर मेरा मिला दो।
वंदिनी माँ को न भूलो, राग में जब मत झूलो।
अर्चना के रत्न कण में, एक कण मेरा मिला लो।।
बालकृष्ण शर्मा ‘नवीन’ की कविताओं में स्वदेश धर्म का निर्वाह, कारागार के शून्य जीवन में भी सार्थकता, मातृभूमि के प्रति अपार लगाव, कवि की अन्तर्चेतना तक जागरण की ध्वनि पहुँचाने की क्षमता और राष्ट्र के प्रति एकनिष्ठ प्रेम से उन्हें कालजयी बनाने का अवसर प्राप्त होता है। राष्ट्रधर्म की रक्षा तत्कालीन समय की मांग थी। अंग्रेजों के समक्ष निडरता से हृदय की अभिव्यक्ति को प्रकट करना साहस भरा कार्य था। ‘नवीन’ जी ने राष्ट्रीय भावों को काव्य का विषय बनाकर भारतीय जनता की स्वातंत्र्य चेतना को विकसित किया। विदेशी दासता के विरूद्ध शंखनाद करती उक्त पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं-
कोटिकोटि कंठों से निकली, आज यही स्वरधारा है।
भारत वर्ष हमारा है यह, हिन्दुस्थान हमारा है।
महाकवि निराला ने युगीन आवश्यकता को दृष्टिगत रखकर राष्ट्रीयता को संस्कृति के स्वरूप में ढालकर चित्रित किया। ‘भारती वंदना’, ‘यमुना के प्रति’, ‘मातृवन्दना’, ‘जागो फिर एक बार’, ‘दिल्ली’, ‘खण्डहर के प्रति’, ‘राम की शक्ति पूजा’, ‘तुलसीदास’ आदि में राष्ट्रीयता का भव्य स्वरूप दृष्टिगोचर होता है। भारत भूमि को माता मानकर स्तुति करते हुए लिखते हैं-
भारति, जय विजय करे, कनक-शस्य-कमल धरे
लंका पद-तल-शत दल, गर्जितोर्मि सागर जल
धोता शुचि चरण युगल, स्तव कर बहु अर्थ भरे।
रामधारीसिंह ‘दिनकर’, जिनके काव्य में राष्ट्र-प्रेम की पूजा है, राष्ट्रीय संस्कृति की पुनः उन्नयन की अभिलाषा है, सामाजिक चेतना की युगाभिव्यक्ति है तथा ओज और प्रसाद का मिश्रण है। उस विराट व्यक्तित्व का महत्त्व न केवल हिन्दी साहित्य में बल्कि भारतीय जन मानस के हृदय की मुखर अभिव्यक्ति में स्पष्ट परिलक्षित होती है । दिनकर अहिंसा को शक्ति और पौरूष के साथ स्वीकार करता है। उनके अनुसार त्याग करूणा और क्षमा शूरवीरों को शोभा देती है और अपमान, शोषण को सहन करना कायरता है-
छोड़ प्रति वैर पीते मूक अपमान वे ही;
जिनमें न शेष शूरता का वह्निताप है।।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपना का स्थापना काल भारत के स्वाधीनता-संघर्ष काल के समय का है। भारतीय राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के विचार को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से यह संगठन स्थापित हुआ और एक शताब्दी की यात्रा इसका प्रमाण है। जिसका उद्देश्य है-ऐसे व्यक्तियों का निर्माण जो राष्ट्र प्रेमी कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, प्रामाणिक और मूल्यों की रक्षा करने वाले हों। संघ के इस विराट उद्देश्य की प्रतिपूर्ति हेतु तथा स्वयंसेवकों को वैचारिक दृष्टि प्रदान करने के लिए संघ गीत रचे गए। इन गीतों की विषय वस्तु में मातृ-वंदना, राष्ट्र-अर्चना, ध्वज-वंदन, ध्येय-चिंतन, केशव-माधव वंदना, उद्बोधन, संचलन एवं प्रासंगिक गीत प्रमुख हैं। आज ये गीत देश के आम जन गुनगुनाते हैं। ‘वन्देमातरम‘ गीत स्वाधीनता संग्राम का महत्त्वपूर्ण प्रेरणा-गीत बनकर उभरा। इस गीत के महत्त्व को एक राष्ट्रप्रेमी व्यक्ति बहुत अच्छी तरह समझता है। यह केवल एक गीत नहीं, बल्कि सांस्कृतिक गौरव का अभियान भी है। ‘राष्ट्र की जय चेतना‘ संघ-गीत में रचनाकार की अनुभूति निम्न शब्दों में प्रकट होती है-
सृष्टि बीज मंत्र का है मर्म वन्देमातरम।
राम के वनवास का है काव्य वन्देमातरम।
दिव्य गीता ज्ञान का संगीत वन्देमातरम।
राष्ट्र की जय चेतना का गान वन्देमातरम।
किसी भी देश की संस्कृति को प्रणम्य बनाने एवं कालखंड को अमरता प्रदान करने में साहित्यकार की अहम् भूमिका होती है। भारतीय संस्कृति सनातन, समृद्ध और जीवन्त है। आज भारतीय समाज जाति-पंथ-मत आदि विषमताओं से संघर्ष कर रहा है। विदेशी ताकतें छल, भय, प्रलोभन आदि से धर्मान्तरण करने के षड़यंत्र कर रही हैं। तब भारतीय साहित्य का अवलोकन समीचीन होगा। भारतीय समाज की समन्वयात्मक दृष्टि सम्पूर्ण साहित्यिक फलक पर प्रतिभासित है। भारतीय चिंतन परम्परा व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित है। हमारे जीवन का कोई पक्ष ऐसा नहीं है, जिस पर हमारी परंपरा ने विचार नहीं किया। हमारे शास्त्रों ने जीवन के उज्ज्वल उदात्त पक्ष को ग्रहण करने पर सदैव बल दिया। इसकी परम विशेषता रही है कि उसने पदार्थ को आवश्यक माना पर उसे आस्था का केन्द्र नहीं, शस्त्र-शक्ति का सहारा लिया, लेकिन उसमें त्राण नहीं देखा, अपने लिए दूसरों का अनिष्ट हो गया, पर उसे क्षम्य नहीं माना। यहाँ जीवन का लक्ष्य विलासिता नहीं, आत्म-साधना रहा, लोभ-लालसा नहीं, त्याग-तितिक्षा रहा।
हिन्दी का भक्ति साहित्य इस दृष्टि से अनिर्वचनीय है, जहाँ कबीर तुलसी जैसे महात्माओं ने समाज के एकात्म को गहराई से पहचाना। युगद्रष्टा कबीर ने जब इस भूमि पर अवतरण लिया, वह युग हिन्दुओं के लिए घोर निराशा का था। उनकी संस्कृति व राष्ट्र दोनों ही पद-दलित हो रहे थे। समाज दिशाविहीन था तो संक्रमणकाल में महात्मा कबीर ने भारत-भूमि के सांस्कृतिक और राष्ट्रीय आदर्श को कायम रखने के लिए लोक-मानस का नेतृत्व किया और अपने प्रखर व्यक्तित्व से घोर-निराशा के दलदल में फँसी भारतीय जनता को नव-जीवन प्रदान किया। उन्हें सांस्कृतिक विरासत के संवाहक की संज्ञा से अभिहित किया जाये, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। भारतीय जन मानस अपनी संस्कृति के प्रति निष्ठावान था, तो बाह्याडम्बरों से उसमें विकृतियाँ भी व्याप्त हो गई थी। आचरण की अपेक्षा उपासना पद्धति महत्त्वपूर्ण हो गई थी। विधर्मियों के उपहास से आहत भारतीय लोक मानस को अपने आन्तरिक आचरण को शुद्ध करने पर बल दिया और आत्म-ज्योति को जाग्रत करने का आह्वान करते हुए कहा कि इस मन को मथुरा, दिल को द्वारका और काया को काशी समझो। दस द्वारों वाला देवालय रूपी शरीर तुम्हारे पास है, उसी में आत्म-ज्योति को तलाश करो, यथा-
मन मथुरा, दिल द्वारिक, काश कासी जाँनि।
दस द्वारे का देहरा, तामें जोति पिछांनि।।
इन पंक्तियों में महात्मा कबीर ने जनता की उपासना पद्धति को परिष्कृत कर उसे भारतीय मूल्यों की ओर अग्रसर किया, जिसमें आत्म-ज्योति का अवलोकन महत्त्वपूर्ण तत्त्व है। हिन्दुस्तान की सांस्कृतिक गत्यात्मकता ने रूढ़ियों को तोड़कर परम्पराओं को परिष्कृत किया। जातिगत दुर्व्यवहार से त्रस्त हिन्दू समाज को मुक्ति दिलाने में महात्मा कबीर का अद्वितीय योगदान रहा। वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के नाम पर जब हिन्दू समाज अस्पृश्यता के दलदल में फँस गया, तो उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा-
काहै को कीजै पांडे छोति विचारा, छोति हि ते उपजा संसारा।
हमारे कैसे लोहू, तुम्हारे कैसे दूध, तुम कैसे ब्राह्मन पांडे, हम कैसे सूद।।
गोस्वामी तुलसीदास ने तत्कालीन सामाजिक परिस्थितियों का अध्ययन कर उसी के अनुरूप अपने युग की रूपरेखा प्रस्तुत की। उन्होंने अपने काव्य में राम जैसे आदर्श चरित्र के भीतर अपनी अलौकिक प्रतिभा एवं काव्य शास्त्रीय निपुणता के बल पर भक्ति का प्रकृत आधार खड़ा किया तथा उसमें मानव जीवन के पारिवारिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक आदि सभी दशाओं के चित्रों और चरित्रों का विधान किया। उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से सामाजिक विषमता और वैमनस्य को कम करने का प्रयत्न किया। विभिन्न मत-मतान्तरों में समन्वय का प्रयास किया। इसी कारण आलोचक उन्हें ‘समन्वयवादी भक्त कवि’ के रूप में सम्बोधित करते हैं। डॉ. हजारी प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में, “तुलसीदास को जो अभूतपूर्व सफलता मिली, उसका कारण यह था कि वे समन्वय की विराट् चेष्टा है। उनके काव्य में ज्ञान और भक्ति, सगुण और निर्गुण, गार्हस्थ्य और वैराग्य, शैव और वैष्णव, राजा ओर प्रजा, शील ओर सौन्दर्य आदि के समन्वय की भावपूर्ण झाँकी देखी जा सकती है। तुलसीदास शुद्ध साधना के समर्थक थे। इसमें वह गृहस्थ और संन्यासी में किसी प्रकार के भेद को स्वीकार नहीं करते थे। उनकी दृष्टि में साधक चाहे घर में रहे या वन में, उसके लिए विषय-वासना से विमुखता आवश्यक है-
जो जन रूखे विषय-रस चिकने राम-सनेह।
तुलसी ने प्रिय राम के कानन बसहिं के गेह।।
तुलसीदास के समय में शैव और वैष्णव संप्रदाय का वैमनस्य चरम पर पहुँच गया था। शैव सम्प्रदाय शिव को तथा वैष्णव सम्प्रदाय विष्णु की भक्ति को सर्वोपरि मानते थे। रामचरित मानस में विष्णु के अवतार श्रीराम को शिव-भक्त बताकर समन्वय की धारा बहाई, यथा-
शिव द्रोही मय दास कहावे।
ते नर मोहि सपनेहु नहिं भावे।।”
आधुनिक रचनाकारों में प्रसाद रचित कामायनी ‘सामरस्य’ पर बल देती है। कामायनी में स्पष्ट होता है कि हमारा सामाजिक जीवन विसंगतियों को शिकार हो गया है। जाति, धर्म, संप्रदाय आधारित विकृत व्यवस्था मानवता के साथ चल रही है, जिसके मूल में मात्र विद्वेष है। यह विद्वेष ही संघर्ष को जन्म दे रहा है। प्रसाद ने कहा-
द्वयता में लगी निरन्तर ही, वर्णों की करती रहे सृष्टि।
अनजान समस्याएँ गढ़तीं, रचती हैं अपनी ही विनष्टि ।।
क्या यह विद्वेष समाप्त नहीं हो सकता? हम आधुनिक मानव एवं विकसित सभ्यता का दंभ पालने वाले ऐसे विश्व का निर्माण नहीं कर सकते, जैसा कामायनी में वर्णित है-
शापित न यहाँ है कोई, तापित पानी न यहाँ हैं।
जीवन वसुधा समतल है, समरस है जो कि जहाँ है।।
एकात्म मानववाद की अवधारणा मनुष्य को खंड-खंड दृष्टि से नहीं देखती, बल्कि उसे केन्द्र में रखकर परिवार, समाज, राष्ट्र और विश्व से जोड़ती है। यह विलक्षण मानवीय चेतना आधारित दृष्टि स्वयंमेव अद्वितीय है। भारतीय मन वसुधा को ही कुटुम्ब मानता है। सुख और शांति के संदेश देने के साथ यहाँ की विचारधारा ने त्रस्त, दुःखी और व्याकुल प्राणी को सदा आश्रय दिया है। यह करुणावृत्ति मानवता का उच्च मानक है। मानवीय चेतना के प्रसार हेतु नैतिक मूल्यों का अनुसरण हों, मानवतावादी स्वरों का विस्तार हो, मानवीय मूल्यों को प्रश्रय मिले और हिन्दुत्व मानवता का कल्याण करे, इन भावों की सृष्टि संघ-गीतों में हैं।
हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। जाति, भाषा, क्षेत्र, वर्ग, दर्शन, पंथ आदि के आधार पर अनेक विभेद बाहरी रूप में दिखाई देते हैं, परन्तु अखण्ड और अमिट संस्कृति के बल पर हम एक हैं। सत्य सनातन धर्म की ध्वजा चिरन्तन काल से अब तक टिकी रही है। यद्यपि इसे मिटाने की पूरी कोशिश हुई। अब हमारी पीढ़ी का यह दायित्व है कि हम राष्ट्रभाव का जागरण करें। ‘नव चैतन्य हिलोरें लेता‘ संघ-गीत में निहित संदेश इसी भाव को प्रकट कर रहा है-
जाति भाषा वर्ग भिन्नता, हैं कितने मिथ्या अभिमान।
क्षेत्र-क्षेत्र के स्वार्थ उभारे, ले अपनी-अपनी पहचान।
राष्ट्रभाव का करें जागरण, पाट चलेंगे सब खाई।
नव चैतन्य हिलोरें लेता, जाग उठी है तरुणाई।।
वर्तमान समाज प्रगतिशीलता के रथ पर आरूढ़ अवश्य है, परंतु मनुष्य के आचरण में असत का प्रवेश चिंता का विषय है। सदाचार से आस्था का विचलन होने से नैतिक व चारित्रिक पतन के लक्षण हमारे समाज में दिखाई देने लगे हैं। इस समस्या का समाधान भारतीय जीवन शैली में विद्यमान है, जहाँ व्यवहार एवं आचरण को सदाचार की कसौटी पर परखा जाता है और सामाजिक प्रतिष्ठा का मापदंड भी माना जाता है। अपने दैनिक जीवन में प्रेम के साथ सात्विकता भी आवश्यक है। यह प्रेम ही जाति, भाषा, प्रांत वर्ग आदि का भेद मिटा सकता है। संघ द्वारा भारतीय जीवन में अपेक्षा की गई है कि वह अपने जीवन में संयम आधारित जीवनशैली अपनाएँ और शुद्ध सात्विक प्रेम को अपने जीवन का अंग बनाकर आदर्श की स्थापना करे। संघ-गीत 'शुद्ध सात्विक प्रेम' में निहित स्वर इस प्रकार है-
जाति, भाषा,प्रांत आदि, वर्ग भेद को मिटाने।
दूर अर्थाभाव करने, तम अविद्या का मिटाने।
नित्य ज्योतिर्मय हमारा, हृदय स्नेहागार है।
शुद्ध सात्विक प्रेम अपने, कार्य का आधार है।।
हम अपने अहिंसक दृष्टि से अनुभवों की भयंकरता का का विनाश कर सकते हैं, अभय के द्वारा भय को नष्ट कर सकते हैं, त्याग के द्वारा संग्रह-वृत्ति को बाधित कर सकते हैं, तब किसी की ओर क्यों जाएँ? यह घोष संस्कृति और कला का प्रतीक बने तो जीवन की भी दिशा बदल सकती है। संघ-गीतों में इन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों के महत्त्व को रेखांकित किया गया है। अप्रासंगिक रूढ़ियों के बंधन से मुक्त होकर समय अनुकूल सांस्कृतिक परिवर्तन और उसका हस्तांतरण कैसे हो? इस पर विचार किया गया है। अब समय आ गया है कि हम सांस्कृतिक आदर्शों को स्वयं के निर्माण में लगाएँ। साथ ही विश्व में भी इन मूल्यों का प्रचार करें। संघ-गीत 'हे जन्मभूमि भारत' गीत में व्यक्त भाव द्रष्टव्य हैं-
जो संस्कृति अभी तक दुर्जेय-सी बनी है।
जिसका विशाल मंदिर आदर्श का धनी है।
उसकी विजय-ध्वजा ले हम विश्व में चलेंगे।
संस्कृति-सुरभि-पवन बन हर कुंज में बहेंगे।।
वर्तमान समय संक्रमणकालीन वेला से गुजर रहा है, नवनवोन्मेषशालिनी प्रज्ञास्फोट की प्रतिध्वनि में बौद्धिकता साहित्य के मस्तिष्क पर विलास कर रही है। हृदय पक्ष अमा-निशा के गर्त में दुबक कर बैठा है। पुरुषार्थ चतुष्ट्य की आंकाक्षी भारतीय सामाजिक परम्पराएँ विद्रुपताओं से ग्रस्त होती जा रही है। आस्था, अनास्था, नव्य-पुरातन, पौर्वात्य-पाश्चात्य के द्वन्द्व में फँसा साहित्य पटल स्वयं ‘अर्थ-वलय’ से ग्रसित है। सत्य, अहिंसा, क्षमा, सहिष्णुता, संयम, त्याग आदि हमारे सांस्कृतिक मूल्य शाश्वत रूप में विद्यमान रहे हैं। भारतीय-चिंतन विज्ञान का सम्मान करता है, किंतु एकांगी दृष्टि से नहीं। यदि सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर विज्ञान का विकास होता है तो वह सदैव श्रेयकारी होगा। पश्चिमी चिंतन ने मानवता को बहुत कष्ट दिया है, पर अब समय आ गया है कि हम अपनी विरासत से प्यार करें। उन मूल्यों को पहचाने जिससे हमारा आने वाला कल समृद्ध बने। ऐसे समय में राष्ट्रीय-सांस्कृतिक भाव दृष्टि और सामाजिक समरसता निर्माण में साहित्य अपनी भूमिका सशक्त ढंग से प्रस्तुत कर सकता है।
==============================================================