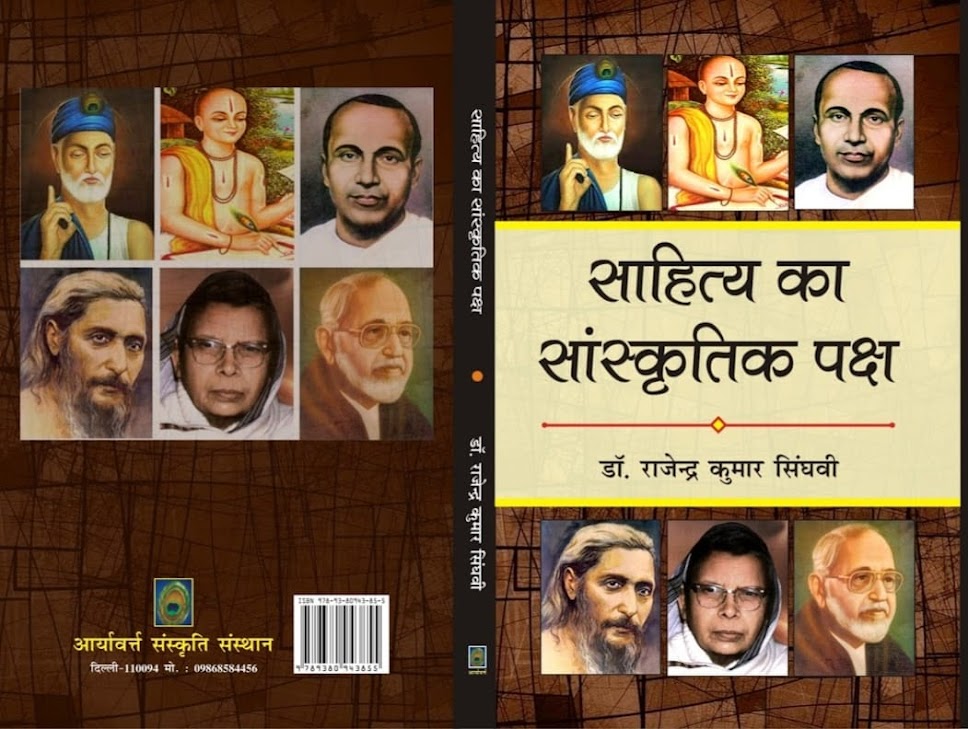कविता का वर्तमान एवं औपनिवेशिकता
जनकृति, अंक दिसम्बर,२०२० में प्रकाशित
सारांश :
15 अगस्त, 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया, किंतु उपनिवेशवादी मानसिकता से हम अभी तक मुक्त नहीं हो पाए हैं। हमारा हीनता बोध से ग्रस्त वर्तमान अतीत के क्रियाकलापों का परिणाम है। हमारे अतीत का गौरव, उसकी गति और तारतम्यता को लक्ष्य बनाकर भ्रष्ट किया गया। भारतीय मेधा को तिरस्कृत कर सोच और कल्पना को ही कुंद कर दिया गया। इस औपनिवेशिकता ने भारत के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर आर्थिक समृद्धि को छीन लिया, वहीं सांस्कृतिक वर्चस्व कायम करने के लिए भारतीय मन और आत्मा को भी पराधीन करने की चेष्टा की। इसमें वे काफी सीमा तक सफल रहे, परिणाम स्वरूप वर्तमान समाज आजादी के बहत्तर वर्षों के बाद भी औपनिवेशिक प्रभाव से मुक्त नहीं हो पाया है। सदी के दूसरे दशक का उत्तरार्द्ध पूर्ण होने जा रहा है। भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के स्खलन, भाषा, रहन-सहन, विचार-पद्धति, जीवन-शैली, वेशभूषा, शिक्षा और जीवन-मूल्यों में जो अवांछित विद्रूपताएँ आई हैं, उन्हें समकालीन हिन्दी कविता ने पहचाना है। उसमें औपनिवेशिक प्रभाव की गहराई और उससे जनित विसंगतियों पर कवियों ने प्रहार किया है। अब वह केवल आक्रोश व्यक्त कर चुप नहीं रहता, वरन् व्यवस्था परिवर्तन के लिए मुखर हो उठा है। वह जीवन की विषमताओं का हल भारतीय मूल्यों में तलाशता है। उसकी लेखनी में इतना पैनापन आ गया है कि राजनीतिक व्यवस्थाएँ भी कविता के संकेतों से प्रभावित होने लगी हैं।
बीज शब्द :
उपनिवेशवाद, सांस्कृतिक मूल्य, यांत्रिक सभ्यता, विश्वग्राम, भारतीयकरण, आवारा पूँजीI
भूमिका:
किसी समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा अपने विभिन्न हितों को साधने के लिए किसी निर्बल किंतु प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण राष्ट्र के विभिन्न संसाधनों का शक्ति के बल पर उपभोग करना उपनिवेशवाद है।1 इसमें जनता एक विदेशी राष्ट्र द्वारा शासित होती है। इतिहास में प्रायः पन्द्रहवीं से बीसवीं शताब्दी तक उपनिवेशवाद की व्यापकता रही। ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का आरंभ हुआ। इसका प्रभाव राजनीति, धर्म, संस्कृति एवं अर्थव्यवस्था पर गइराई से पड़ा। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद ज्ञान को भी संहारक बना देते हैं। कृष्णकुमार लिखते हैं, “ज्ञान-विज्ञान व विचारों की प्रकृति वैश्विक होती है, लेकिन साम्राज्यवाद ने शिक्षा, पाठ्यचर्या के माध्यम से उपनिवेशों के नागरिकों में हीनता पैदा करने के लिए ज्ञान को हथियार की तरह प्रयोग किया। अपनी उपलब्धियों को श्रेष्ठ-अनुकरणीय, आधुनिक-प्रगतिशील बताया।”2 मैकाले का कथन- “किसी भी अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी ही पूरे भारत और अरब की संपूर्ण ज्ञान-संपदा से अधिक है।”3 वस्तुतः यह कथन मात्र कूटनीतिक नहीं, बल्कि हमारे दिलो-दिमाग पर साधा गया अचूक निशाना था, जिसके घाव अभी तक हरे हैं।
विषय-विस्तार :
औपनिवेशिक शक्तियाँ सर्वप्रथम प्राचीन संस्कृति के उद्धार के बहाने उसकी रचनात्मकता, सनातनता और प्रेरक परम्पराओं को निशाना बनाती है तथा अपने ज्ञान-विज्ञान से शासित वैचारिक नेतृत्व प्रदान करती है। यह मानसिक उपनिवेशीकरण सांस्कृतिक प्रभुत्व में परिवर्तित होकर बुद्धिजीवियों की समझ को भी कुंद कर देता है। अन्ततः पराधीन जन-मानस उसकी ही वाणी में बोलकर गर्व का अनुभव करता है और औपनिवेशिक प्रभाव में स्वयं का विलयन कर तदनुसार ही व्यवहार करने लग जाता है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति में राष्ट्रवाद एकमात्र विकल्प प्रतीत होता है। यह अतीत से ऊर्जा ग्रहण कर वर्तमान संदर्भों में उसकी पुनर्व्याख्या करता है। साथ ही महान् सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मूल्यों के सहारे चेतना का निर्माण कर अपने सांस्कृतिक औजारों से कुचक्रों को नष्ट करता है। इस पुनीत कार्य में साहित्य की भूमिका अनिर्वचनीय है।
स्वप्निल श्रीवास्तव के अनुसार- “ आज का यथार्थ मारक और अविश्वसनीय है। वह फैंटेसी के आगे का यथार्थ है। आज के यथार्थ का चेहरा रक्तरंजित और अमानवीय है। यथार्थ हमारे सामने विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत करता है, जो कल्पनातीत है।”4 विस्मयकारी यथार्थ का जो दृश्य नई सदी के दो दशकों में दिखाई देता है, वह उपनिवेशवादी प्रभाव का परिणाम है। फलतः जो कारक हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनमें प्रमुख हैं- वैश्वीकरण, मुक्तबाजारवाद, विकृत उभोक्तावाद, राजनीतिक अधिनायकवाद, मूल्यहीनता, सांस्कृतिक संघर्ष, भ्रष्ट आचार, हिंसक वर्चस्व आदि। यद्यपि ये कारक वैश्विक हैं, किन्तु भारतीय मन इससे ज्यादा प्रभावित है। प्रस्तुत आलेख में नई सदी के दो दशकों में हिन्दी कविता ने किस तरह औपनिवेशिकता से संघर्ष किया, उसकी विवेचना है-
नई सदी की सर्वाधिक ज्वलन्त चुनौती वैश्वीकरण है। जिसने बाजारवाद के प्रश्रय के साथ जीवन-मूल्यों का ह्रास किया, सांस्कृतिक विविधताओं का विलोपन किया, विकृत उपभोक्तावादी दृष्टि ने हमें जड़ों से उखाड़ों से उखाड़ दिया। फिर भी नई सदी का कवि निराश नहीं है। वह इनका प्रतिरोध करता हुआ यह संदेश देता है कि जो अपने मूल तत्त्व से जुड़कर संघर्ष करेगा, अन्ततः वही बचेगा-
जड़ से उखड़ गए बहुत से पेड़
इस प्रभंजन में
अपने रूप-रस-गंध पर मुग्ध
जो थे इठलाते-झूमते
धराशायी हो गये वे
बचे केवल वही
जिनके मूलांकुरों ने रात-दिन जागकर
धरती की अंधेरी परतों में घुसकर
किया था अथक संघर्ष।5
यांत्रिक सभ्यता के दौर में नगरीकरण का विस्तार हुआ। नगरों की भीड़ में सबकुछ खो गया। मनुष्यता और संवेदना की परतें भी उखड़ती गई। अन्ततः हम अपने बचे हुए अवशेषों को भी सहेज कर नहीं रख पा रहे। महानगरीय भीड़ में तेज रफ्तार वाले वाहनों के मध्य चलती बैलगाड़ी को कवि ने सभ्यता का आखिरी मनुष्य इंगित करते हुए सावचेत किया-
लगता है एक वही तो है
हमारी गतियों का स्वस्तिक चिह्न
लगता है एक वही है, जिस पर बैठा हुआ है
हमारी सभ्यता का आखिरी मनुष्य।6
प्रो. योगेन्द्र सिंह ने अपनी पुस्तक ‘भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण’ में लिखा है- “वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सांस्कृतिक सापेक्षिकता और इतिहासपरकता का तत्त्व वर्तमान है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में ‘स्थानीयता’ का तत्त्व बना रहता है। ‘ग्लोबलाइजेशन’ के साथ ‘ग्लोकालाइजेशन’ की निरन्तर उपस्थिति इसको उजागर करती है।”7 इससे उत्पन्न दारुण और बदरंग यथार्थ यह है कि नव उपनिवेशवादी वृत्ति में आतंक का आततायीपन प्रकट होने लगा है-
वे
चिड़ियों के पर कतर रहे हैं
और कह रहे हैं-
‘परिवर्तन हो रहा है’
वे हरियाली निचोड़ रहे हैं
और कह रहे हैं-
‘प्रकृति में क्रांति हो रही है’8
औपनिवेशिक मानसिकता से ग्रस्त समाज अपने अतीत को भूलकर वर्चस्व की लड़ाई लड़ता है। नई सदी के आरंभ में एक विकृति तेजी से उभरी है, वह है- धर्मोन्माद। यहाँ सभ्यताओं को भी धर्म का पर्याय बनाकर प्रस्तुत कर दिया गया है। फलतः घृणा, हिंसा और प्रतिशोध की आग में बस्तियाँ जल रही है और उसकी तपिश नई सदी में महसूस की जा रही है। इस उन्माद के पश्चात बचता है तो केवल-वैमनस्य। कवि ने इस ओर संकेत किया है-
कि कहीं मिलता है आधा जला हुआ दुपट्टा
कहीं आधा जला हुआ खिलौना
कहीं अधजली बीड़ी
कहीं दमकलों के पाइप
कहीं दिलजले
कहीं कहीं तो
केवल जलन मालूम होती है।”9
वैश्विक स्तर पर आर्थिक उदारीकरण आधारित विश्व-व्यवस्था, जनसंचार का प्रसार और विश्वग्राम की जन्नत को हकीकत में बदलता देख साम्राज्यवादी शक्तियाँ नव-उपनिवेशवादी संस्करण में उपस्थित हो रही हैं। ये अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, विश्व व्यापार संगठन आदि के माध्यम से पुनः पंगु बनाकर गरीबी के रसातल में धकेल रहा है। उपनिवेशवादी शक्तियों की इस कुत्सित चाल को समझकर कवि स्पष्ट करता है-
वह बहुत ताकतवर है
क्रूर कुचाली और महाकपटी
विश्व बैंक उसका घातक अस्त्र है।
अन्तरराष्ट्रीय मुद्राकोष उसका कुचक्र
विश्व व्यापार संगठन उसका इन्द्रजाल
वह किसी का मित्र नहीं है।10
औपनिवेशिक मानसिकता ने हमें पदार्थवादी बना दिया। आवारा पूँजी के प्रभाव से यदि हमने कुछ खोया है तो वह है- रिश्तों की बुनियाद। शहर में चारों ओर कंक्रीट के जंगल उग गये हैं। बुजुर्गों से भरी शहरी कोलोनियाँ किलकारियों के लिए तरस रही है। चारों तरफ रिश्ते दरक रहे हैं, परिवार टूट रहे हैं और जीवन अशांत। सामयिक यथार्थ को उजागर करती ये पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-
बहुत कुछ कहना चाहता है वह
मगर कहे किससे
उसके आसपास अब
सब कुछ उजाड़ है।11
बाजारवादी शक्तियों के पूर्ण प्रभाव में आकर आज का मीडिया भी सत्ता का सहयोग कर ‘कारपोरेट जगत’ को अनुकूल वातावरण दे रहा है। भूखे और नंगों की हकीकत बयां कर उसे बेचने का कर्म भी वह कर लेता है। अपने भारी-भरकम शब्दों के माध्यम से खबरों को उठाता है और फिर बेच देता है, इन्हीं व्यावसायिक घरानों के हाथ। यह व्यापार जारी है-
हम ज्ञानहीनों के बारे में ज्ञानियों के/हम गुमनामों के बारे में
नामचीनों के/शब्द छप रहे हैं/भारी भरकम शब्द
हम दुबले अबलों के बारे में/चिकने चुपड़े शब्द/
हम रूखे सूखों के बारे में/खाये/अधाये शब्द/
हम भूखे नंगों के बारे में/खबरों में छप रही है।12
चमकती दुनिया में मध्यम वर्ग अनिर्णय का शिकार है। लाभ का सौदा दिखते ही वह दौड़ लगाना शुरूकर देता है। गंतव्य उसे ज्ञात नहीं है। आडम्बर की संस्कृति को वह खुशनुमा मानता है। मौन-प्रतिक्रिया में अपनी शांति खोजता है। विसंगतियों के विरूद्ध वह चुप रह जाता है-
एक गंदी अंधेरी गली में परिवार पालता/
वह अपनी नहीं दूसरों के संघर्ष की/अंतहीन
कथा कहता है और एक दिन मर जाता है/
हम कुछ नहीं कहते ।13
निष्कर्ष :
भारतीय औपनिवेशिक मानसिकता से संघर्ष में हिन्दी साहित्य की भूमिका अविरल रूप से गतिमान है। हिन्दी कथा, नाट्य एवं काव्य-साहित्य में न केवल औपनिवेशवादी दुश्चक्रों की पहचान की गई है, वरन् उनका प्रतिकार भी है। बहुलतावादी भारतीय समाज में जातीय-धार्मिक उन्माद, सांस्कृतिक मूल्यहीनता, वैचारिक अतिवाद एवं भटकाव का सबसे बुरा समय माना जा सकता है। सुखद पहलू यह है कि हिन्दी कविता ने इन कारकों को पहचान लिया है और भारतीय समाज को चेतनावान बनाने की ओर निरन्तर प्रयासरत है। औपनिवेशिक दासता से मुक्ति के लिए हिन्दी कविता का आगामी दशक समाधान प्रदान करने वाला होगा, ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।
संदर्भ-
1. वेब पेज, विकिपिडिया,उपनिवेशवाद, पृ.1
2. कृष्ण कुमार, औपनिवेशिक दासता का ज्ञानकाण्ड, देस हरियाणा, नव.-दिस.2015, पृ.23
3. पूर्ववत्, पृ.22
4. आलोचना, अप्रैल-जून,2003, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.32
5. इन्दुशेखर तत्पुरूष, बचे केवल वही, पीठ पर आँख, बोधि प्रकाशन जयपुर, सं.2017, पृ.10
6. भगवत रावत, बैलगाड़ी, तद्भव अंक-9, पृ.155
7. योगेन्द्र सिंह, भारतीय परम्परा का आधुनिकीकरण, रावत पब्लिकेशन, जयपुर,सं.2006, पृ.7
8. संजय पंकज, यवनिका उठते तक, समीक्षा प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.2001, पृ.79
9. अष्टभुजा शुक्ल, बस्ती एक धीमा शहर है, तद्भव, अंक-10 पृ.113
10. विजेन्द्र, दैत्य को पछाड़ो, बेघर का बना देश, साहित्य भण्डार, प्रयागराज, सं.2014,पृ.64
11. हरीश पाठक, पहले ऐसा नहीं था, नमन प्रकाशन, नई दिल्ली, सं.2008, पृ.22
12. हरे प्रकाश उपाध्याय, खबरें छप रही हैं, तद्भव, अंक-12, पृ.122
13. ऋतुराज, हम कुछ नहीं कहते, तद्भव, अंक-2,पृ.150
- - -