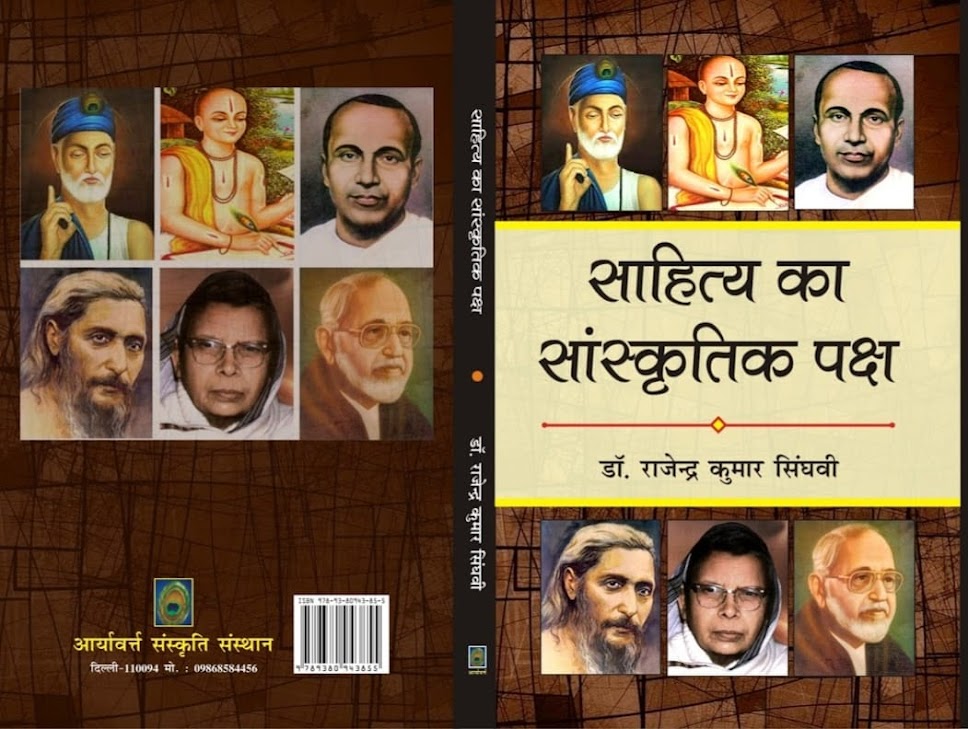आस्थावादी दृष्टि का विस्तार एवं धर्मवीर भारती का काव्य
('भावक' पत्रिका के अक्तूबर-दिसम्बर, २०२२ अंक में..)
डॉ. धर्मवीर भारती प्रयोगवादी और नई कविताओं की संक्रांतिकालीन बेला के साक्षी रहे हैं। तत्कालीन परिस्थितियाँ जहाँ एक ओर युद्ध जनित त्रासदियों की शिकार मानवता है, तो दूसरी ओर अंधकारमय वातावरण में भी जीवन के प्रति उत्कट भाव प्रवणता। इस संधिकालीन समय में कवि भारती के मन में दुविधा, संशय और भय के साथ-साथ आस्था का स्वर भी अंकुरित होता है। ‘ठंडा लोहा’, ‘अंधायुग’, ‘कनुप्रिया’, ‘सात गीत वर्ष’ जैसी कृतियाँ डॉ. भारती की एक दशक की ऐसी रचनाएँ हैं, जहाँ वे नवीन भाव और विचार बोध को जन्म तो देते हैं, परंतु संपूर्ण कृतित्व में आस्था और अनास्था का द्वंद्व निरंतर जारी रहता है।
डॉ. भारती की आरंभिक रचनाओं में गहरी भावुकता, स्वप्निल उड़ान, प्रणय भावना के साथ सामाजिक संघर्ष के स्वर मिलते हैं। इन रचनाओं में किशोरावस्था का प्रणय, रूपासक्ति, आत्मसमर्पण की भावना और अहं का शमन कर जीवन की व्यापक सच्चाई को ग्रहण किया गया है। डॉ. धर्मवीर भारती के शब्द हैं- “किशोरावस्था के प्रणय, रूपासक्ति, और आकुल निराशा से एक आत्मसमर्पणमयी वैष्णव भावना और उसके माध्यम से अपने मन के अहं का शमन कर अपने से बाहर की व्यापक सच्चाई को हृदयंगम करते हुए संकीर्णताओं और कट्टरता से ऊपर एक जनवादी भाव-भूमि की खोज, मेरी इस छंद-यात्रा के यही प्रमुख मोड़ रहे हैं।”1 वस्तुतः धर्मवीर भारती ने धर्म, दर्शन, समाज की शोषित करने वाली रूढ़ि, मृत परम्परा व सड़े-गले मूल्यों को चुनौती दी है, अशिव को जन्म देने वाली मान्यताओं के प्रति अनास्था बरती है, किंतु मानवतावादी पक्षों को ध्यान में रखकर आस्था व विश्वास को भी उसी निष्ठा से सृजित किया।
डॉ. भारती अपनी प्रखर मेधा का परिचय देते हुए ‘अंधायुग’ में महाभारत के मिथकीय आवरण में समकालीन युद्धजनित समस्याओं का बखूबी चित्रण ही नहीं किया, बल्कि निजी अनुभूति को व्यापक सत्य के रूप में प्रकट किया । ‘अंधायुग’ कृति के रचनागत उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए वे लिखते हैं- “......... इस कृति का पूरा जटिल वितान जब मेरे अंतर में उभरा तो मैं असमंजस में पड़ गया । थोड़ा डर भी लगा । लगा कि इस अभिशप्त भूमि पर एक कदम भी रक्खा कि फिर बचकर नहीं लौटूँगा।”2 परन्तु रचनाकार अपने दायित्व से विमुक्त नहीं हो सकता, इसीलिए वे आगे लिखते हैं- “पर एक नशा होता है- अन्धकार के गरजते महासागर की चुनौती को स्वीकार करने का, पर्वताकार लहरों से खाली हाथ जूझने का, अनमापी गहराइयों में उतरते जाने का और फिर अपने को सारे खतरों में डालकर आस्था के, प्रकाश के, सत्य के, मर्यादा के कुछ कणों को बटोर कर, बचाकर, धरातल तक ले आने का।”3
कविवर डॉ. भारती प्राचीनता के अर्वाचीन शिल्पी माने जाते हैं। ‘कनुप्रिया’ में राधा के चरित्र को व्यापक व्यक्तित्व का रूप प्रदान कर युगीन संदर्भों में ढालकर प्रस्तुत किया है; जहाँ समस्याओं का समाधान है। दूसरी ओर ‘सातगीत वर्ष’ की कविताओं में आधुनिक जीवन का यथार्थ, जिसमें टूटन, घुटन, निराशा, निरर्थकता, पराजय आदि भावों का स्वाभाविक चित्रण तो हुआ है, पर आशा, उत्साह, दृढ़ता व साहस के साथ सृजनधर्मी रहने का संदेश भी है। कवि की मान्यता यह रही है- “साहित्य में शब्द तभी समर्थ, प्रेषणीय और प्राणवान बनते हैं, जब उनमें मानवीय मूल्य आन्तरिक रूप से प्रतिष्ठित रहता है।”4 यही आस्था भाव कवि को सृजनात्मक धर्म की ओर प्रेरित तो करता है, पर अंतस् में निहित व्याकुलता द्वंद्व को जन्म देती है । जो कवि संक्रमणकालीन परिस्थितियों और विसंगतियों का द्रष्टा हो, वह अपने भावों को निश्चित रूप से इन्हीं शब्दों में प्रकट करेगा-
तुमने कब झेली संक्रांति / तुम क्या समझोगे ओ प्रभु !
इन गत्यवरोधों का दर्द / कैसे तरूणाई में ही /
घुट भर जाते हैं विश्वास / प्राणों की समिधाएँ
जमकर हो जाती हैं सर्द!”5
‘अंधायुग’ में ‘कृष्ण’ का चरित्र जिस रूप में प्रकट हुआ है, उस बारे में कतिपय आलोचकों का मत है कि भारती जी ने भारतीय संस्कृति में कृष्ण के प्रति आस्था को कम कर दिया है, किंतु गहराई से दृष्टिपात करें तो यह प्रकट होता है कि कृष्ण की मृत्यु अश्वत्थामा के अनास्था भाव को समाप्त कर देती है । उक्त पंक्तियाँ अवलोकनीय हैं-
सुनो मेरे शत्रु, कृष्ण सुनो
मरते समय क्या तुमने इस नर पशु अश्वत्थामा को
अपने ही चरणों पर धारण किया
अपने ही शोणित से मुझे अभिव्यक्त किया?”6
भारती के कवि से ‘ध्वंस में पड़ मूर्च्छित जिंदगी’ को बहुत आशाएँ हैं। कवि ने आस्था, सृजन, उत्थान व विश्वास के इतने सहानुभूतिपूर्ण गीत गाये कि अन्तर आलोकित कर देते हैं। कवि की मानवतावादी चेतना भी क्रियात्मक एवं रचनात्मक शक्ति रखती है। कुंठा, आकुलता, हिंसा, विकृति, रक्तपात और बर्बरता में भी कृष्ण का यह आश्वासन सृजन का संदेश देता है, यथा-
मर्यादायुक्त आचरण में / नित नूतन सृजन में /
निर्भयता के / साहस के / ममता के / रस के /
क्षण में / जीवन और सक्रिय हो उठूंगा मैं बार-बार।7
‘सात गीत वर्ष’ में संकलित ‘प्रमथ्यु गाथा’ का नायक अग्निवाहक, अकेला चलने वाला, कांतिकारी और हुतात्मा है, परंतु जनसाधारण भीरू, भाग्यवादी और शक्तिहीन है। उनके कल्याण के लिए प्रमथ्यु अपने प्राणों की बाजी लगा देता है, उसका यह कर्तृत्व आशावादी दृष्टि पर ही आधारित है, यथा-
उनमें से एक-एक के अन्दर /
मूर्च्छित प्रमथ्यु कहीं बन्दी है।
अवसर जिसे मिला नहीं साहस कर पाने का /
कोई तो ऐसा दिन होगा / जब मेरे ये पीड़ा-सिक्त स्वर /
उसके मन को वेध मुर्च्छित प्रमथ्यु को जगायेंगे।8
‘कौन चरण’ नामक कविता में कवि उस आधार की तलाश कर रहा है, जहाँ वह अपने टूटे मन के तारों को जोड़ सके । आस्था भाव उसे अभी तक अप्राप्य है । उसको पाने की आकुलता भी स्पष्ट है । आरंभ में कवि ‘ऐसे कोई भी नहीं चरण’ कहकर निराशा व अनास्था से अपने मन को भर लेता है, किंतु अंत में वह फिर अपने लक्ष्य भ्रष्ट मन को आस्था भाव से भर लेता है और कहता है-
‘आखिर होंगे वे यही चरण
जिसमें इस लक्ष्य भ्रष्ट मन को
मिल पाएगी अन्त में शरण ।’9
महाभारत की कथा में वर्णित अभिमन्यु के रथ का ‘टूटा पहिया’ कवि की दृष्टि में टूटे हुए मन का प्रतीक बन गया है । आधुनिक संदर्भ में वह व्यक्ति जो अन्याय के सामने नतमस्तक है, शौर्यहीन है, उसके लिए यह टूटा व्यक्ति भी नवीन युग के निर्माण का आश्रय बन सकता है, इन संभावनाओं के मध्य कवि की आस्थावादी दृष्टि इस तरह प्रकट की है-
“मैं रथ का टूटा पहिया हूँ / लेकिन मुझे फेंको मत /
क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में / अक्षौहिणी
सेनाओं को चुनौती देता हुआ / कोई दुस्साहसी अभिमन्यु
आकर घिर जाये / बड़े-बड़े महारथी / अपने पक्ष
को असत्य जानते हुए भी / निहत्थी अकेली आवाज़को /
अपने ब्रह्मास्त्रों से कुचल देना चाहें /
तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया / उनके हाथों में ब्रह्मास्त्रों से
लोहा ल सकता हूँ ।”10
‘कनुप्रिया’ में राधा-कृष्ण का प्रेम शाश्वत नर-नारी का प्रेम बन गया है, जो काल की सीमा से परे है । पौराणिक होते हुए भी यह प्रणय-गाथा आधुनिक मन की दिव्यताओं और तन्मयताओं को अभिव्यक्ति देती है । कवि का निष्कर्ष यह है कि प्रेम की दुनिया को उजाड़ने वाला, अमानुषिक घटनाओं को जन्म देने वाला ‘युद्ध’ कभी भी मानव-जाति का भला नहीं कर सकता। कनुप्रिया अपने ‘कनु’ से प्रश्न करती है-
धारा में बह-बह कर आते हुए, टूटे रथ / जर्जर पताकाएँ किसकी हैं? /
हारी हुई सेनाएँ, जीती हुई सेनाएँ / नभ को कँपाते हुए,
युद्ध घोष, क्रन्दन-स्वर / भागे हुए सैनिकों से सुनी हुई ।
अकल्पनीय अमानुषिक घटनाएँ युद्ध की / क्या ये सब सार्थक हैं ?”11
‘अंधायुग’ में प्रभु अपने अवसान के क्षणों में जब ध्वंस का दायित्व अपने ऊपर लेते हैं तो भविष्य की कल्पना भी रखते हैं। आस्था का प्रश्न संजय, युयुत्सु और अश्वत्थामा के माध्यम से कवि ने प्रस्तुत किया है और अनास्था को आस्था की भूमिका के रूप में स्वीकार किया है। विदुर का निवेदन इसी का प्रमाण है-
यह कटु निराशा की / उद्धत अनास्था है / क्षमा करो प्रभु। /
यह कटु अनास्था भी अपने / चरणों में स्वीकार करो । /
आस्था तुम लेते हो / लेगा अनास्था कौन ?”12
आस्था और अनास्था के द्वंद्व में भी कवि का समष्टि भाव ही अधिक मुखर रहा है। ‘अंधायुग’ में युयुत्सु का चरित्र आस्था के प्रति अनास्था भाव को प्रकट करने वाला है, वहीं कृष्ण की मृत्यु पर अश्वत्थामा का आस्थावान् बन जाना अपूर्व है। ‘प्रमथ्यु गाथा’ में प्रमथ्यु का आत्मबलिदान जनसाधारण को चेतनावान बनाने का संदेश देता हे, तो ‘कनुप्रिया’ युद्ध के ध्वंस का विरोध करती है । आम आदमी की पीड़ा, संत्रास, तिरस्कार और उपेक्षा के बीच कवि का स्वर लघु मानव की शक्ति को आस्थावादी दृष्टि से देखने का रहा है। कवि की उक्त पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-
“हम मनुष्य बौना है, लेकिन / मैं बौनों में बौना ही बनकर
रहता हूँ / हारो मत, साहस मत छोड़ो / इससे भी अथाह शून्य में /
बौनों ने ही तीन पगों में धरती नापी ।”13
समग्रतः डॉ. धर्मवीर के काव्य में युगीन विद्रुपताओं, वेदना व पीड़ा की गाथाओं, युद्ध जनित विषमताओं, मानवता को त्रास पहुँचाने वाली कई घटनाओं के चित्रण के बावजूद वे अपनी आस्था का स्वर कभी ‘लघुमानव’ में तलाश करते हैं, तो कभी अश्वत्थामा के हृदय परिवर्तन में। ‘कनुप्रिया’ के कांत सम्मित उपदेश में यही दृष्टि दिखाई देती है । इस संपूर्ण रचना-प्रक्रिया में आस्था और अनास्था के द्वंद्व में आस्थावादी दृष्टि का आकर्षण- पाठकों को सदैव आकर्षित करता है और भावी मूल्यों के निर्माण की प्रेरणा भी देता है ।
संदर्भ
- ठंडा लोहा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 1998, भूमिका
- अंधायुग, किताब महल, नई दिल्ली, सं. 1914, भूमिका
- वही, भूमिका
- मानव मूल्य और साहित्य, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 1999, पृ.177
- सात गीत वर्ष, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, सं. 1956, पृ.43
- अंधायुग, किताब महल, नई दिल्ली, सं. 1914, पृ.123
- वही, पृ.128
- सातगीत वर्ष, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, सं. 1956, पृ.24
- वही, पृ.82
- वही, पृ. 79-80
- कनुप्रिया, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 2013, पृ.73-74
- अंधायुग, किताब महल, नई दिल्ली, सं.1914, पृ.19
- सात गीत वर्ष, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, वाराणसी, सं. 1956, पृ.124