नई सदी के हिंदी उपन्यासों में आदिवासी जीवन के अनुत्तरित प्रश्न
(समवेत जनवरी-जून,2023 में प्रकाशित)
संविधान की पंचम अनुसूची में आदिवासी समुदाय को 'जनजातियाँ' शब्द से परिभाषित किया है। इन्हें वनवासी, आत्विका, गिरिजन, वन्यजाति या आदिमजाति भी कहा जाता है। इस वर्ग को जेकब्स तथा स्टर्न ने इस तरह परिभाषित किया है, “एक ऐसा ग्रामीण समुदाय या ग्रामीण समुदायों का ऐसा समूह जिसकी समान भूमि हो, समान भाषा हो, समान सांस्कृतिक विरासत हो और जिस समुदाय के व्यक्तियों का जीवन आर्थिक दृष्टि से एक दूसरे के साथ ओतप्रोत हो, जनजाति कहलाता है।“1 भारत में अनेक जनजातियाँ हैं, जिन्हें सात विभागों में चिह्नित किया जाता है- उत्तर, पूर्वोत्तर, पूर्वी, मध्य, पश्चिम, दक्षिण और द्विपीय क्षेत्र। आदिवासियों का अपना धर्म है, वे प्रकृति पूजक हैं। उनमें से कुछ लोगों ने हिंदू, ईसाई, बौद्ध एवं इस्लाम धर्म भी अपनाया है। भारत में प्रमुख रूप से भील, गोंड, संथाल, मीजी, असुर, न्यीशी, हो, गालो, मोमपा, तागीन, खामती, मेमबा, नाक्टे, कंजर, कबूतरा, आपातानी, मुंडा, सांसी, नट , मदारी, सँपेरे, दरवेशी, पासी, बोरी, समोड, कोल, पादाम, मिन्योंग, देववर्मा, रियाँग, नोवतिया, उचई, चाकमा, डोंबारी, कोली, पारधी, मीणा, आन्गे, गरसिया, सहरिया, लेपचा, थारू, उराँव, भवघूरा, बोंडा आदि जनजातियाँ आदिवास करती हैं, जिन्हें आदिवासी कहा जाता है। ऐसे अनेक आदिवासियों को केंद्र में रखकर भारतीय स्तर पर अनेक भाषाओं में साहित्य लिखा जा रहा है।
आदिवासी साहित्य की अवधारणा के सम्बन्ध में कुछ विद्वान आदिवासी विषय पर लिखा गया साहित्य इस श्रेणी में मानते हैं तो कुछ जन्मना और स्वानुभूति के आधार पर आदिवासियों द्वारा लिखे गए साहित्य को ही आदिवासी साहित्य मानते हैं। एक अवधारणा उन आदिवासी लेखकों की है, जो ‘आदिवासियत’ के तत्वों का निर्वाह करने वाले साहित्य को ही आदिवासी साहित्य के रूप में स्वीकार करते हैं। ऐसे लेखकों और साहित्यकारों के भारतीय आदिवासी समूह ने 14-15 जून 2014 को रांची में आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार में इस अवधारणा को ठोस रूप में प्रस्तुत किया, जिसे ‘आदिवासी साहित्य का रांची घोषणा-पत्र’ के तौर पर जाना जा रहा है और अब वह आदिवासी साहित्य विमर्श का केन्द्रीय बिंदु बन गया है। इसके अनुसार, "आदिवासियों की आदिवासियत को न तो आप वर्गीकृत कर सकते हैं न ही किसी मानक से नाप सकते हैं, क्योंकि यह तो विरासत में मिला हुआ वह गुण है, जिसे कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता और न ही इसे कोई खारिज कर सकता है। किसी व्यक्ति की आदिवासियत को आप इस बात से भी नहीं तय कर सकते हैं कि उसमें आदिवासी खून कितना है।"2 हिन्दी की विविध विधाओं में आदिवासी जीवन को विषय बनाया गया है, उसमें उपन्यास विधा में अधिक गहराई दिखाई देती है।
आदिवासी जीवन आधारित हिन्दी उपन्यासों का जब अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि उपन्यासकारों ने उन पहलुओं को उजागर किया है, जिन पर अब तक किसी ने प्रकाश नहीं डाला था। हिंदी उपन्यासकार स्पष्ट करते हैं कि आजादी बाद भी इन्हें उपेक्षितों का जीवन जीना पड़ रहा है। उन्हें यहाँ की समाज व्यवस्था ने हाशिये पर रखकर आज भी आदिम रूप में जंगलों में रहने के लिए बाध्य किया है। यह एक सुखद संयोग है कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर भारतीय गणतन्त्र के सर्वोच्च पद पर आदिवासी प्रतिनिधित्त्व है, इससे यह प्रतीत होता है कि इस वर्ग की ओर अब लोगों का ध्यान गया है। यह सत्य है कि समाज की मुख्य धारा से विस्थापित आदिवासी समुदाय की आवाज को साहित्य ने पूर्ण तटस्थता से व्यक्त किया।
नई सदी में जो उपन्यास आदिवासी जीवन पर केन्द्रित हैं, उनमें प्रमुख हैं- मंगल सिंह मुंडा कृत ‘छैला संदु’, प्रतिभा राय का ‘आदिभूमि’, विनोद कुमार रचित ‘समर शेष है’, श्रीप्रकाश मिश्र लिखित ‘जहाँ बांस फूलते हैं’, राजीव रंजन का ‘आमचो बस्तर’, रणेंद्र कृत ‘ग्लोबल गाँव का देवता’ व ‘गायब होता देश’, हरीराम मीणा का ‘धूणी तपे तीर’, तेजिंदर गगन रचित ’काला पादरी’, भगवानदास मोरवाल का 'रेत', राकेश कुमार का ‘पठार पर कोहरा’, महुआ माझी का ‘मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ’ आदि महत्त्वपूर्ण हैं। इन उपन्यासों में आदिवासी जीवन के अनेक पहलुओं को उजागर किया है। निस्संदेह आदिवासी लेखन से आधुनिक सभ्य समाज के समक्ष ऐसे प्रश्न उपस्थित हुए हैं, जिनका उत्तर दिया जाना शेष है।
आधुनिक सभ्यता की देन है- भूमंडलीकरण। रणेन्द्र का उपन्यास 'ग्लोबल गाँव के देवता' झारखंड के 'असुर' जनजातियों के शोषण, विस्थापन को उजागर करता है । आज वैश्वीकरण के इस युग में एक ओर हम विकास कर रहे हैं तो दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का अमर्यादित उपयोग करके प्रकृति को दूषित कर रहे हैं । वहाँ के आदिवासियों, वनवासियों को उनके जंगलों से खदेड़ रहे हैं । इन्हीं अमानवीय बातों को रणेन्द्र ने इस उपन्यास में अभिव्यक्त किया है । ‘ग्लोबल गाँव के देवता’ असुरों का वैश्विक परिप्रेक्ष्य पेश कर उसका इतिहास प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ इस भूमण्डलीकरण के दौर में उनकी सांस्कृतिक पहचान के ऊपर हो रहे हमलों को भी उद्घाटित करता है। उपन्यास की एक पात्र ललिता के शब्दों में असुर संस्कृति को समझा जा सकता है, वह कहती है, “हमारे महादनिया महादेव वह नहीं हैं, लंगटा बाबा के है। हमारे महादेव यह पहाड़ है, जो हमें पालता है। हमारी सरना माई न केवल सखुआ गाछ में बल्कि सारी वनस्पतियों में समाई है। हम सारे जीवों से अपने गोत्र को जोड़ते है। छोटे जीवों, कीट-पतंगों को भी अपने से अलग नहीं समझते। हमारे यहाँ ‘अन्य’ की अवधारणा नही है जिस समाज के पास इतनी बड़ी सोच हो उसे किसी लंगटा बाबा या किसी और की शरण में जाने की जरूरत ही क्या है?‘‘3 इस उपन्यास में वैश्वीकरण, औद्योगीकरण के कारण आदिवासी आदिवासियों पर हो रहे अन्याय-अत्याचार को भी व्यक्त किया है। उपन्यासकार लिखते हैं कि आकाशचारी देवताओं को जब अपने आकाशमार्ग से या सेटेलाईट की आँखों से छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, झारखंड आदि राज्यों की खानिज सम्पदा, जंगल और अन्य संसाधन दिखते हैं तो उन्हें लगता है कि राष्ट्र-राज्य तो वे ही हैं, तो हक तो उनका ही हुआ । सो इन खनिजों पर, जंगलों में, घूमते हुए लँगोट पहने असुर-बिरिजिया, उराँव-मुंडा आदिवासी, दलित-सदान दिखते हैं तो उन्हें बहुत कोफन होती है। वे इन कीड़े-मकोड़ों से जल्द निजात पाना चाहते हैं।
औपनिविशिकता का दंश भारतीय समाज अच्छी तरह से जानता है, परन्तु आदिवासियों ने इसका जिस तरह से सामना किया है, वह एक दारुण यथार्थ है। तेजिन्दर का 'काला पादरी' मध्यप्रदेश की 'उराँव' जनजाति की समस्याओं को व्यक्त करने वाला उपन्यास है। उपन्यास में भूख मिटाने के लिए जहरीली वनस्पतियाँ, बूटियाँ और बिल्लियों का मांस खाने का वास्तव सामने रखा। प्रो. चमन लाल गुप्ता के समालोचनात्मक शब्द है, ''वास्तव में 'काला पादरी' उपन्यास में भारत के सर्वाधिक उत्पीड़ित व उपेक्षित आदिवासियों की जीवन स्थितियों के अनेक पहलुओं को लेखक ने समाजशास्त्रीय दृष्टि, किन्तु साथ ही लेखकीय संवेदना से इस ढंग से चित्रित किया है कि भारतीय समाज की जटिलता भी उभरकर सामने आती है और साथ ही आदिवासियों के जीवन की पीडा का मार्मिक अंकन भी लेखक की कलम से होता चलता है।''4 आदिवासी भूख, अभाव, दारिद्र्य, शोषण आदि से परेशान होकर ईसाई, हिन्दू, बौद्ध धर्म में दीक्षित होने के कारकों की ओर भी संकेत करता है। आदिवासियों के भूख, अभाव और दारिद्र्य को व्यक्त करता हुआ वह लिखता है, ''साहब रात में बच्चा मर गया। उसकी माँ ने कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। उसको गोद में लेकर उसकी माँ भी मर गयी। उसने भी कई दिनों से कुछ खाया नहीं था।'5' उपन्यासकार आदिवासियों का औपनिवेशिक व्यवस्था में फँसे होने का कारुणिक यथार्थ सामने रखता है। इसी तरह महुआ माझी का 'मरंगगोडा नीलकंठ हुआ' झारखंड के 'हो' आदिवासी जनजाति को केन्द्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है । इस उपन्यास में मुख्यतः अणु-परमाणु, नाभिकीय ऊर्जा के आदिवासी जीवन पर हो रहे दुष्परिणामों की ओर ध्यान खींचा है। यह विवशता उत्तर मांगती है ।
सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार हमारे समय का सच है। आदिवासी जीवन तो वैसे भी नगरीय जीवन की कारगुजारियों से अनभिज्ञ है, ऐसी स्थिति में उसका शोषण सहज है, वह सामने भी नहीं आ पाता। ‘पठार पर कोहरा' झारखंड के 'मुंडा' आदिवासियों की करुण कथा है। राजीव गांधी की सरकारी योजनाओं के बारे में दस प्रतिशत वाली बात को उपन्यासकार आदिवासियों की योजनाओं में हो रहे भ्रष्टाचार के रूप में इस प्रकार व्यक्त करता है, ''आजादी के बाद आदिवासियों की कल्याण की सैंकड़ों योजनाएँ बनी हैं पर उनके क्रियान्वयन का क्या हुआ? आबंटित राशि का दस प्रतिशत भी देश के आदिवासियों तक नहीं पहुँच रहा है। कई योजनाएँ कागज पर चलती रहती हैं। कई योजनाएँ तो फाइलों की कब्र में ही दफन हो गयी... यदि अफसरशाही और राजनीति का यही तालमेल कायम रहा तो पता नहीं कितने समय तक आदिवासी समाज इसी तरह अपढ़, असंस्कृत, भूखा, नंगा, शोषित, उपेक्षित और लोकतंत्र के ज्ञान एवं विज्ञान से कटा रहेगा।''6 राकेशकुमार सिंह ने आजादी के बाद भी आदिवासियों के जीवन समस्याओं का कोहरा न हटने की बात उपन्यास में की है। उपन्यास में सरकारी योजनाओं के भ्रष्टाचार का भंडा-फोड़ किया है। यह त्रासद स्थिति कब सुधरेगी, विचारणीय है।
प्रतिभा राय का 'आदिभूमि' यह उपन्यास उडीसा के आदिवासी 'बोंडा' जनजाति पर लिखा गया है। यह उपन्यास बोंडा के जीवन-व्यवहार, हिंसा, प्रतिहिंसा, प्रतिरोध, सरलता, लोकरूढि, लोकविश्वास, स्त्री-पुरुष संबंध, स्त्री-शोषण आदि को सशक्त रूप में उजागर करता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भी इनके शोषण का सिलसिला जारी होने के सत्य को प्रतिभा राय उजागर करती हैं। इस उपन्यास में सरकारी योजनाओं- इंदिरा आवास योजना, साक्षरता आदि की धोखाधडी, झूठ-फरेब, भ्रष्टाचार, स्त्रियों का यौन शोषण आदि को प्रकट किया है। उपन्यास में शिक्षा के प्रति आदिवासियों की रूचि बढ़े इसलिए मास्टर सीतानाथ के माध्यम से उपन्यासकार अपनी बात रखती हैं। आदिवासी इलाकों में समाज सुधार करना आसान नहीं है, क्योंकि कई लोगों के स्वार्थ वहाँ पर अटके हुए होते हैं । उनमें प्रशासक बी. डी. ओ., पुलिस, राजनेता, एम. एल. ए. जैसों का समावेश होने की बात उपन्यासकार करती हैं। आलोचक कृष्णचंद्र गुप्त लिखते हैं, “उपन्यास का सीतानाथ अपनी निष्ठा के बल पर इस जंगली झुंड को 'आदमी' बनाने पर तुला हुआ है।''7 किंतु अवसरवादी उनका तबादला दूसरी जगह कर देते हैं । इस प्रकार आदिवासी जीवन समस्याओं के साथ-साथ प्रकृति की सम्पन्नता को भी उपन्यासकार प्रतिभा राय उजागर करती हैं।
इसमें आदिवासी इतिहास के प्रति उपेक्षा ने कई पहलुओं को प्रकट नहीं होने दिया, जिससे सांस्कृतिक तत्त्वों का सम्यक विश्लेषण अधूरा ही रहा। रणेंद्र का दूसरा उपन्यास है- ‘गायब होता देश’ इसमें मुंडा आदिवासी समुदाय के शोषण को रेखांकित किया गया है। इसके साथ ही लेखक ने मुंडाओं की सांस्कृतिक-ऐतिहासिक विवरण को भी भावपूर्ण तरीके से उकेरा है।उपन्यास के प्रमुख पात्र सोमेश्वर के माध्यम से लेखक का कथन है- “लेकिन इतना तो तय है किलेमुरिया समुद्र में प्रकट हुआ, पुनः समुद्र में डूब गया, लेकिन नए युग के उदय के साथ वह पुनः प्रकट होगा।“8 इसमें बताया गया है कि मुण्डाओं को अपने देश से कितना प्यार है, यह उनके शब्दों में ‘सोने जैसा देश’ से प्रकट हो जाता है और वही सोने जैसा देश गायब होता जा रहा है जिसका दर्द सोमेश्वर कि शब्दों से उभरती मर्मान्तक चीज को सुनकर जाना जा सकता है ‘‘थोड़ी देर के लिए सोचिए बच्चू! अगर लुटियन दिल्ली के नीचे कोयला निकल आये, इलाहाबाद सिविल लाइन्स के नीचे बाक्साइट, यूरेनियम चण्डीगढ के नीचे आयरन, लखनऊ, चेन्नई, बेंगलुरू के नीचे तो क्या उजाडेगा लोग उसे? होगा वहाँ विस्थापन? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि वहाँ रहने वाले एलीट सम्माननीय नागरिक हैं। भारत माता के अपने खास बेटे। फिर हम क्या हैं? केवल लाभुक, कोई टार्जेट ग्रुप या फिर किसी शोध के लिए एक ठोस केसर। क्या हैं हम? क्या मुआवजा के रजिस्टर के बस एक नम्बर, या कि कल्याण विभाग के फाइल की फटी हुई झोली, फादर हाफमैन, वरियर एल्विन जैसो की किताबों की ब्लैक एण्ड व्हाइट तस्वीरें। क्या हैं हम? सच बात है कि उनकी नजर में हम हैं ही नहीं। फिर यह हमारी साँस लेती हुई जिन्दगी क्या है? क्या हम आपके सौतेले बेटे हैं भारतमाता।’’9 आदिवासियों का विस्थापन और उसके साथ मिट्टीकी गंध को कौन लील रहा है, सोचना होगा।
आदिवासी स्त्री की करुण गाथाएँ भी इन उपन्यासों में प्रकट हुई है, जब पुलिस, प्रशासन आदि भी उनके साथ अत्याचार करते हैं। भगवानदास मोरवाल का 'रेत' उपन्यास हरियाना के 'कंजर' जनजाति के सामाजिक-सांस्कृतिक संरचनाओं को प्रस्तुत करता है। 'कंजर' अर्थात् काननचर याने जंगल में घूमनेवाले। प्रस्तुत उपन्यास एक ओर आदिवासी विमर्श की कृति है, तो दूसरी ओर आदिवासी स्त्री विमर्श की भी कृति है। सामान्य तौर पर कंजरों को (जरायमपेशा) चोरी करनेवाली जनजाति समझा जाता है। अंग्रेज सरकार ने इन पर कई बंधन डाल दिये थे जिसे उपन्यासकार ने थानेदार केसर सिंह के माध्यम से कहलवाया है। केसर सिंह कबीले के मुखिया से कहता है, ''यही कि बिना इजाजत या इत्तिला दिए कोई कंजर गाँव छोड़कर नहीं जा सकता ...और जाता है तो मुखिया को इसकी जानकारी होनी चाहिए, जिसकी इत्तिला मुखिया को थाने में देनी होती है।''10इनकी महिलाओं को भी थाने जाकर हाजरी देनी पड़ती है। घर के पुरूष जेल में या बाहर होने के कारण इन्हें मजबूरी वश वेश्या-व्यवसाय करना पड़ता है। इन्हीं बातों को उपन्यासकार ने बडी स्पष्टता से उपन्यास में रखा है। नई सदी में भी में भी इन दृश्यों की उपस्थिति विचलित करती है।
संक्षेप में कहा जा सकता है कि आदिवासी लेखन में उपन्यासकारों ने कुछ ऐसे चित्र उपस्थित किए हैं जो सभी समाज के विपरीत है । जब कभी मानव सभ्यता चाँद को छूने के लिए ब्रम्हांड को चीरती है तब ये चित्र मानव को आदिम युग में ले जाते है, जो शर्मनाक है। मनुष्यता के कलंक से विमुक्ति का प्रयास आदिवासी जीवन के प्रति एकात्म भाव से ही संभव है, अन्यथा विकास की गति केवल छलावा है। हिन्दी उपन्यास परम्परा का अवदान इस दृष्टि से स्तुत्य है।
सन्दर्भ-
1.डॉ. लक्ष्मणप्रसाद सिन्हा, भारतीय आदिवासी, जय भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2010, पृष्ठ 88)
2.वेब पेज https://hi.wikipedia.org/wiki
3.रणेन्द्र, ग्लोबल गाँव के देवता, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 2014, पृष्ठ 72
4.प्रो. चमनलाल, दलित साहित्य: एक मूल्यांकन, राजपाल एंड संस, सं. 2012 पृष्ठ 166
5.तेजिन्दर, काला पादरी, नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, सं. 2004, पृष्ठ 21
6.राकेशकुमार सिंह, पठार पर कोहरा, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 2003,पृष्ठ 137
7.कृष्णचंद्र गुप्त - 'बोंडा जाति का औपन्यासिक समाजशास्त्र', हंस, फरवरी, 2002, पृष्ठ 88
8.रणेंद्र, गायब होता देश, पेग्विन इंडिया, नई दिल्ली, सं. 2014, पृष्ठ 131
9.रणेंद्र, गायब होता देश, पेग्विन इंडिया, नई दिल्ली ,सं. 2014, पृष्ठ 263
10.भगवानदास मोरवाल, रेत, राजकमल प्रकाशन, सं. 2009, पृष्ठ 51
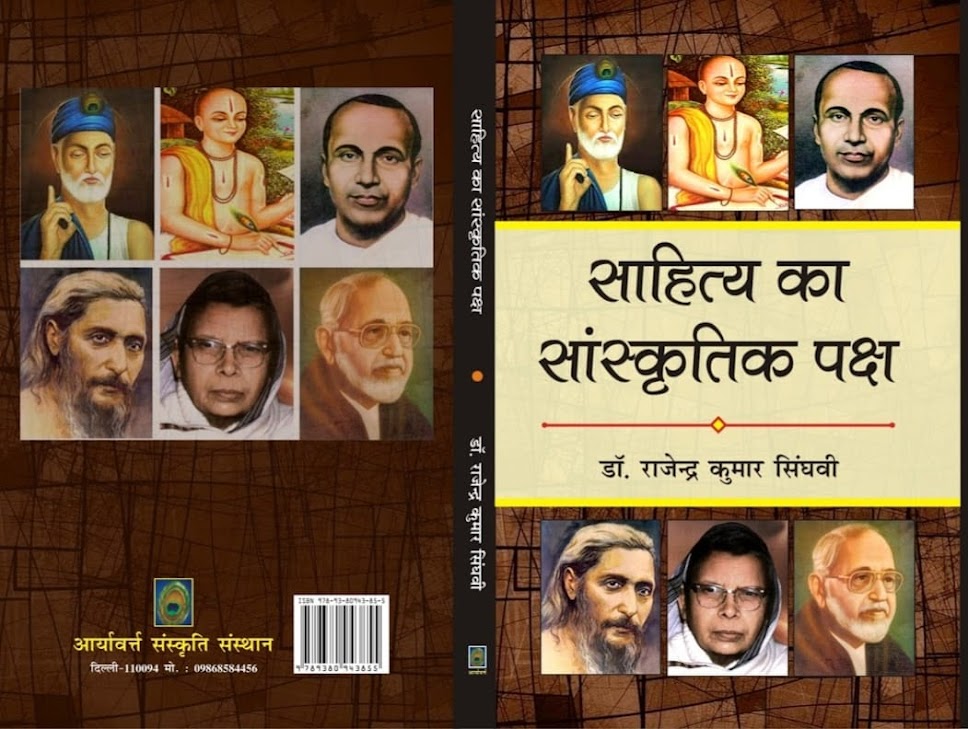
No comments:
Post a Comment