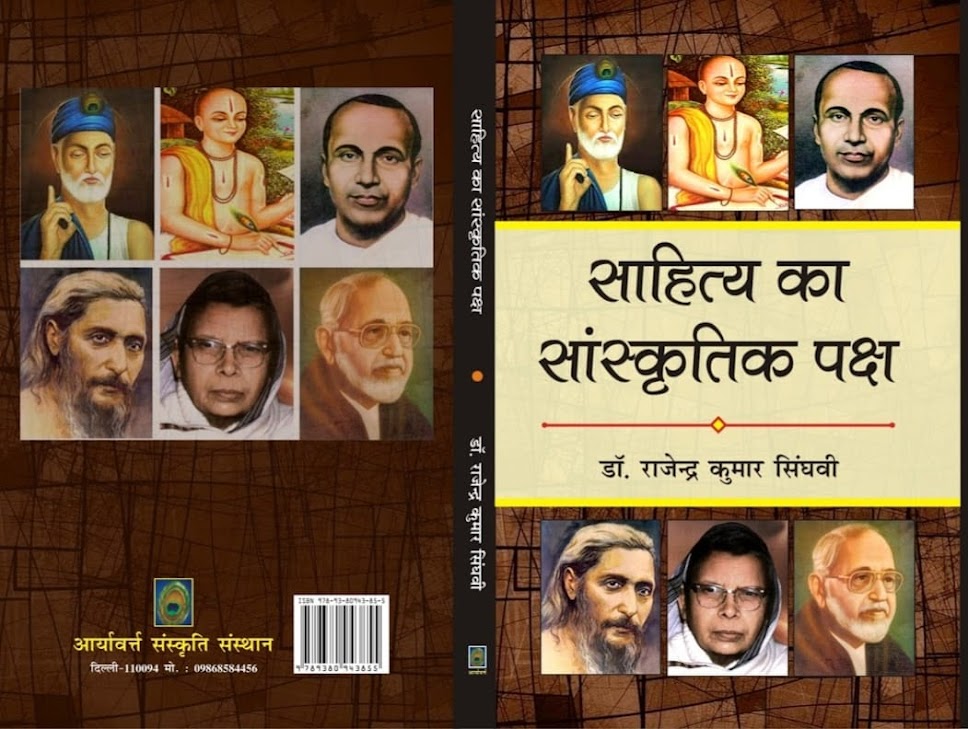|
| विजया बुक्स, 1/ 10753, सुभाष पार्क, गली नं 3, नवीन शाहदरा, दिल्ली 110032 |
कविवर नन्द भारद्वाज का सध्य प्रकाशित काव्य-संग्रह ‘आदिम बस्तियों के बीच’ वस्तुतः आदमी को तलाश करता प्रतीत होता है । रेतीले धोरों के बीच कवि ने अपना बचपन सँवारा और उदारीकरण की आर्थिक जीवन शैली में आज वह नगरीय जीवन का हिस्सा बन गया । यह कहानी हर मध्यमवर्गीय परिवार की हो सकती है । इस काव्य संग्रह में कवि का अतीत बार-बार उसे आदिम ग्रामीण जीवन शैली से जोड़ता है, जबकि कवि यह जानता है कि इस आदिम ग्रामीण जीवन शैली से मेरा जुड़ा होना न खूबी है न कैफियत । इसके बावजूद कवि को यह अहसास है कि साहित्य और संस्कृति को लेकर ऊपरी तौर पर वहाँ कोई स्वरूप या संकेत नहीं दिखाई देते, लेकिन उन संस्कारों की जड़ें उनमें गहरे पैठी है ।
कवि भारद्वाज अपने इन्हीं संस्कारों के कारण कभी अपने बचपन के घर की यादों में खो जाते हैं, कभी माता-पिता व सहोदर से संवाद कायम करने की कोशिश करते हैं तो कभी अपने बच्चों व पत्नी के प्रति दायित्व बोध को समझकर किंकर्तव्यमूढ़ भी बन जाते हैं । अपनों की तलाश में कवि की कुल अड़तीस रचनाएँ इस काव्य-संग्रह में है, जिसे आधुनिक मानव की मर्मभरी अन्तःपीड़ा माना जा सकता है जो आर्थिक बाजारीकरण से संघर्ष करती अपनी जड़ों की तलाश में है ।
 |
| डॉ. नन्द भारद्वाज |
कवि का अभिमत है- रचना के भीतर मूर्त होता जीवन-यथार्थ, उसमें अन्तर्निहित मानवीय सरोकार और उसके लक्षित पाठक वर्ग से बनता रिश्ता ही यह तय कर पाता है कि कविता उसकी जीवन-प्रक्रिया में कितनी प्रासंगिक और प्रभावी रह गई है । कविता संग्रह की प्रथम कविता ‘अपना घर’ और अन्तिम कविता ‘आदिम बस्तियों के बीच’ है । जिसमें जीवन यात्रा के पड़ाव दृष्टिगोचर होते हैं । कवि अपने बचपन के उन क्षणों को याद कर विस्मृत होता है, जब वे बारिश से भीगी रेत को घरोंदे का आकार देते थे । उसमें मन चाहा आकार देते थे, जहाँ आयताकार ओरे, तिकोनी ढलवांसाल, अनाज की कोठी, बुखारी, गायों की गोर सब कुछ होती थी, पर चहार-दीवारी नहीं । पंक्तियाँ द्रष्टव्य हैं-
न जाने क्यों
वैसा अपना घर बनाते
अक्सर भूल जाया करते थे
घर को घेर कर रखने वाली
वह चहार-दीवारी ।
( अपना घर )
आर्थिक उदारीकरण के दौर में शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है और इस प्रक्रिया में सर्वाधिक नुकसान ‘संवेदना’ का हुआ है । जहाँ व्यक्ति अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है । उसके सामने बच्चों को अभावों से दूर रखने की कवायद है । इसी जुगत में दिनभर हाड़तोड़ मेहनत के बाद अपने घर-संसार में प्रवेश करते आज के मध्यमवर्गीय व्यक्ति का चित्र दृष्टव्य है-
यह खयाल रखते कि संध्या-काल
अंधेरा घिर आने से पहले
लौट जो आना है घर की ओर,
झाड़ते - बुहारते - सींचते
तमाम तरह के अभावों-
और अनहोनियों के बीच
थामे जो रहते थे अपनी जान से
कि कोई आँच न आये
बच्चों की नींद और उनके
सपनों में पलते घर - संसार में ।
(घर तुम्हारी छाँव में)
गाँवों से पलायन और शहरों में बस जाने पर भी जीवन में सहजता न होना आधुनिक मानव मन त्रासदी है । एक अजीब भय उसके मन में सदैव व्याप्त रहता है, शायद शहरी जीवन की यही चर्या भी है । इस मन को दुखाने वाली जीवन चर्या को अंगीकार करना उसकी नियति बन गई है और मजबूरी भी, यथा-
सिर्फ मैं ही नहीं जान पाता
इस जीवन-चर्या का सार,
बच्चे खुश हैं
अपनी बदलती दुनिया में,
और वह बनी रहती है
उन्हीं की इच्छाओं के पास,
वहीं से वह देख लिया करती है
हर असार में सार की संभावना ।
(जीवन-चर्या)
आर्थिक झंझावतों ने हमारी आकांक्षाओं की कमर तोड़ दी है । भावनाओं को केन्द्रित करना सीखा है और रिश्तों को भी ताक पर रख दिया है । हम सवालों से डरने लग गए हैं और अपेक्षा करते हैं कि जैसा चल रहा है उसे घर का हर सदस्य स्वीकार कर ले । यहाँ तक कि हमारी सहधर्मिणी के साथ भी अभावों की चर्चा करना मुनासिब नहीं समझते । यथा-
पत्नी अक्सर कुछ कहते कहते
रूक जाती है
और हमसे यह तक नहीं कहते बनता
कि वह अपनी बात कहे-
अपेक्षा करते हैं
जिस हाल में हैं, उसी में मौन रहे ।
( बहस से हटकर )
समय के साथ मानवता का भी पतन हुआ है और इंसानियत की हदें पार करते हुए मनुष्य हिचकता भी नहीं है । कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि चारों ओर आदमखोर घूम रहे हैं और हमारी साँसें सुरक्षित नहीं हैं । जीवन के पटल पर असुरक्षा भाव मनुष्यता को रिस-रिस कर मार रहा है । संशय की इसी परिधि में कैद मानवीय जीवन का परिदृश्य कवि ने बखूबी अंकित किया है-
धरती की छाती पर
लोटते रहे जहरीले सांप-
खूंखार भेड़िये और आदमखोर
अपने शिकार की तलाश में
भटकते रहे,
गाँव की सुनसान गलियों में
बे आवाज -
हर सांस अकेली और असुरक्षित है
हर घात अंधा और संशयहीन ।
(गर्म राख के नीचे)
शहरी जीवन में सन्नाटों की त्रासदी है, गलियाँ गमगीन हैं, बेखौफ़ अबोलापन है जो दूसरी ओर आत्मरक्षा में उठती आवाजें चीखती रहती हैं । अमन का आशियाना कभी बसता नज़र नहीं आता । कवि इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि-
और इस दिखाऊ दहशत के बिपरीत
शहर के भीतर तह में इकट्ठा हो रहा है
फिर वही बेखौफ अबोलापन-
वह डर जाया करती है
अमूमन पीछा करती
एम आदिम परछाई से,
और बदहवास होकर
रौंदने लगती है अमन का आशियाँ ।
(उसका अहसास)
अपने बीवी-बच्चों के साथ अनजान शहर में रहने वाला व्यक्ति अपनी अतीत की यादों को मन में सहेजता, पीड़ा भोगता मौन होकर क्यों स्वीकारता है? यह प्रश्न अनुत्तरित है । अपने बूढ़े पिता के संताप को जानकर भी उसका पुत्र उससे दूर क्यों भाग जाता है, कोई नहीं बता सकता । गाँवों में बूढ़े पिता का संताप आधुनिक जीवन शैली पर व्यंग्य के रूप में अभिव्यक्त हुआ है-
धड़कते हुए कलेजे में
संजोए रखना
एक अदद कुँआरी बेटी का अवसाद
और गुजारे की खोज में
परदेस गये दुलारों का
बेचैन बैठे इन्तजार करना ।
(बूढ़े पिता का संताप)
बदलते दौर में अपना भाई भी बेगाना लगता है । उससे संवाद की गुंजाईश खत्म हो गई है । वह हर पल अपने से दूर जाता दिखाई देता है और कभी-कभी लगता है कि अब शायद ही कभी अपने साथ आ पाए । अपना लाड़ला सहोदर और उसके बारे में अपनी पीड़ा का संवाद कवि के शब्दों में -
मैं चिन्तित और हैरान हूँ-
कितनी आसानी और
बिना किसी संकोच के
नेकी और ईमान से इतनी दूर
दुनियादारी के दलदल में
उतर जाते हैं मेरे सहोदर
जहाँ से आगे नहीं दीख पड़ती
कोई संवाद की संभावना ।
(सहोदर से संवाद)
समय के साथ समझौता करना माँ ने भी सीख लिया है, वह भी शिकायत नहीं करती । वत्सलता का सागर उमड़ाने वाली माँ आज आपसे कोई उम्मीद नहीं रखती । उसका आँचल यद्यपि आज भी ममता की छाँव है, पर उसे पता है कि वहाँ उसका लाल अब कभी आश्रय नहीं लेगा । आधुनिक जीवन का यह पहलू कवि के शब्दों में-
कहने को कुछ भी नहीं था पास उसके
न कोई शिकवा - शिकायत
न उम्मीद ही बकाया,
फकत् देखती भर रहती थी अपलक
हमारे बेचैन चेहरों पर आते उतरते रंग
हम कहाँ तक उलझाते
उसे अपनी दुश्वारियों के संग ।
(माँ की याद)
कवि इस आपाधापी के जीवन में मानवीय संवेदना के टूटते हुए दृश्य को रेखांकित करता है, जहाँ पीड़ाएँ अभिव्यक्त नहीं हो पाती । अन्तःकरण द्रवित होकर इस कगार पर आ पहुँचा है कि उसे मात्र एक ढाँचे के रूप में जीना है-
एक अवयव टूटकर बिखर गया है कहीं भीतर
लहू लुहान- सा हो गया है मेरा अन्तःकरण
पीड़ा व्यक्त होने की सीमा तक,
आकर ठहर गई है ।
(जो टूट गया है भीतर)
इंसान अपने दर्द की सकल पीड़ा को भोगते हुए भी जीवन की कोख में बना रहना चाहता है । वह जीवन से पलायन नहीं करता । एक अज़ब सी जिजीविषा उसे किंकर्तव्यविमूढ़ स्थितियों में आदिम बस्तियों के बीच बनाये रखने की कोशिश करती है, यथा-
 |
यह समीक्षा आलेख हाल में
'कथन'
जैसी लोकप्रिय साहित्यिक पत्रिका के
जनवरी-मार्च-2013 के अंक में छपा है।
|
ढांप ले फलक तक फैले
दीठ का विस्तार,
मुझे पानी और मिट्टी के बीच
बीज की तरह
बने रहना है इसी जीवन की कोख में ।
(आदिम बस्तियों के बीच)
समग्रतः कवि नंद भारद्वाज ने अपने अनुभव के आवेग में ‘आदिम बस्तियों के बीच’ रहते मानव की मनःस्थिति, बदलते परिवेश में उसका रूख और मौन यथार्थ की स्वीकारोक्ति को बहुत ही सहज ढंग से अभिव्यक्त किया है । कवि की पंक्तियाँ प्रत्येक संवेदनशील प्राणी की आन्तरिक कहानी है, जिसे वह भोग रहा है । सन् अस्सी के दशक के बाद ‘रिश्तों को खोने’ की पीड़ा को कवि ने बहुत ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है । आशा है यह कृति विचारशील चिंतकों को रास्ता तलाशने में मदद करेगी ।