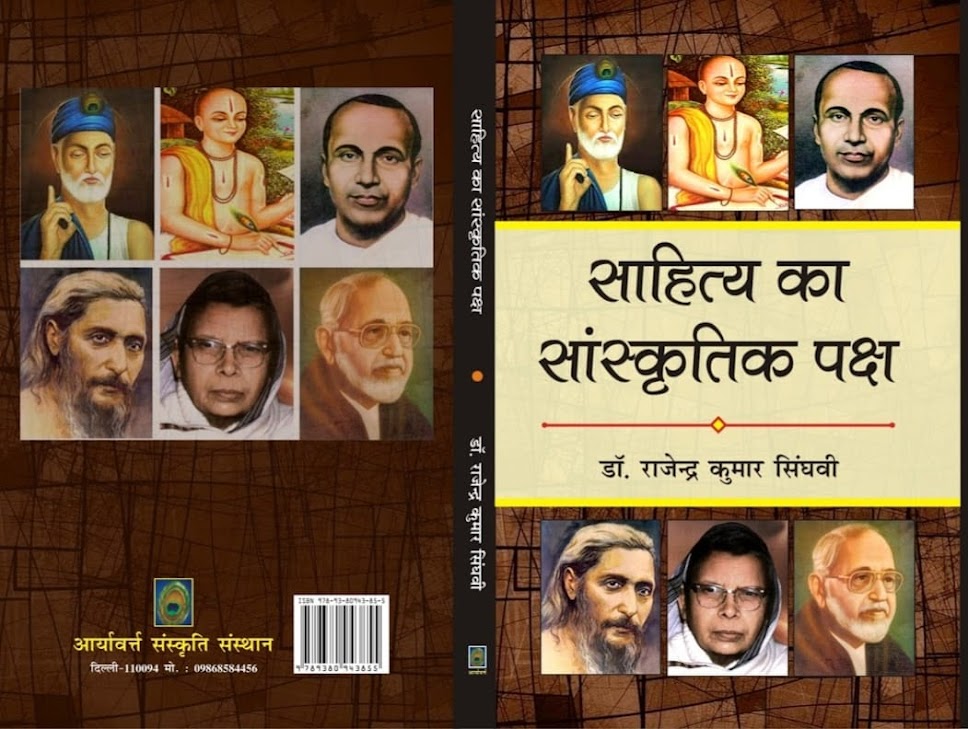नासिरा शर्मा के उपन्यासों में संवेदना का धरातल
'विविधा' जनवरी-मार्च,2025 में प्रकाशित
साहित्य संसार के प्रति मानसिक प्रक्रिया अर्थात् विचारों व भावों की अभिव्यक्ति है। यह ‘हित का साधन’ भी करता है, अतः संरक्षणीय भी है। इसे समाज का उत्पादन भी कहा जाता है, जिससे विशाल मानव जाति की आत्मा का स्पन्दन ध्वनित होता है। साहित्य जीवन की व्याख्या भी करता है, इसी कारण उसमें जीवन देने की शक्ति भी आती है। इस प्रकार साहित्य व समाज का अन्योन्याश्रयत्व चिरकाल से रहा है। स्वप्निल श्रीवास्तव के अनुसार- “आज का यथार्थ मारक और अविश्वसनीय है। वह फैंटेसी के आगे का यथार्थ है। आज के यथार्थ का चेहरा रक्तरंजित और अमानवीय है। यथार्थ हमारे सामने विस्मयकारी दृश्य प्रस्तुत करता है, जो कल्पनातीत है।”[1] विस्मयकारी यथार्थ का जो दृश्य नई सदी के दो दशकों में दिखाई देता है, वह उपनिवेशवादी प्रभाव का परिणाम है। फलतः जो कारक हमारे समक्ष उपस्थित हैं, उनमें प्रमुख हैं- वैश्वीकरण, मुक्तबाजारवाद, विकृत उभोक्तावाद, राजनीतिक अधिनायकवाद, मूल्यहीनता, सांस्कृतिक संघर्ष, भ्रष्ट आचार, हिंसक वर्चस्व आदि। यद्यपि ये कारक वैश्विक हैं, किन्तु भारतीय मन इससे ज्यादा प्रभावित है।
नासिरा शर्मा हिंदी कथा साहित्य की एक सशक्त हस्ताक्षर है। उनकी कृतियों में समाज और संस्कृति का कैनवास विराट रूप में मिलता है। उनके उपन्यासों में रिश्तों की दास्तान, लुप्त होती संवेदनाओं की पड़ताल, वैश्विक परिदृश्य में इंसानियत तथा समकालीन परिवेश में संघर्षशील समाज का बहुआयामी पक्ष बखूबी उभरता है। उन्होंने बाजार और तकनीक के मकड़जाल में फँसी युवा पीढ़ी को भी सावचेत करने का प्रयास किया है। उनके प्रत्येक उपन्यास में समाज के विविध पक्षों को लेकर चिंताएँ व्यक्त की गई हैं। ‘सात नदियाँ: एक समंदर’ ईरानी क्रांति पर लिखा गया दुनिया का पहला उपन्यास है। ‘शाल्मली’ स्वतंत्रता के बाद महिला विमर्श की चेतना को इंगित करने वाला उपन्यास है तो ‘ठीकरे की मंगनी’ एक संघर्षशील युवती की दास्तान है। ‘जिंदा मुहावरे’ में भारत विभाजन का दर्द छलकता है। ‘अक्षयवट’ में युवा पीढ़ी का संघर्ष दिखाई देता है, वहीं ‘कुइयां जान’ में शुष्क होती संवेदनाओं का प्रकटीकरण है। ‘जीरो रोड’ में देश के सामयिक यथार्थ का अंकन है तो ‘पारिजात’ में संस्कृति और परंपरा में नए सूत्र को खोजने की कोशिश है। ‘अजनबी जजीरा’ में इराक की दारुण स्थितियों का अंकन है। ‘कागज के नाव में बेरोजगारी और पलायन की विसंगतियों को उजागर करने की कोशिश है। ‘शब्द पखेरू’ में बाजार का परिदृश्य तो ‘दूसरी जन्नत’ में आधुनिकता की तेज रफ्तार पर फिसलती जिंदगी का सजीव चित्रण है। इस प्रकार मानव जीवन के समग्र पक्षों को नासिरा शर्मा ने अपने उपन्यासों की विषय-सामग्री के रूप में प्रस्तुत किया है।
भारत ने अथक संघर्ष के उपरांत 15 अगस्त, 1947 को आजादी तो प्राप्त कर ली, किन्तु विभाजन की त्रासदी के दंश के आघात को भी झेला। जहाँ धर्म और संप्रदाय के आधार पर मानवता का विभाजन हुआ और मनुष्यता के पतन का रक्तस्नात् चेहरा भी प्रकट हुआ। हजारों लोग बेघर, दंगे, अकाल मृत्यु, विध्वंस, द्वेष के दृश्य के साथ संवेदना का अवसान भी देखने को मिला। नासिरा शर्मा ने उन विभीषिकाओं का केवल ब्यौरा प्रस्तुत न कर उस मानसिकता को नंगा किया है, जो संकटकालीन स्थितियों में भी सब कुछ छीनने और मौके का फायदा उठाने की मनोवृत्ति से ग्रस्त है। नासिरा शर्मा का 'जिंदा मुहावरे' उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी के आधार पर लिखा गया है। धर्म के नाम पर हुए कत्लेआम और इंसानियत के मर जाने का वीभत्स चित्रण करता हुआ यह उपन्यास हिंदी साहित्य जगत में अपनी विशिष्ट पहचान रखता है। फैजाबाद गाँव में रहने वाला रहीमुद्दीन का छोटा बेटा निजाम उपन्यास का केंद्रीय पात्र है, वह पाकिस्तान का ख्वाब देखते हुए करांची चला जाता है और सोचता है "जहाँ जात है अब वही हमारे वतन कहल इहे। नया ही सही अपना तो होइहे। जहां रोज-रोज ओकी खुद्दारी को कोई ललकारिए तो नाहीं।"[2] परंतु पाकिस्तान जाकर वह अपनी जन्मभूमि की गंध के लिए तड़पता है, क्योंकि उसके माँ-बाप, भाई-बहन तो अपनी पैतृक जमीन भारत में ही हैं। वह भारत लौटने के लिए लालायित रहता है, परंतु सियासत उसे ऐसा नहीं करने देती। उसकी तड़प मर्म को हिला देती है। इससे यह प्रकट होता है कि विभाजन का दर्द हमारे समय का घातक सच है।
वैश्विक धरातल पर यदि हम अवलोकन करें तो किसी भी समाज में महिलाओं को समान स्तर प्राप्त नहीं हुआ। पुरुष की परंपरागत मानसिकता में नारी की संघर्ष गाथा है। यह विश्व के प्रत्येक देश में देखी जा सकती है। ईरान की क्रांति पर आधारित उपन्यास ‘सात नदियां: एक समंदर’ में अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठती स्त्रियों की संघर्ष गाथा है। इस उपन्यास की सारी प्रमुख पात्र स्त्रियां हैं, जहां खुमेनी शासन के आने पर उनकी उम्मीदें टूट जाती है। शासन के विरोध में बोलने का नतीजा यह होता है कि पहले तो वह अपने वैवाहिक जीवन से दूर हो जाती है और तैयब अपनी कलम को खुमेनी शासन के विरुद्ध चलाती है तो अंततः शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना देते हुए उसे गोली से उड़ा दिया जाता है। यहां नासिरा शर्मा लिखती है, “ईरान की क्रांति पर लिखा मेरा यह उपन्यास उन अनुभवों का लेखा-जोखा है जो पिछले नौ वर्ष में मुझे ईरान की धरती पर हुए इन नौ वर्षों के पीछे लगभग नब्बे वर्षों का अतीत सांस ले रहा था जिसमें 5000 वर्ष पुराने ईरान की सभ्यता संस्कृति का वैभव अपनी ऐतिहासिक गाथा गुनगुना रहा था।“[3] वास्तव में युद्ध हो या क्रांति, स्त्रियों का संघर्ष अपने लिए कुछ पा न सका।
आर्थिक नाकाबंदी में इराक की जनता जिस गरीबी और महंगाई से जूझ रही थी, उसी में अमेरिकन बमबारी, सद्दाम का तख्ता पलट और आम आदमी किस तरह सियासी खबरों के पीछे छुप जाता है उसका सुख-दुख ‘अजनबी जजीरा’ में प्रकट हुआ है। युद्ध ग्रस्त विभीषिका में औरतों की स्थिति का सत्य और भी भीषण है। लेखिका ने इस सत्य को इस उपन्यास की पात्र समीरा के मुँह से कहलवाया है, "युद्धग्रस्त समाज की कठिनाइयाँ कितनी नई परेशानियों से हमारा परिचय कराती है, तब पेट के आगे बदन बेचना यहां तक की अपने बच्चे तक को बेचना मुश्किल काम नहीं लगता, बल्कि मौत को नजदीक पाकर जीने की तमन्ना ज्यादा बढ़ जाती है। मुझे ही देखो जवान बेटियों की भूख के आगे मैं अपनी भूख को दबा नहीं पाती..।"[4] समीरा का यह कथन मानवीय त्रासदी की पराकाष्ठा है। जब वह कहती है, “जिस्मफरोशी से मुझे हालात ने महफूज रखा वरना वह भी मुझे करना पड़ता.. हालात अच्छाई और बुराई के मायने कैसे बदल कर रख देते हैं.. पेट भरे लोगों के लिए उंगली उठाना कितना आसान होता है मगर भूखे के लिए रोटी हर फलसफे से बढ़कर अहम हो उठती है।“[5] सभ्य कहलाने वाले इस आधुनिक विश्व में विध्वंस का यह मूर्त रूप पाठकों को स्तब्ध कर देता है। ऐसे परिदृश्य में मान्यता तारतार होती है और स्त्री विमर्श के समूचे निहित अर्थ बदल जाते हैं।
पेट की आग व्यक्ति को कुछ भी करने कोई वश कर देती है उसे समय उसके सामने नैतिकता का मायने बदल जाते हैं। विदेशी सेना के आक्रमण और बम हमले से इराक पूरी तरह नष्ट हो गया है। फौजी शासन के तले लोगों को जरूरत की चीजों के लिए घरेलू सामान बेचना पड़ रहा है। अधिकांश इराक के समर्थक मारे जा चुके हैं। ऐसे भीषण समय में एक बूढी औरत जो अपने दो छोटे नवासों की एकमात्र संरक्षक है। बच्चों की भूख को शांत करने के लिए बाजार में दो रोटी छुपाने के आरोप पकड़ी जाती है। वह अपना दुखड़ा समीरा के समक्ष कहती है, "मेरे दो नवासे हैं, कल से भूखे हैं। चारा क्या था मेरे पास?"[6] यह सच मानवता के नाम पर कलंक है।
धर्म के नाम पर हमारा सामाजिक ताना-बाना आज के समय में छिन्न-भिन्न दिखाई देता है। 'जीरो रोड' उपन्यास में धार्मिक कट्टरता के नाम पर इंसानियत को तबाह करने का दृश्य दिखाई देता है। कई ऐसे दृष्टांत है जिसके माध्यम से पाठक सोचने पर मजबूर हो जाता है। उपन्यास का पात्र मुन्ना हाफिज का घर राम प्रसाद व जगत रामजी के मोहल्ले में है। वह चौक में मजहबी किताबों की दुकान लगाकर परिवार का पालन पोषण करता है। अपनी ईमानदारी व उदार दृष्टिकोण के कारण अपने ही मजहब के कट्टर व संकुचित मानसिकता वाले लोगों को चुभने लगता है। उनके उकसाने पर वह तबलीगी जमात वालों को जवाब देते हुए कहता है, "कान खोल कर सुन लें आप सभी साहेबान! मैं किसी के ना खिलाफ कोई काम करता हूँ ना किसी मजहब की तब्लीग पर। मैं गैर मुसलमान को गाली नहीं देता हूँ, बल्कि उन बातों की शिकायत करता हूँ, जो हमें खलती है, जिससे हमें नुकसान पहुँचता है।"[7] उसके इस उदार मनोवृति का परिणाम यह होता है कि एक दिन अचानक रात के दो-तीन बजे उसकी दुकान में आग लगा दी जाती है। लगभग दो लाख की किताबें जलकर खाक हो जाती हैं। इस घटना को लेकर उनके ही जमात के लोग तरह-तरह के आशंकाएं व्यक्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि इसे सांप्रदायिक रूप दिया जाए।
जब भी दुनिया में सांस्कृतिक एकता के इतिहास की बात होती है तो भारत का जिक्र होना लाजमी ही है। यहाँ के संस्कारों में दो संस्कृतियाँ यूँ घुली-मिली हैं मानो दोनों एक दूसरे की पूरक हों। ‘पारिजात’ उपन्यास नासिरा शर्मा की एक ऐसी ही कृति है, जो भारत की समावेशी संस्कृति को परत-दर-परत खोलती और मानवीय रिश्तों की बुनावट को भाषा के एहसासों से पाठक के अंदर जीवंत करती है। ‘पारिजात’ आज की पीढ़ी के सपनों, उसके निर्णय, माता-पिता के प्रेम, स्त्री की भारतीय और पाश्चात्य छवि के साथ गुरु-शिष्य के संबंधों और एक समुदाय विशेष के प्रति पाश्चात्य पूर्वाग्रह से घायल समाज जैसी संवेदनाओं को एक नए फलक में तर्कों के साथ बयां करता है, वहीं ‘अक्षयवट’ उपन्यास में लेखिका ने इलाहाबाद से जुड़ी अपनी स्मृतियों के बहाने मानवीय संवेदना में आए बदलाव को रेखांकित किया है। इस उपन्यास के केंद्र में इलाहाबाद शहर के पत्थर गली, नखास कोना, रानी मुंडी, दरियाबंद, हिम्मत गंडा, बताशा वाली गली आदि भागों में रहने वाले लोगों की जिंदगी को दर्शाया है।
यहाँ हम देखते हैं कि उपभोक्ता संस्कृति ने उत्सवों में छिपे सार तत्त्वों को सोख लिया है। स्वयं लेखिका कहती है, "परंपरा के निर्वाह के लिए रावण के पुतले में आग लगाना और बुराई को सदा के लिए मिटा देने का संकल्प हर दिल में होता, मगर व्यावहारिक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनने की जिज्ञासा किसी में ना जगती। क्योंकि त्याग करने पर आज के दौर में कोई राजी ना था, उल्टे त्याग की जगह पैसा कमाने की नई-नई तरकीबों में सबका मन मस्तिष्क रमता। रावण को ना करते हुए भी रावण- कृत्य को अपनाने की छुपी लालसा आज का सबसे कड़वा यथार्थ था।"[8] वस्तुतः इलाहाबाद की धमनियों में अक्षयवट के समान अविराम भाव धारा विरासत के रूप में सदैव विद्यमान रही, लेकिन समय के साथ उसमें भी व्यवस्था की सड़ांध और अवसाद भरी जिंदगी के चिह्न नजर आने लगे हैं।
आर्थिक उदारीकरण के दौर में शहरीकरण की प्रक्रिया तीव्र हुई है और इस प्रक्रिया में सर्वाधिक नुकसान ‘संवेदना’ का हुआ है। जहाँ व्यक्ति अपने घर को बचाने के लिए संघर्ष करता दिखाई देता है। हमने भावनाओं को केन्द्रित करना सीखा है और रिश्तों को भी ताक पर रख दिया है। हम सवालों से डरने लग गए हैं और अपेक्षा करते हैं कि जैसा चल रहा है उसे घर का हर सदस्य स्वीकार कर ले। 'शब्द पखेरू' उपन्यास हमें आगाह करता है कि कैसे नई पीढ़ी अनजाने में ही साइबर क्राइम का हिस्सा बन जाती है। आम जीवन में बढ़ते इंटरनेट के इस्तेमाल और सामाजिक संबंधों में आए बदलावों को हमारे समक्ष बखूबी उपस्थित करता है, दूसरी और मध्यमवर्गीय परिवार की घुटन, संवादहीनता और सीमित संसाधनों के साथ बड़े सपनों को पूरा करने की जद्दोजहद में लगे बच्चों की कथा यह उपन्यास बारीकी से कहता है। आज के मध्यमवर्गीय परिवारों में यह दृश्य सामान्यतया दिखाई दे सकता है।
आज की पीढ़ी बुजुर्गों के बजाय गूगल से मिलने वाले ज्ञान पर ज्यादा सहज है। "मनीषा शैलजा में बढ़ता विश्वास देख रही थी जो कभी-कभी उसे बाद आक्रामक लगता। हरदम लैपटॉप की स्क्रीन पर आंखें गाड़ी रहती। एक दिन उसने ईर्ष्या वश उसका नाम 'इंटरनेट बेबी' रख दिया था, मगर उसे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। फेसबुक पर हर फ्रेंड रिक्वेस्ट को कंफर्म कर देना जैसे उसके लिए जरूरी था। किताब या नोटबुक खुली है, सामने मैटर ढूँढने के बहाने चैट चल रही है। दिखावा ऐसी करती है जैसे बेचारी पढ़ाई को लेकर हलकान हो रही है। इंटरनेट के विस्तृत आकाश पर देखने पढ़ने और खोजने के लिए बहुत कुछ था। उसने गूगल को 'ग्रैंडपा' का नाम दे रखा था।"[9]
समग्रतः यह कहा जा सकता है कि जब कभी मानव सभ्यता चाँद को छूने के लिए ब्रम्हांड को चीरती है तब ये चित्र मानव को आदिम युग में ले जाते है, जो शर्मनाक है। मनुष्यता के कलंक से विमुक्ति का प्रयास मानव जीवन के प्रति एकात्म भाव से ही संभव है, अन्यथा विकास की गति केवल छलावा है। विश्व साहित्य की प्रथम पुस्तक, जिसे यूनेस्को ने भी स्वीकार किया है, वह है- ऋग्वेद। उसमें कहा गया है- मनुर्भवः, अर्थात् मनुष्य बनो। मनुष्यता का बोध ही भारतीय संस्कृति का मूल है, जो वर्तमान और भविष्य के लिए भी जरूरी है व रहेगी। हिन्दी उपन्यास परम्परा में नासिरा शर्मा का अवदान मानवीय संवेदनाओं के धरातल पर इस दृष्टि से स्तुत्य है।
संदर्भ-
1. आलोचना, अप्रैल-जून,2003, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, पृ.32
2. जिंदा मुहावरे, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2017, पृष्ठ 11
3. सात नदियां: एक समंदर, अभिव्यंजना प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 1984, पृष्ठ 7
4. अजनबी जजीरा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृष्ठ 78
5. अजनबी जजीरा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृष्ठ 120
6. अजनबी जजीरा, लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद, सं. 2017, पृष्ठ 24
7. जीरो रोड, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 2003 पृष्ठ 286
8. अक्षयवट, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, सं. 2003 पृष्ठ 42
9. शब्द पखेरू' वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 2017, पृष्ठ 40