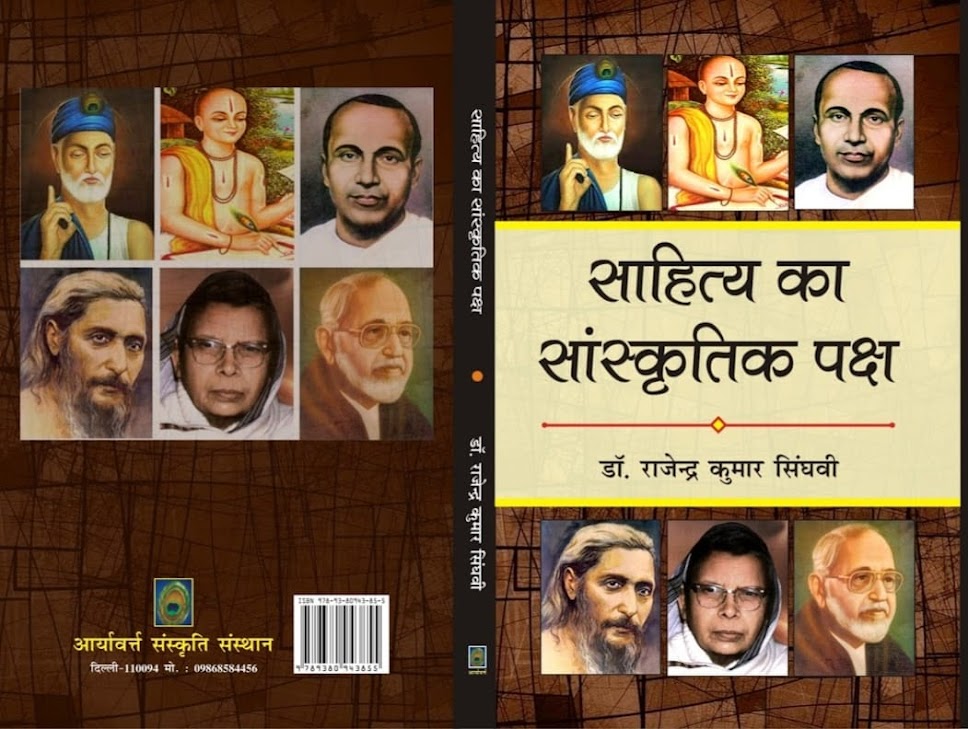राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक समरसता में साहित्य की भूमिका
मिथकीय चेतना एवं लोकमन (सन्दर्भ: नदी केंद्रित यात्रावृत्त)
मिथकीय चेतना एवं लोकमन
(सन्दर्भ: नदी केंद्रित यात्रावृत्त)
समवेत, अगस्त, २०२५ में प्रकाशित
नदियों के किनारे विकसित संस्कृतियाँ हमेशा नदियों के आँचल को ही ओढ़कर अपने अस्तित्व को प्रकट करती रही हैं। इन सरिताओं ने सदियों से अपने नाम, गुण और धर्म के कारण जनसमुदाय को आकृष्ट किया है। नदियों के पौराणिक और मिथकीय सन्दर्भ लोकमन में अपना स्थान घेरते रहे हैं। नदियों के प्रति ऐसे ही श्रद्धाभाव और सहज सौंदर्य के वशीभूत होकर भारतवर्ष के आमजन सहित अनेक लेखकों व कवियों ने भी यात्राएँ की हैं। इन्हीं यात्राओं का ब्यौरा यात्रा साहित्य में प्रकाशित हुआ है। यात्रा-पथ में आने वाली नदियों का शाश्वत सौन्दर्य और उनका पुरात्मक महत्त्व यात्रावृत्तों का वर्ण्य विषय रहा है। अनेक लेखकों ने अपनी उत्तर एवं दक्षिण भारत की यात्राओं के दौरान पथ की नदियों का विस्तारपूर्वक वर्णन पेश किया है। उन नदियों से जुड़े मिथकीय, पौराणिक, लोक कथात्मक और ऐतिहासिक प्रसंग भारतीय संस्कृति के जल तत्त्व और उसके प्रति सम्मान का बोध करवाते हैं।
मिथक शब्द अंग्रेजी के मिथ (Myth) शब्द से लिया गया है। ‘माइथोस’ शब्द से इसकी उत्पत्ति मानी गयी है। इस शब्द का आशय ‘मुहँ से निकला हुआ’ होता है। अतः ये मौखिक कथा से सम्बंधित हैं। “भारतीय सन्दर्भ में मिथ का अर्थ ‘पुराण’ होना चाहिए। पुराण अर्थात् पुरा कथा। यह समझदारी नहीं होने के कारण हमने 'मिथक' चूँकि उक्त अर्थ में झूठी कथा है, को हमने इतिहास का पाठ नहीं माना जब कि भारतीय सन्दर्भ में मिथक झूठी कथा न होकर 'पुरा कथा' है।' जिसमें इतिहास के खोज की अनन्त संभावनाएँ हैं। वस्तुतः जहाँ इतिहास नहीं है अथवा जहाँ इतिहास खो गया है, वहाँ पुराण हमारे लिए एक पाठ का काम कर सकता है।”[1] आदिम मानव प्रकृति की शक्तियों को समझ नहीं पाया अतः उसने प्रकृति की शक्तियों को अपनी कल्पना से अतिमानवीय देवी-देवताओं के रूप दे दिए। “इस प्रकार धार्मिक विश्वास तथा मिथक में अटूट सम्बन्ध है। धार्मिक विधि-विधान से जुड़े आख्यानों ने भी मिथक का रूप ले लिया। इनके पीछे उन रहस्यमयी शक्तियों को तुष्ट करके विपत्तियों से जन-समाज की रक्षा करने की भावना प्रमुख थी।”[2] मिथक मनुष्य जाति में एकता और समाज में संसार के प्रति आस्था जगाते हैं।
मिथक प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त होते हैं। ये सृष्टि की उत्त्पत्ति, इसके सृजन की प्रक्रिया तथा मनुष्य के जीवन अनुभवों को विभिन्न प्रतीकों और कथाओं का सहारा लेकर व्यक्त करते हैं। मिथक का यथार्थ मनुष्य के वर्तमान भौतिक जगत् से साम्य नहीं रखता है, परन्तु यह मानव के अंतर्मन और पारलौकिक सत्य को व्यक्त करता है। मिथक को मनुष्य समाज के सामूहिक मन की सच्चाई कही जाती है। मनोविज्ञान ने भी निजी मन की गुत्थियों को सुलझाने के लिए इस सामूहिक सच का सहारा लिया है। भारत में मिथक साहित्य केवल एक विधा नहीं है बल्कि यह जीवन को संचालित करने वाली संस्कृति है। उषा पुरी विद्यावाचस्पति लिखती हैं, “प्रत्येक देश का मिथक साहित्य उस देश की संस्कृति, कला, विज्ञान, आचार-विचार आदि का आरक्षण करता है। अनैतिक कार्य करते हुए मानव पर अंकुश स्थापित करने वाला मिथक साहित्य नैतिकता को प्रोत्साहित करता है।”[3] भारतीय समाज पुरातन और आधुनिक दोनों ही रूपों में एक साथ गतिमान है। यहाँ के जीवन में मिथकीय विश्वासों के साथ विज्ञानयुक्त चिंतन भी देखा जा सकता है। समय और जीवन पद्धति में बदलावों के साथ इन मिथकों में बहुत कुछ परिवर्तन देखे गए हैं, परन्तु इन्हें नकारा नहीं गया। भारतीय मिथकों में वेद, पुराण, उपनिषदों, रामायण, महाभारत आदि की कथाओं और पात्रों को सम्मिलित किया जाता हैं।
हिन्दी यात्रा साहित्य में नदियों को केंद्र में रखकर लेखन मिथकीय चेतना और लोकमन के अवगाहन बिना पूर्ण नहीं होता। इन कृतियों में अमृत लाल वेगड़ के नर्मदा नदी केन्द्रित तीन यात्रावृत्तांत ‘सौन्दर्य की नदी नर्मदा’, ‘अमृतस्य नर्मदा’ और ‘तीरे तीरे नर्मदा’ हैं। इसी तरह विष्णु प्रभाकर का ‘जमना-गंगा के नैहर में’, अभय मिश्र एवं पंकज रामेंदु द्वारा लिखित ‘दर दर गंगे’, सांवरमल सांगानेरिया का ‘ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे’, राकेश तिवारी का ‘सफर एक डोंगी में डगमग’, श्रीराम परिहार का ‘संस्कृति सलिला नर्मदा’, राजेश कुमार व्यास का ‘नर्मदे हर’, अमरेन्द्र कुमार राय का ‘गंगा तीरे’ और अर्जुनदास केसरी का ‘एक आँख गंगा एक आँख सोन’ आदि अनेक यात्रावृत्त हैं, जिनमें भारतीय पौराणिक मिथकों और लोक मानस की अभिव्यक्ति सांस्कृतिक धरातल पर हुई है।
वाराणसी मोक्षदायिनी पुरी है। गंगा किनारे का यह प्रसिद्ध नगर सदियों से संस्कृति का केंद्र है। गंगा तट के घाटों में राजा हरिश्चंद्र के नाम से भी घाट है जहाँ श्मशान स्थित है। यहीं पर उन्होंने सत्य की टेक रखते हुए अपने पुत्र रोहित के शव का अंतिम संस्कार करने का भी शुल्क अपनी पत्नी से वसूल किया था। सफर एक डोंगी में डगमग यात्रावृत्तांत के लेखक राकेश तिवारी ने राजा हरिश्चंद्र के मिथक को अपने वृत्तान्त में जगह दी है। वे लिखते हैं, “आगे आया हरिश्चन्द्र की सत्यनिष्ठा बखानता चिर प्रज्वलित महाश्मशान।....भयानक श्मशान के साथ राजा की अद्वितीय सत्यनिष्ठा की कथा का योग इस स्थल के साथ रोमांच समावेशित कर इसमें चुम्बकीय आकर्षण भर देती है।”[4]
गंगा नदी के जाह्नवी नाम के पीछे का मिथक बड़ा प्रसिद्ध हुआ है। गंगा नदी का जाह्नवी नाम जन्हु ऋषि के कारण पड़ता है। इसके पीछे की कथा का विवरण हमें यात्रावृत्तांत जमना-गंगा के नैहर में मिल पाता है। गंगा भगीरथ के पीछे-पीछे आती हुई अपने प्रबल वेग से जह्नु ऋषि के आश्रम को बहा ले जाती है। क्रुद्ध जह्नु आचमन करके गंगा को पी जाते हैं। भगीरथ ने उनसे प्रार्थना की। इसको आगे बढ़ाते हुए वे लिखते हैं, “महर्षि प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी जांघ चीरकर भागीरथी को फिर धराधाम पर जाने दिया। इसीलिए भागीरथी का एक और नाम हुआ जाह्नवी।”[5] अभय मिश्र और पंकज रामेन्दु भी अपनी गंगा यात्रा में इस मिथक का जिक्र करते हैं। बिहार के भागलपुर से कुछ दूर कहलगाँव है। “कहते हैं इसी जगह पर जह्नु ऋषि ने गंगा को अपनी जांघ पर रोक दिया था। बाद में भागीरथ की प्रार्थना पर उन्होंने गंगा को छोड़ दिया।”[6] कहलगाँव में गंगा का नाम जाह्नवी है। सफ़र एक डोंगी में डगमग यात्रावृत्तांत में भी इसकी चर्चा लेखक ने की है। “यहाँ गंगा 'जाह्नवी' कहलाती है।”[7] फरक्का में गंगा नदी पर बने हुए बैराज को देखते हुए लेखक को पौराणिक कथा स्मरण हो आई। फरक्का के बाद दो धाराओं में बहती गंगा पद्मा और भागीरथी के नाम से जानी जाती है। “कहते हैं गोमुख से राजा भगीरथ के साथ चली गंगा को यहीं आकर... गंगा को चेताया तो मुख्य प्रवाह से एक धारा निकलकर गंगासागर की ओर चल दी जिसे 'भागीरथी' कहा गया। मुख्य धारा आज के बांग्लादेश में बहती है और पद्मा कहलाती है।”[8]
मिथकों में नदियों के किनारे के प्रमुख तीर्थों, नगरों और स्थानों आदि के नामकरण के संदर्भ भी जुड़े हुए मिलते हैं। नदी केंद्रित यात्रावृत्तांतों में ऐसे प्रसंग भी देखने में आए हैं। जैसे नारद को आशीर्वाद देने के लिए शिव के द्वारा रौद्र रूप धारण करने से रुद्रप्रयाग नाम पड़ा। कर्णप्रयाग में दानवीर कर्ण ने सूर्य भगवान की तपस्या की थी। नंद प्रयाग में कण्वाश्रम के महादेव मंदिर में रावण ने अपने दस सिर काट कर चढ़ाये थे अतः दशमौली से ही इस क्षेत्र का नाम दशौली पड़ना बताया जाता है। हरिद्वार में हरि की पौड़ी पर ही अमृत की बूँदें गिरने के कारण ही इसे ब्रह्म कुंड माना जाता है। गंगनानी के साथ वेदव्यास की माता मत्स्यगंधा और पराशर ऋषि की एक प्राचीन कथा जुड़ी हुई है। ब्रह्मपुत्र के किनारे स्थित गुवाहाटी नगर के नीलकूट पर्वत पर कामाख्या देवी की कहानी के पौराणिक संदर्भ हमें ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे के लेखक बयाँ करते हैं।
नदियों के किनारे के नगरों, प्रमुख स्थानों आदि के साथ कुछ किवदन्तियाँ और अंतर्कथाएँ भी प्रचलित होती हैं। उस क्षेत्र के अस्तित्व की पुरातनता को सिद्ध करने अथवा लोक में उसकी महत्ता बताने के लिये भी परम्परा से इनका प्रसार होते हुए देखा जा सकता है। नर्मदा नदी को चिरकुमारी माना गया है। चिरकुमारी होने के कारण नर्मदा अत्यन्त पवित्र नदी मानी गई। इसीलिए भक्तगण और साधारणजन उसकी परिक्रमा करते हैं। यह प्राचीनतम नदियों में से एक है। ऋग्वेद में भी इस नदी के प्रमाण मिलते है। जनमानस में नर्मदा के प्रति काफी सम्मान व्याप्त है। दर्शन मात्र से पाप का शमन करने वाली नर्मदा नदी के साथ शोणभद्र नद की प्रणयकथा लोक में बहुश्रुत है। वेगड़ जी ने इसके बारे में लिखा है, “नर्मदा और शोणभद्र नद एक दूसरे को चाहते थे, दोनों का विवाह होने वाला था। एक बार नर्मदा ने अपनी दासी जुहिला के हाथ शोण के लिए सन्देश भेजा। काफी देर बाद भी जब जुहिला नहीं आई, तो नर्मदा स्वयं गई। उसने देखा कि शोण जुहिला से ही प्रेमक्रीड़ा कर रहा है। उसे शोण पर अत्यन्त क्रोध आया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा करके पश्चिम की ओर चल दी। निराश और हताश शोण पूर्व की ओर चल पड़ा।”[9] यह कथा प्रकृति के उपादान के माध्यम से लोक में प्रेम की एकनिष्ठता को स्थापित करती दिखाई पड़ती है। श्रीराम परिहार भी अपने यात्रावृत्तांत में इसका जिक्र करते हैं, “एक लोक कथा है- शोण और नर्मदा की प्रणय कथा।”[10] राकेश तिवारी अपने यात्रावृत्त में जब गंगा की सहायक नदियों का जिक्र करते हैं तो उनमे सोन का नाम भी लेते हैं। साथ ही इसी दंतकथा को दुहराते हैं, “किसी बात पर दोनों में ठन गई। सोन तुनक के उत्तर चले और नर्बदा पश्चिम।”[11]
लोक-परम्परा के अनुसार नर्मदा नदी के पैंदे से निकले शिवलिंग पूरे देश में पूजे जाते हैं। इस नदी के पत्थर सुडौल और तराशे हुए मालूम जान पड़ते हैं। इसके संदर्भ में एक पौराणिक उद्धरण राजेश कुमार व्यास देते हैं। उनके अनुसार, “स्कंद पुराण में आता है, तपस्यारत शिव के शरीर से निकलने वाले स्वेद से नर्मदा की उत्पत्ति हुई।... स्वेद से उत्पन्न पुत्री ने पिता से वर माँगा, महेश्वर-पार्वती सहित उनके तट पर विराजे। शिव ने इसे स्वीकारा। इसीलिए नर्मदा के जल में स्थित सभी पाषाण शिवतुल्य कहे गए हैं। कहते भी हैं, 'नर्मदा के कंकर, सब शिवशंकर'।”[12] मिथक अपने भीतर सूत्र छिपाए रखते हैं। वर्तमान भौतिक जगत् में इन संदर्भों को समझना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता हैं, परन्तु उनके भीतर के प्रतीकों के माध्यम से उनके अभिप्रायों के निकट पहुँचा जा सकता हैं। मिथक हमें नदियों के जन्म के संदर्भ भी देते हैं। उनके नामकरण के बारे में भी बताते हैं। सांवरमल सांगानेरिया के वृत्तान्त ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे में इसकी बानगी देखिए, “शान्तनु मुनि को ब्रह्मा से वरदान स्वरूप उनका अग्निमय ओज प्राप्त हुआ।...उस दिव्य ओज को अपनी भार्या अमोघा के गर्भ में स्थापित कर दिया, जिससे एक जलस्वरूप पुत्र ने जन्म लिया। कालान्तर में वही जलधारा के रूप में प्रवाहित होने पर ब्रह्मपुत्र कहलाने लगा।”[13]
इन यात्रावृत्तांतों में बड़ी और महत्त्वपूर्ण नदियों से जुड़े संदर्भ और दंतकथाओं के साथ ही सहायक और छोटी नदियों से जुड़ी किवदंतियाँ भी हमें पढ़ने को मिलती हैं। जरूरी नहीं कि ये कथाएँ प्राचीन हों ही। यथा केन नदी से सम्बंधित एक अंतर्कथा आती है जो गाँव की लड़की किनिया की प्रेम कहानी से जुड़ी है। राजेश कुमार व्यास लिखते हैं, “प्रेमी का शव देखते ही किनिया ने भी अपने प्राण त्याग दिए। वर्षा के पानी से नदी निकली और नदी का नाम किनिया हो गया।"[14] इसी तरह सरयू नदी से सम्बंधित अंतर्कथा भी पढ़ने में आती है। चंबल नदी के नामकरण पर बात करते हुए लेखक राकेश तिवारी ने उसकी उत्पत्ति के स्रोत का परिचय प्रस्तुत किया है। राजा रन्तिदेव की कथा का जिक्र करते हुए वे लिखते हैं, “अग्निहोत्र नामक यज्ञ के अवसर पर उनकी पाक-शाला से मेध्य पशुओं के चमणे की राशि से चर्मण्वती नदी प्रभूत हुई। यही चर्मण्वती आज की चम्बिल, चामिल, चम्बल, चामर या चामल है।”[15] उनके वृत्तान्त में चंबल किनारे के गाँव पिनहट के नामकरण के पीछे पांडु-हाट शब्द में छिपी जनश्रुति का जिक्र होता है।
कई बार स्थानीय निवासियों द्वारा भी परम्परा से चली आती कथा को नदियों के नामकरण के संदर्भ में भी स्वीकार कर लिया जाता है। लोक में पारिवारिक रिश्तों के आधार पर भी नदियों की पहचान स्थापित होती है। मानवीकरण द्वारा लोक नदियों के बारे में किसी रिश्ते से सम्बंधित कथाएँ गढ़ लेता है। इसी संदर्भ में यमुना की सहायक नदी 'ससुर-खदेरी' के नामकरण की जनश्रुति बड़ी ही रोचक लगती है। “धान की रोपाई के मौके पर ससुर और बहू में शर्त लग गई, देखें कौन कितना धान रोपता है। ... शाम को जब सब लौटते तो बाजी बहू के हिस्से पड़ती। ...ससुर विस्मय में पड़ गया—'यह तो मानुस की काया में देवी लगती है। ... पैर छूने के चक्कर में ससुर पीछे दौड़ा। बहू भागती रही, ससुर खदेड़े रहा। बहू ने लज्जावश यमुना में छलांग लगा दी। बहू की मृत्यु से दुखी ससुर भी यमुना में डूब गया। बहू के भागने की जगह से यमुना तक एक पुण्य-धारा फूटकर बह चली जिसका नाम पड़ा 'ससुर-खदेरी'।”[16] हालाँकि आज के दौर में इन दंतकथाओं पर विश्वास करना मुश्किल होता है, पर इनके पूर्वकालिक आधारों को एकदम से नकारा भी नहीं जा सकता हैं। सफ़र एक डोंगी में डगमग में गहमर गाँव के मंदिर में लड़कों से बात करने पर लेखक को एक पतली नदी के नाम के पीछे की गाथा ज्ञात हुई। यहाँ त्रिशंकु की अंतर्कथा के द्वारा इसी पतली कर्मनाशा नदी के उद्भव की बात कही गई है।
इन यात्रावृत्तांतों में नदियों से सम्बंधित मिथक, अंतर्कथाएँ और दंतकथाएँ बहुतायत में पढने को आती हैं। दरअसल नदियों के किनारे रहने वाला समाज नदियों से सम्बंधित पौराणिक सन्दर्भों को अपने मानस में उतार लेता है। समय के अनुसार इन सन्दर्भों में वह अपनी सुविधा और समझ के चलते परिवर्तन भी कर लेता है। यही बात दंतकथाओं के संदर्भ में भी सटीक बैठती हैं। कुछ अंतर्कथाएँ नदियों के किनारे स्थित गाँवों, शहरों, प्रसिद्ध स्थानों के नामकरण के बारे में भी मिलती हैं। राकेश तिवारी के यात्रावृत्त में गंगा तट पर स्थित बक्सर शहर के नाम की उत्पत्ति में छिपे मिथक से परिचय प्राप्त होता है। “कहा जाता है यहाँ वेदशिरा ऋषि का आश्रम था। … वेदशिरा शाप पाकर बाघ बन बहुत समय तक इसी रूप में विचरते… रहे। दूसरे मुनियों से उन्हें पता चला कि निकट ही स्थित 'अधसर' में स्नान करके अनचाही मुसीबत से मुक्ति मिल सकती है। उन्होंने ऐसा ही किया और तब से तालाब व्याघ्रसर कहलाया। कालान्तर में वहाँ बसी बस्ती 'ब्याघ्रसर' व्युत्पत्ति के अनुसार 'बक्सर' कहलाई।”[17] नामकरण की ये कथाएँ बुजुर्गों की स्मृतियों और उनकी बातों में उपस्थित रहती हैं। गंगा की यात्रा के दौरान लेखक राकेश तिवारी ने अपनी डोंगी में एक बुजुर्ग को बैठाया था। उसने जनश्रुति द्वारा तट के लाक्षागिरि गाँव के नामकरण की जानकारी दी।
इसी पुस्तक में गंगा तट के गाँव विंध्याचल से संबंधित लोक मान्यता का विवरण प्राप्त होता है। गंगा के प्रवाह के निकट स्थित चरणाद्रि पर्वत, जिस पर ऐतिहासिक चुनार दुर्ग निर्मित है, के संबंध में राजा बलि और भगवान् विष्णु के वामन अवतार की पौराणिक कथा का जिक्र भी सफ़र एक डोंगी में डगमग में किया गया है। “कहते हैं, पुण्यात्मा बलि यहीं कहीं रहते थे और विष्णु का पहला कदम इसी चरणाकृति जैसी पहाड़ी पर पड़ा।”[18] चुनार दुर्ग की तरह वे काशी नगर के नामकरण के संदर्भ भी प्रस्तुत करते हैं, “राजा काश के नाम पर यह क्षेत्र काशी कहलाया। कुछ लोग काश और कुश नामक स्थानीय घास से काशी की व्युत्पत्ति मानते हैं।”[19] असम को कामरूप कहे जाने के पीछे तपस्यारत भगवान् शिव द्वारा कामदेव को भस्म करने के मिथक का उल्लेख ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे में मिलता है। “उसकी पत्नी रति ने शिवाराधना की, तब उसे आदेश हुआ कि कामदेव की भस्मी लेकर प्राग्ज्योतिषपुर जाए। आखिर शिव-कृपा से उसे यहीं नया रूप मिला था, तब से यह क्षेत्र कामरूप कहलाने लगा।”[20] इस प्रकार हम पाते हैं कि पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से भी किसी क्षेत्र का नाम प्रचलन में आ जाता है। यह नाम चिरकाल तक स्थायी और स्वीकार्य भी रहता है।
भारतीय समाज का नदियों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध लोकगीतों सहित लोक कथाओं के माध्यम से भी परिलक्षित होता है। लोककथाएँ वाचिक परम्परा का साहित्य है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी यात्रा करती हुई अपना अस्तित्व कायम रखती हैं। मौखिक परम्परा ने अपने श्रुत-कौशल और विवेक से इसे आगे बढ़ाया है। कथा कहने और सुनने के क्रम में काल के साथ कुछ परिवर्तन भी होता है। इनमें कुछ घटाव और बढाव संभव है। स्थान के अनुसार भी लोक कथाओं में पात्र और परिस्थितियाँ स्थानीय रूप धारण कर लेते हैं। इन कथाओं में सम्पूर्ण समाज के मंगल का विधान निहित होता है। सामाजिक विश्वास, मान्यताएँ और आस्थाएँ इनमें आसानी से ढूँढी जा सकती हैं।
सुदर्शन वशिष्ठ इन लोक कथाओं के बारे में लिखते हैं, “भारतीय साहित्य का परम ध्येय मंगलकामना रहने के कारण हमारी अधिकांश कथाएँ ‘और अंत में सब सुखपूर्वक रहने लगे’ के आदर्श पर आधारित हैं।”[21] इन कथाओं में कोई संदेश अथवा गूढ़ बात निहित होती है। ये लंबे अनुभव और व्यावहारिक दृष्टिकोण को अपने भीतर समाए रहती हैं। भारतीय समाज में नदियों के साथ भी लोक कथाएँ जुड़ी हुई हैं। ये कहानियाँ नदियों की संस्कृति को समाज के साथ एकाकार करने में बड़ी भूमिका निभाती हैं। कईं बार अतिरंजित वर्णन के कारण ये विश्वास से परे होती दीखती है, लेकिन लोक अपनी छवि का दिग्दर्शन इनमें कर पाता है। इन यात्रावृत्तांतों में हमें नदियों के उद्गम, प्रवाह क्षेत्र, प्रभाव और उनके महत्त्व से जुड़ी लोक कथाओं से परिचय प्राप्त होता हैं। सफ़र एक डोंगी में डगमग यात्रावृत्तांत में हम देख पाते हैं कि लोककथा के माध्यम से जनसमाज ने कोसी नदी से सांस्कृतिक संबंध स्थापित किया। कोसी मइया की कथा घर-घर में गाई सुनी जाती है। “कोसिका महारानी नदी नहीं तिरहुत की कन्या। बंगाल में ब्याही गई। झगड़ालू सास-ननदों के अत्याचार सहते-सहते दुखी होकर लड़ पड़ी, खीझ के मारे सोरह मन के चमचमाते चाँदी के आभूषण चूर-चूर करके धूर कर डाले और चिटककर तिरहुत की ओर भागी। ननदों ने कुल्हाड़े वाले हजार दानव लेकर चलने वाली कुल्हाड़ी-आँधी और पहाड़ डुबाने वाले पहड़िया पानी पीछे लगा दिए। कोसी मइया जान छोड़कर भागी, बंगला जादू के जोर से आँधी-पानी ने पीछा पकड़ लिया। जहाँ-जहाँ कोसी भागी आँधी-पानी ने सब नष्ट कर डाला। इलाका उजाड़ हो गया। तब तक कोसी मइया की दुलारी बहिन दुलारी दाय ने एक दीया जलाकर जादू काट दिया। कोसी रुक गई।”[22] इन लोक कथाओं में जीवन का उल्लास और संघर्ष दोनों मौजूद हैं। विरह और करुणा के साथ मंगल की सृष्टि भी उपस्थित रहती है।
कहा जा सकता है कि लोक कथाएँ जीवन के सभी रंग अपने भीतर रखती हैं। बहुत सी लोक कथाओं में नदियों का जिक्र आता हैं। उन कथाओं में नदियों के कारण कथानक की गति में बदलाव भी देखा जाता है। लोरिक और मंजरी की कथा में इसी तरह का वर्णन मौजूद है, जहाँ सोन नद मुख्य भूमिका में दिखाई दे जाता है। यात्रावृत्तांत एक आँख गंगा एक आँख सोन में लोककथा सोननद के साथ जुड़ी लोरकहा का चित्रण लेखक करता है। अर्जुनदास केसरी सोन नद की यात्रा में गोठाना के साथ लोरिक की ससुराल का सम्बन्ध बताते हैं। वे लिखते हैं, “पानी जांघ तक, फिर सीना तक, उसके बाद कंठ तक आने लगा। डूब जाने का भय, इसलिए गाँव के रत्थी नाई यहाँ की घटना 'लोरिकी गाकर सुनाया करते थे जिसमें लोरिक की बारात के डूबने-उबरने, झीमल मल्लाह द्वारा लोरिक की बारात को नदी पार करने और फिर मोलागत राजा से लोहा लेकर मंजरी की बिदाई कराने का विस्तृत वर्णन सुन रखा था।”[23] गोठाना के लिए कहा जाता है कि यही वह अञ्चल है, जहाँ कथा-नायिका मंजरी ने जन्म लिया था और वीर लोरिक उसे ब्याहने गौरा से यहाँ सवा लाख बारातियों को लेकर आया था। राजा ओव्रागत से उसका भयंकर युद्ध हुआ था और लाशों से धरती पट गयी थी। इतना शोणित वहाँ था कि सोन खून की नदी बन गयी थी।
नदी के साथ समाज के अन्तःसंबंधों का विश्लेषण करने पर हम देखते हैं कि नदी किनारे के व्यक्ति, समाज, परिवार, रीति-रिवाज, धर्म, दर्शन, अध्यात्म, साहित्य, मिथक, पर्यावरण इत्यादि के साथ गहरा सम्बन्ध बना लेते हैं। इन सभी को नदियाँ किस प्रकार प्रभावित करती हैं और इनके भीतर किस प्रकार पैठ बनाती है, इसे लोकमन में देखा जा सकता है। मिथकों, लोकगीतों और लोक कथाओं में नदी की मौजूदगी के साथ समाज द्वारा नदियों के साथ व्यक्त की जाने वाली श्रद्धा, आस्था और विश्वास मुग्धकारी है। इस प्रकार हम देखते हैं कि नदियों पर केंद्रित यात्रावृत्तांतों में प्रयुक्त कथात्मक और मिथकीय प्रसंग भारत की नदियों के साथ यहाँ के निवासियों का अटूट संबंध व्यक्त करते हैं। ये पुरा कथाएं भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रतिनिधित्व करती हैं । इनके माध्यम से हम उन तत्त्वों को पहचान सकते हैं जो भारतीय संस्कृति का संबंध जल, जल स्रोत, जल संस्कृति, नदी और तीर्थों के साथ स्थापित करती है।
संदर्भ सूची -
[1] बद्री नारायण : लोक संस्कृति और इतिहास, लोक भारती प्रकाशन, नई दिल्ली, 2009, पृ. 87
[2] अमरनाथ : हिदी आलोचना की पारिभाषिक शब्दावली, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, चौथा संस्करण,
2016, पृ. 282
[3] उषा पुरी विद्यावाचस्पति : भारतीय मिथकों में प्रतीकात्मकता, सार्थक प्रकाशन, नई दिल्ली, 1997, पृ. 1
[4] राकेश तिवारी : सफर एक डोंगी में डगमग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 106
[5] विष्णु प्रभाकर : जमना-गंगा के नैहर में, सस्ता साहित्य मंडल, नई दिल्ली, 1964, पृ. 112
[6] अभय मिश्र एवं पंकज रामेंदु : दर दर गंगे, पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया प्रा. लि. गुड़गाँव, 2013, पृ. 172
[7] राकेश तिवारी : सफर एक डोंगी में डगमग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 165
[8] वही, पृ. 174
[9] अमृत लाल वेगड़ : तीरे-तीरे नर्मदा, मध्यप्रदेश हिंदी ग्रन्थ अकादमी, भोपाल, द्वितीय संस्करण, 2018, पृ. 53
[10] श्रीराम परिहार : संस्कृति सलिला नर्मदा, आदिवासी लोक कला एवं तुलसी साहित्य अकादमी मध्यप्रदेश
संस्कृति परिषद्, भोपाल, 2006, पृ. 24
[11] राकेश तिवारी : सफर एक डोंगी में डगमग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 141
[12] राजेश कुमार व्यास : नर्मदे हर, पुरोवाक्, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2018, पृ. 7
[13] सांवरमल सांगानेरिया : ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2015, पृ. 126
[14] राजेश कुमार व्यास : नर्मदे हर, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, 2018, पृ. 15
[15] राकेश तिवारी : सफर एक डोंगी में डगमग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 42
[16] वही, पृ. 83
[17] वही, पृ. 129
[18] वही, पृ. 101
[19] वही, पृ. 107
[20] सांवरमल सांगानेरिया : ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे, भारतीय ज्ञानपीठ, नई दिल्ली, 2015, पृ. 20
[21] सुदर्शन वशिष्ठ : हिमाचल प्रदेश की लोक कथाएँ, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, नई दिल्ली, दूसरा संस्करण, 2017,
भूमिका, पृ. 8
[22] राकेश तिवारी : सफर एक डोंगी में डगमग, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2014, पृ. 166
[23] अर्जुनदास केसरी एवं शेख जैनुल आब्दीन : एक आँख गंगा एक आँख सोन, लोकवार्ता शोध संस्थान,
राबर्ट्सगंज, सोनभद्र, 1999 पृ. 3
==================