मधुमती, अगस्त,2017 में प्रकाशित।
ईलोक चौपाल-2
ख्यातनाम कवि एवं आलोचक हेमंत शेष ने अपने रचनाकर्म से साहित्य एवं कला जगत् को सम्मोहित किया है। फेसबुक वाल पर उन्होंने लिखा कि कैसे रचता है कोई लेखक अपनी कृति? कविता, कहानी, उपन्यास..... ये सवाल पूछना अपने रचनाकार की सीमा से कुछ बाहर निकलकर खुद से एक तटस्थ ‘वैज्ञानिक’ किस्म की तटस्थ जिज्ञासा से जुडा प्रश्न पूछना है।.... हर शुरू होने से पहले, बहुत कुछ है अज्ञात, अपूर्वमेय, अँधेरे में डूबा... एक बहुत गहरी बावडी, जिसकी सीढियाँ किसी अज्ञात अनंत की ओर उतरती है.. क्या वहाँ जल है या सिर्फ सूखी खडखडाती निस्तब्धता... कोई नहीं जानता! रचना-प्रक्रिया को रेखांकित करते हुए साफगोई से वे लिखते हैं, ‘‘हर अच्छी रचना, लिखे जाने से पूर्व एक गहरी अपूर्वमेयता का लबादा ओढे रहती है... काले भारी कम्बल को हटा सकूँ तो आकृति, कोई रूपरेखा दिखे!’’ ‘साहित्य का सच और वैचारिक प्रतिबद्धता शीर्षक प्रसंग में हेमंत शेष की टिप्पणी विचारणीय है कि इस बात पर विचार किया जाना चाहिए कि साहित्य के साथ जोडे गए आदर्श-उसकी सम्प्रेषणीयता ने आखिर क्या खतरे पैदा किए हैं?... कहीं इसके अति आग्रह से हमारा साहित्य कहीं सतहीपन, सरलीकरण, सामान्यीकरण में बदलता जटिल और सूक्ष्मतर गुणों से विरत होता किसी अर्थ के भौंथरेपन, कोडीफिकेशन, थोथेपन के नजदीक तो नहीं पहुँच रहा है?
दिल्ली में बैठकर साहित्य रचना करने से कोई लेखक यदि भ्रम में है कि वह बडा बन गया है तो उसकी वास्तविकता से परिचय करवाते हुए अनूप शुक्ल ने व्यंग्यात्मक लहजे में टिप्पणी करते हुए लिखा-‘राजधानी दिल्ली में रहकर लिखने पढने का अपना सुख है.... दिल्ली केन्द्र है; सत्ता का भी, साहित्य का भी और साहित्य की सत्ता का भी।... प्रायः सारे महत्त्वपूर्ण लेखक दिल्ली में हैं.... साहित्य की वाचिक परम्परा के बडे-बडे स्तंभ दिल्ली में ही हैं.... वहाँ के लेखकों के वक्तव्यों की भी काफी मांग है। किसी अनर्गल विषय पर दिल्ली के अमहत्त्वपूर्ण लेखक का अप्रासंगिक मत भी महत्वपूर्ण मान लिया जाता है, जिस पर देशभर के छोटे-बडे साहित्यकार चर्चा करते हैं।.... अंत में वे सावधान करते हैं कि दिल्ली को देश की राजधानी बनाना तो ठीक, लेकिन उसे साहित्य की भी राजधानी बनाना साहित्य के भविष्य के साथ खिलवाड करना और साहित्य की समृद्धि को सीमित करना है। पुरानी कहावत है कि दुष्टों को बिखरने नहीं देना चाहिए और संत-विद्वानों को बिखेरकर रखना चाहिए, तभी मानवता का कल्याण संभव है; और शब्द-साहित्य का भी!
भारतीय सांस्कृति परम्पराओं; प्रतीकों का अपमान करना बुद्धिजीवियों की निशानी बना रहा है। राजेन्द्र रंजन चतुर्वेदी ने तथाकथित विचार समूहों को संकेत करते हुए लिखा कि जो यह सामझते हैं कि देश की प्राचीन-संस्कृति सामंतों और पुरोहितों की रचना है, वे बहुत घाटे में हैं। वे लोक की शक्ति की पहचान नहीं कर पाते। वे गंगा के पास जाकर भी केवल घाटों के देखकर ही लौट आये! गंगा के प्रवाह को नहीं जाना, वह निर्मल-धारा, जो प्रेम की सर्वोपरिता का अभिषेक करती है। उन्होंने अपने मन का सवाल रखते हुए वर्तमान साहित्य ‘जगत’ की दिशा पर भी प्रश्न खडा किया-मेरे मन में सवाल था कि कहीं ब्राह्मणवाद शब्द की आड लेकर भारत की समूची विद्या-परम्परा को, विद्या साधना, तप त्याग जैसे जीवन मूल्यों को नकारा तो नहीं जा रहा? भारत की संस्कृति, दर्शन, वेदपुराण-उपनिषद-साहित्य का तिरस्कार तो नहीं किया जा रहा?
आतंकी वारदातों के बीच अम्बिका दत्त चतुर्वेदी की अमरनाथ यात्रा रोमांचकारी रही। डल झील के गरीब नाविकों की मनः स्थिति का चित्रण करते हुए वे लिखते हैं-जब ये दीन (धर्म), राजनीति, आतंक के शिकंजे में लोभ, भय, आस्था और भ्रम की रस्सियों में जकडे कसमसाते होंगे, कैसी मुश्किल होती हेागी? जो रोज कुआँ खोदता और रोज पानी पीता है, उसके लिए एक तरफ तो रोजी रोटी, बच्चों की परवरिश के यथार्थ की हकीकत है, उससे जुडे सवाल हैं और दूसरी तरफ भ्रम, भय, आतंक, अंधविश्वास और लोभ के दाँव अपने विकराल पाश लिए खडे हैं.... लेकिन जीवन और कविता भी इन्हीं असंभव लगने वाले हालात के बीच गाया जाने वाला खुशबूदार उम्मीद का मीठा नगमा है जो हर बुरे से बुरे वक्त में, बुरे से बुरे इंसान के अन्दर बजता रहता है और जीवन को वापस लौटा लाने का काम करता है। हम उसी नगमे, उसी फूल, उसी खुशबू के लौट आने की दुआ करते हैं।
काठमांडू यात्रा के वृतान्त को साझा करते हुए सवाई सिंह शेखावत लिखते हैं कि नेपाल की यात्रा छोटे भाई के घर जाने जैसी है। भाषा, भूषा, मुद्रा, रीत-परम्पराएँ कुछ भी आडे नहीं आता। नेपाल के लोगों का धैर्यपूर्ण जीवन-व्यवहार भी बहुत मुतासिर करता है। सडक पर चलते हुए माला फेरने का आम रिवाज है। उसमें प्राचीन भारतीयता के साथ बुद्धत्व का असर भी साफ दिखता है। नेपाली कवि ‘सुमन पोखरेल’ की कविता ‘पेड’ का संदर्भ देकर जीवन की समग्रता को रेखांकित किया मैं देख रहा हूं पेड को/पेड टुकडों में नहीं जीता। जब तक जीता है, जिंदगी की संपूर्णता में/ अपने में समाहित कर जीता है/ धूप में धूप से संतुष्टि/बरसात में भीगने की खुशी। पेड की भूख अपने आकार से बडी कतई नहीं। जीने की दौड-धूप से परेशान मैं/दिल दिमाग और बदन से थका-माँदा मैं/उसकी छाया में लेटकर/उगती चाँदनी के साथ देखता हूँ उसे/और वह खडा है, सौम्य निडर और निश्ंचत!
कथा सम्राट प्रेमचंद को उनके जन्मदिन पर याद करते हुए पुनीत बिसारिया कहते हैं कि प्रेमचंद को पढना भारत की आत्मा को पढना है। उनके पात्र यहीं कहीं घूमते दिख जाएंगे। आदर्श और यथार्थ का ऐसा विरल संयोग अन्यत्र दुर्लभ है। उनके जाने के अस्सी साल बाद भी उनके पात्र आकर हमारी आँखों के सामने चुनौती देते प्रतीत होते हैं कि हो सके तो हमारी विपदा दूर करो। एक तरफ मंत्र, कफन, सद्गति, दो बैलों की कथा जैसे दुखियारे पात्र हैं तो दूसरी तरफ नमक का दारोगा, पंच परमेश्वर, ईदगाह के सच्चे निष्कलुष, निष्कलंक पात्र। कौन कह सकता है कि जालपा घीसू-माधव, सूरदास, बूढा, होरी, गोबर, मिस मालती, जुम्मन मियां, हल्कू आज के भारत में नहीं मिलेंगे। प्रेमचंद की जन्मभूमि ‘लमही’ को केन्द्र में रखकर भरत प्रसाद ने कविता ‘गाँव गाँव लमही’ साझा की-लमही नहीं है लमही में/नहीं है बनारस में/ नहीं है उत्तर प्रदेश में/ लमही के लिए / भारतवर्ष छोटा पड गया है/ लमही है तो कलम के सिपाहियों की उम्मीद/ अभी बाकी है/बाकी है पशुओं को हीरा-मोती कहने का सपना/उम्मीद है कि/अंतिम मनुष्य की मुक्ति की लडाई/फिर कोई प्रेमचंद लडेगा/वरना अब कौन कहेगा? धरती की फसलें, पानी-वानी से नहीं/किसी के खून, पसीने से लहलहाती है।
भाषायी दृष्टि से समृद्ध भारत में भाषा-विवाद सत्ता के गलियारे में पहुँच गया है। उषारानी राव ने इस संदर्भ में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा कि तेजी से बदलते संवदेशील दौर में जहाँ वैश्वीकरण विशाल संभावनाओं के नये द्वार खोलता जा रहा है, वहीं अनेक अवरोध भी। विकास उन्नति का सोपान है। चतुर्दिक विकास के द्वारा समाज असमानताओं से छुटकारा पाता है। स्थान, जलवायु एवं सभ्यता के प्रभावान्तर्गत भाषाओं की विविधता द्रष्टव्य है। अनेक भाषाओं से संपन्न उत्कृष्ट एवं समृद्ध साहित्य वाले देश में भाषाओं को समग्र स्थान देकर वैश्विक रूप से स्थापित करने के बजाय आज राजनीतिक स्वार्थ की कलुषता के कारण सरकार की नीतियाँ ऐसी बनती जा रहीं है कि हमारी भाषाओं को एक-दूसरे के सामने द्वन्द्वात्मक मुद्रा में खडी कर दिया गया है।
नवोदित रचनाकार विमलेश शर्मा ने आधुनिक समाज में स्त्रियों की दशा को बखूबी रेखांकित किया है- कंदील का बुझना हर जगह एक जैसा ही है... हर समाज की जाने कितनी कहानियाँ हैं... कितने पथरीले और तंग सफर हैं और जाने कितने अँधेरे कोने हैं जहाँ आँसुओं के सैलाब से मन की सीलन उघडती रहती है। जाने कितने धु*व अब भी हैं जो विषम हैं... स्त्री का मुखर होना, अपनी बात रखना... आखिर क्यों समाज को सालता है... प्रश्न सदियों से ज्यों का त्यों है.... अजीब बिडम्बना है, जिन प्रश्नों के उत्तर सबसे पहले खोजे जाने चाहिए थे, वही प्रश्न आज भी मुँह बायें खडे हैं।
रामकाव्य की दृष्टि से वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास कृत ‘रामचरित मानस’ अप्रतिम हैं। डॉ. राजेश श्रीवास्तव ने दोनों की तुलना करते हुए क्रमशः शास्त्र और लोक का पर्याय बनाया है। तुलसी जयन्ती पर वे लिखते हैं कि जो शास्त्र में छूट जाता है वह लोक में मिल जाता है। शास्त्र लिखित रूप में होने के कारण अपरिवर्तनशील होता है, किंचित कठोरता के साथ; किंतु लोक बहुत लचीला एवं परिवर्तनशील होता है। लोक जनसामान्य के निकट होता है। लोक को यह अधिकार भी होता है कि वह उसमें अपने अनुसार परिवर्तन करता चले। अपने आराध्य राम की आलोचना एक हिरणी के मुख से करवाना तुलसीदास का लोकाधिकार ही है- तुम जिन भय मानहुँ मृग जाए। केचन मृग ढूँढन ये आए’’ मानस का यही लचीलापन उसे लोक प्रसिद्धि देकर शास्त्र से भी श्रेष्ठ स्थान प्रदान करता है।
विस्थापन और आतंक का लोकधर्मी सौंदर्य अग्निशेखर की कविताओं में मिलता है। सुशील कुमार ने समीक्षा करते हुए लिखा, ‘‘अग्निशेखर की कविताओं में प्रकृति के बिम्ब विस्थापन की भावभूमि पर आकर जो रूप लेते हैं, वह दुःख, भय, त्रासदी और आशा के बीच के अंतर्द्वन्द्व को जिस काव्यात्मक सौष्ठव और मेधा के साथ प्रकट करते हैं, वह पाठक के मन में कई भावों-अनुभावों का एक मिश्रित हिलोर या कम्पन (मिक्सड वाइब्रेशन) पैदा करता है-‘‘छलनी-छलनी मेरे आकाश के ऊपर से/बह रही है/स्मृतियों की नदी/ओ मातृभूमि!/क्या इस समय हो रही है/मेरे गाँव में वर्षा?/ कविता-वर्षा।
हिन्दी सिनेमा में गीतों के बदलते रूप पर गौरीनाथ ने टिप्पणी की है, वे मुखर रूप से लिखते हैं कि सिनेमा में गीतों का चरित्र भीषण रूप से बदला है।... म्युनिक चैनलों पर लगातार चल रहे नए गीतों में शब्द, स्वर और संगीत का महत्व उतना नहीं रह गया है, जितना देह और दृश्यों का। मानो वह गीत एक साथ देह से गाया जा रहा हो, कपडों से गाया जा रहा हो, बाथ-टब, साबुन या शो-रूम की असंख्य लग्जरी ची*ाों के माध्यम से गाया जा रहा हो! कम समय में अधिकतम प्रमोशन और विज्ञापन इन गीत-दृश्यों का प्रमुख लक्ष्य बन गया है, तभी तो बाजार-वस्तुओं की भरमार और देह के कटावों का अधिकतम इस्तेमाल यहाँ दिखता है।...
युवा कवि की प्रतिमा और संभावनाओं को सम्मानित करने वाला भारत भूषण पुरस्कार अच्युतानंद मिश्र को दिए जाने के समाचार के बाद ई लोक में वाद-विवाद चल ही रहा था कि कृष्ण कल्पित द्वारा कवयित्री अनामिका और अच्युतानंद पर टिप्पणी फेसबुक वाल पर लगाई, तीव्र विरोध के बाद वह हटा ली गई, लेकिन घमासान जारी है। लीना मल्होत्रा लिखती हैं कि कृष्ण कल्पित कवि कैसे भी हों, उनकी सोच बहुत घटिया है। उनकी भाषा में सामंती दृष्टि और स्त्रियों के प्रति दुराग्रह साफ दिखता है। आशीष त्रिपाठी ने लिखा-साहित्य में ऐसा विकृत मर्दवादी आचरण असल में व्यक्तिगत कुंठा से ज्यादा सामंतवादी पितृसत्तात्मक मन की अभिव्यक्ति है। जो हिन्दी में अभी भी बहुत ज्यादा जगह घेरे हुए है। मनीषा कुलश्रेष्ठ की पीडा इन शब्दों में उजागर हुई, हिन्दी जगत स्त्रियों को मिलते सम्मान को हमेशा नीचता से लेता है। बहुत स्त्री विमर्श का शोर है हिन्दी जगत में, लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा जलील स्त्रियाँ होती रही हैं।... अब वक्त बदल चुका है। चरित्र, स्त्री लेखन की तुम्हारी परिभाषाओं पर तमाचा पड चुका है। तुम्हारी तय की गई पतनशीलता अब तुम्हारे गले की हड्डी है। अनेक साहित्यकारों ने उस टिप्पणी की निन्दा की है। इस विवाद में कुछ साहित्यकार कृष्णकल्पित के साथ भी आ जुटे हैं। देखते हैं यह घमासान कब तक चलता है। ?
शेष अगले अंक में...... 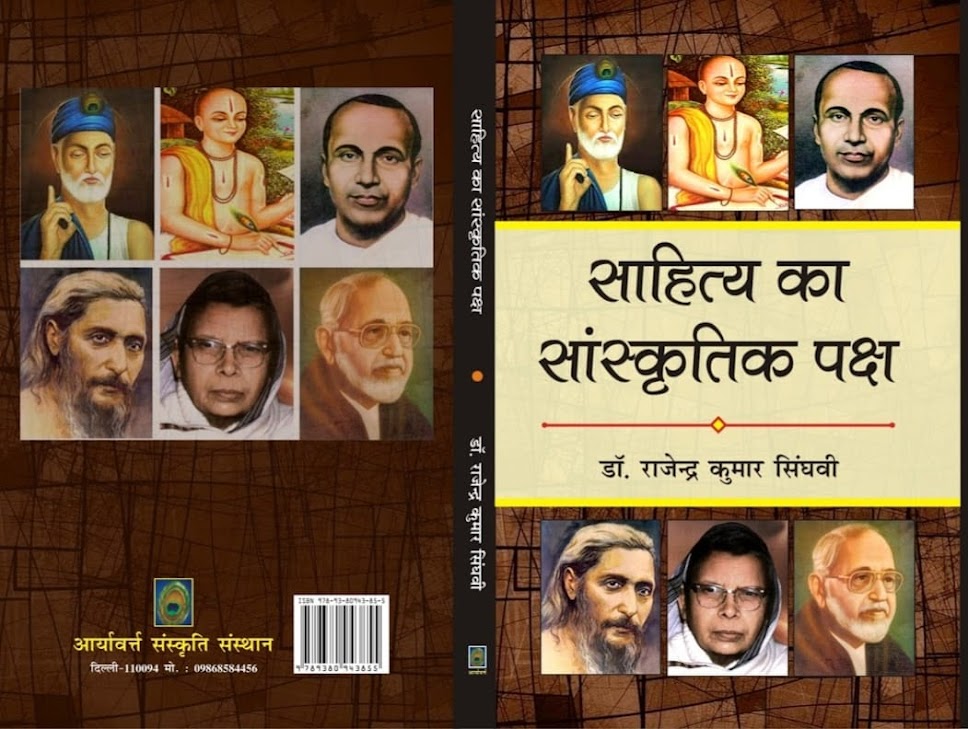
No comments:
Post a Comment