
नेमिचन्द्र जैन हिन्दी साहित्य में तार सप्तक के कवि, नाट्य आलोचना के जनक एवं ‘नटरंग’ प्रतिष्ठान के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। हिंदी की रंग-आलोचना के क्षेत्र में नेमिचंद जैन ऐसे पहले संपूर्ण आलोचक हुए, जिन्होंने उसे एक तार्किक व्यवस्था में बांधा। उन्होंने नाट्य सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप दिया तथा नाट्य चिंतन को विमर्श के केंद्र में लाने का प्रयत्न किया। नाट्य आलोचना पहली बार हिंदी में प्रामाणिक रूप से उभर कर सामने आया। इसके अतिरिक्त प्रमुख समाचार पत्र ‘स्टेट्समेन’, ‘दिनमान’ तथा ‘नव भारत टाइम्स’ के स्तंभ- लेखन से हिन्दी आलोचना के नए आयाम ‘रंग-विमर्श’ को उन्होंने जन्म दिया। नेमिजी ने नाट्य-विशेषज्ञ के रूप में इंग्लैंण्ड, सं.रा. अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, पौलेण्ड, यूगोस्लाविया और चेकोस्लाविया की यात्रा कर भारतीय साहित्य जगत् को गौरवान्वित किया।
नेमिचंद्र जी द्वारा रचित अधूरे साक्षात्कार(1966), जनांतिक(1981) पुस्तकों में औपन्यासिक आलोचना है, तो बदलते परिप्रेक्ष्य(1968)
में गहरे सांस्कृतिक-विमर्श का परिचय है।
रंगदर्शन(1993) में भारतीय नाट्य-परम्पका
विशद् विवेचन है। इस पुस्तक ने नाट्यालोचन की सैद्धांतिकी निर्मित की। ‘नटरंग’ पत्रिका के संपादकीय कौशल ने भारतीय रंगमंच को अभूतपूर्व ऊँचाई दी एवं ‘नटरंग’ प्रतिष्ठान की स्थापना के साथ नेमिचन्द्रजी ने नाट्य-अनुसंधान के द्वारा खोल
दिए। ‘मुक्तिबोध रचनावली’
तथा ‘मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक’ का संपादन करने
के साथ ‘मेरे साक्षात्कार’
पुस्तक में अपने संघर्षों और विचारों का
प्रामाणिक साक्ष्य भी प्रस्तुत किया।
हिन्दी आलोचना में उनका प्रवेश ‘अधूरे साक्षात्कार’ पुस्तक के साथ हुआ। इसमें उन्होंने ‘उसका बचपन’, ‘नदी के द्वीप’,
‘यह पथ बंधु था’, ‘बूंद और समुद्र’, ‘भूले बिसरे चित्र’, ‘मैला आँचल’,
‘झूठा-सच’, ‘जयवर्धन’, ‘चारुचन्द्र लेख’
आदि उपन्यासों की कलात्मकता का वर्णन किया।
उपन्यासों के मूल्यांकन उपरांत उनका असंतोष प्रकट हुआ। वे मानते थे कि हिन्दी
उपन्यासों ने अपना सम्पूर्ण स्तर अभी तक प्राप्त नहीं किया। ‘अधूरे साक्षात्कार’ के दूसरे संस्करण में जैन ने यह आशंका व्यक्त की है कि- “क्या हिन्दी उपन्यास अपना पूरा स्तर प्राप्त
किए बिना ही, अपनी पूरी
संभावनाओं को चरितार्थ किए बिना ही, अनिवार्य रूप से अकाल को प्राप्त होगा?”1 इस आशंका में
उनकी यह वेदना प्रकट हो रही है कि हिन्दी उपन्यास अपना अपेक्षित उत्कर्ष प्राप्त
नहीं कर सका।
नेमिचन्द्र जैन ने रंग-आलोचना में मौलिक कार्य किया और नई
जमीन तैयार की। 1965 में ‘नटरंग’ पत्रिका के प्रकाशन के दो वर्ष बाद 1967 में ‘रंग-दर्शन’
पुस्तक का प्रकाशन हुआ। इस पुस्तक में भारतीय
रंगमंच की विशेषताओं, प्रवृत्तियों,
अपेक्षाओं की विवेचना के उसकी सामाजिकता और
ऐतिहासिकता का गहन मूल्यांकन किया, यह पुस्तक अपनी
समग्रता के साथ हिन्दी नाट्य आलोचना की दृष्टि से धरोहर है। इसमें उन्होंने रंगकर्मी
की दृष्टि से रंगमंच की सार्थकता खोजी और यह मत प्रकट किया कि नाटक की सफलता रंग
मंच पर ही निर्भर करती है, जिसका हिन्दी
नाटकों में अभाव है। वे लिखते हैं- “जब तक हमारे देश का रंगकर्मी इन परिस्थितियों
और उनके इन अन्तर्विरोधों से साहसपूर्ण साक्षात्कार नहीं करता, तब तक वह एक प्रकार
के अपरिचित रिक्त में छटपटाता रहेगा और कोई सार्थकता प्राप्त नहीं कर सकेगा।“2
सन 1978 में ‘आधुनिक हिन्दी नाटक और रंगमंच’ पुस्तक का संपादन किया। इसकी भूमिका में भारतीय
रंगमंच के सूत्रों का सम्यक् विवेचन है। इसके अलावा 1993 में मोहन राकेश के नाटकों का संपादन ‘मोहन राकेश के संपूर्ण नाटक’ शीर्षक से किया, यह उनकी रंगमंच के प्रति अभिन्न रूचि का प्रमाण है। नाट्य
आलोचना की शृंखला में ‘भारतीय नाट्य
परम्परा’ पुस्तक भी चर्चा में रही
है। इसमें रंग-परम्परा और उसकी व्याख्या के साथ नेमिचन्द्र जी ने स्वीकार किया है
कि शहरों में बदलती जीवन-शैली व दुरूह जीवन से रंग-परम्परा का ह्रास हुआ है।
‘नटरंग’ पत्रिका को रंगमंच की अनिवार्य पत्रिका के रूप में स्थापित करने का श्रेय
नेमिचन्द्र जैन को है। भारतीय रंगमंच का इतिहास इस पत्रिका से सामने आया। भारतीय
रंगमंच का कोई पक्ष ऐसा नहीं रहा, जिसकी चर्चा
नटरंग में नहीं हुई हो। इसके माध्यम से रंगकर्मियों को मंचन योग्य नाटक उपलब्ध हुए,
जो हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषाओं में अनुदित
रूप में थे। कालान्तर में नेमिचन्द्रजी ने ‘नटरंग प्रतिष्ठान’ की स्थापना की। यह संस्थान दुर्लभ दस्तावेजों का ऐसा संग्रहालय है, जिसके बिना रंगकर्म के क्षेत्र में शोध नहीं हो
सकता। ज्योतिष जोशी के अनुसार-“ कहना न होगा कि नटरंग ने नेमिजी की चिंताओं का
निर्वाह कर हिन्दी सहित भारतीय रंगमंच को दिशा दी और अनेक स्टारों पर नाट्यालोचन
को स्थिर करने में बड़ी भूमिका निभाई।“3
‘दिनमान’ पत्रिका में नियमित स्तंभ लेखक के रूप में ‘दर्शकों’ व ‘भाषा’ संबंधी जो प्रश्न उठाए हैं, वे भविष्य की समीक्षा-दृष्टि में प्रतिमान हैं।
हिन्दी रंगमंच के प्रति उनकी चिंता भी विचारणीय है। उनकी नाट्य समीक्षा की प्रमुख
विशेषता यह है कि उनका ध्यान प्रस्तुतकर्ता पर न होकर प्रस्तुति पर रहता है,
जहाँ से निर्देशक अपने लिए सूत्र पा सकता है। नेमिजी की नाट्यालोचना व्यव्हार और जीवन व्यापार से बाहर कथित सैद्धांतिक अपेक्षाओं पर पर
लिखे जाने वाले नाटकों का न केवल निषेध करती है, वरन उसकी सार्थकता का भी प्रश्न उठाती है। 'रंगदर्शन' में वे लिखते हैं, "यह प्रायः कहा जाता है कि
समसामयिक सार्थकता के बिना नाटक की सफलता संभव नहीं। इस बात का यही अभिप्राय है कि
नाटक मूलतः समकालीन दर्शक के लिए ही रचा जाता है । एक काव्य की रचना भविष्य के लिए
चाहे हो सकती हो, पर नाटक आज के दर्शकों के निमित्त ही लिखा
जाना संभव है, क्योंकि आज के दर्शकों पर उसका प्रयोग और
प्रभाव परीक्षण अनिवार्य है ।“4
नेमिचन्द्र जी ने
साहित्यिक मूल्यों के साथ-साथ रंग-मूल्यों के प्रश्न भी उठाए। नाट्य-आलेख को
रंगमंच से काटकर परखने और विश्लेषित करने की परम्परा को अनुचित बताया। नाटक के पाठ
के भीतर छिपे हुए रंग-तत्त्वों की खोज के लिए नाट्य आलोचना के नए उपकरण तैयार किए।
उन्होंने नाटक रचे जाने की संपूर्ण प्रक्रिया के विविध आयामों को अपनी आलोचना
पद्धति में सम्मिलित किया। उसके लेखन, मंचन और दर्शकों तक पहुँचने को सूत्रबद्ध किया।
दृश्यकाव्य कहे जाने वाले नाटक की काव्यात्मक
संवेदना के साथ-साथ रंगकर्म के व्यवहार पक्ष को भी महत्त्व दिया नाटक की भाषा को
लेकर उनकी राय स्पष्ट थी कि उसमें भाव, विचार और चित्र तीनों को वहन करने का सामर्थ्य तो हो, पर फिर भी वह बोलचाल की भाषा से बहुत दूर न हो। ‘रंगकर्म की भाषा’ पुस्तक में वे लिखते हैं, “ रंगकला की अनन्य
श्रेष्ठता उसके समावेशी होने के कारण है, उसकी समग्रता के कारण है, उसके अंतर्गत सभी कलाओं के जुड़ सकने के कारण, सारे अभिव्यक्ति
माध्यमों को एक साथ जोड़ सकने के कारण है। उसमें काव्य सहित सभी कलाएँ एक साथ
मुखरित होती हैं, ध्वनित होती हैं, अभिव्यक्त होती
हैं और इस समग्र शक्ति से ही जो कुछ भी कहा जाना है, उसको कहती हैं हैं। यही रंगकला की श्रेष्ठता का स्रोत
है । उसमें से बाकी सब तत्त्वों को, विशेषकर श्रेष्ठ कार्यों को निकाल कर केवल अभिनेता के शरीर
की भाषा को ही बनाए रखना उसको बहुत कुछ 'एस्पोवरिश' करना है, दरिद्र बना देना है, दुर्बल करना है, उसकी बहुआयामी प्रभावशीलता को क्षीण करना है।“ 5
आलोचक के लिए नाटक की भाषा के साथ-साथ दृश्यबंध, दृश्यसज्जा और
रूपसज्जा की तकनीकी भाषिक के साथ अभिनेता की भाषा का भी नाटक और उसके सभी आयामों
का ज्ञान आवश्यक है। वे लिखते हैं, "रंगकला के आलोचक के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अगर उसको इतनी तमाम भाषाओं
की सृष्टि करनी है, उनको फिर से परिभाषित करनी है, तो वह कैसे करें? ऐसी कौनसी भाषा होगी, जो इन सरे भाषाओँ को
समेटकर रचना की पुनर्सृष्टि कर सकें? या कि जो सर्जनात्मक भाषा अभिनेता ने और उसके
सहयोगियों ने मिलकर अपनी-अपनी अलग-अलग भाषाओँ को समन्वित करके बनाई
है, जिसके आधार पर अभिनय का
प्रदर्शन होता है, पूरी प्रस्तुति रूपाकार लेती है, उसको फिर से शब्दों में, आलोचना
के रूप में प्रस्तुत कर सकें।“6
नेमिचन्द्र जैन के कविता समय के मध्य में ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ की स्थापना के साथ ही लेखकों के ध्रुवीय विभाजन की शुरूआत
हुई। उस आकर्षण के दौर में भी उन्होंने विवेक का परिचय दिया। 1943 में प्रकाशित ‘तारसप्तक’ के अपने
कवि-वक्तव्य में उन्होंने लिखा- “साहित्य में
प्रगतिशीलता में मेरा विश्वास है और उसके लिए एक सचेष्ट प्रयत्न का भी मैं
पक्षपाती हूँ। किन्तु कला की सच्ची प्रगतिशीलता कलाकार के व्यक्तित्व की सामाजिकता
में है, व्यक्तिहीनता में नहीं।”7
साहित्य की इस ध्रुवीय राजनीति में बुनियादी ईमानदारी से
उन्होंने समझौता नहीं किया। मार्क्सवादी-समाजवादी विचारधाराओं की संकीर्णता को समय
पर पहचान भी लिया। अज्ञेय के वैचारिक निबंधों की पुस्तक ‘हिन्दी साहित्य: एक आधुनिक परिदृश्य’ की समीक्षा करते हुए लिखते हैं कि वे इन विचारधाराओं का
नकारात्मक पक्ष ही देखते हैं। तो अज्ञेय क्या करें? नकारात्मक पक्ष को दरकिनार करके प्रगतिशील लेखक संघ में
भर्ती हो जाएँ। उन्होंने डॉ. नामवर सिंह की पुस्तक ‘कविता के नये प्रतिमान’ पर आक्षेप भी तटस्थ दृष्टि से किया। उन्होंने कहा कि भाई साहब, मार्क्सवादी रूझान
के बीच आपकी रूपावादी आलोचना दृष्टि की खिड़कियाँ भी खुली हुई हैं। इस अंतर्विरोध
को हल कर सकेंगे? ऐसा मुझे नहीं लगता। पक्षधर आलोचक महाशय की पक्षधरता कम से
कम किसी विशिष्ट जीवन-दृष्टि के स्तर पर तो नहीं है, बल्कि उसका अभाव ही कुछ आशंका जनक लगता है।
परम्परा के प्रति नेमिजी
की सजगता सदैव विद्यमान रही। उन्होंने परम्परा को कभी पुनरुत्थानवादी दृष्टि से
नहीं देखा। संवेदनशीलता के साथ परम्परा में नवाचारों का समर्थन किया। नेमिजी ने
समकालीन और आधुनिक नाट्य को परंपरा के सृजनशील अवयवों से जोड़ा है। उनकी मान्यता
है कि रंगकर्म को महज मनोरंजन बनाए रखना औपनिवेशिक मानसिकता का ही नतीजा है। वे
यहाँ संकेत करते हैं कि जैसे-जैसे और जिन जिन रंगकर्मियों ने इस मानसिकता से उबरने
की कोशिश की है, वैसे-वैसे उसकी 'सांस्कृतिक' और 'सृजनात्मक
सार्थकता' का एहसास उनमें
प्रबल हुआ है।
अपने प्राचीन
रंगकर्म के प्रति सकारात्मक दृष्टि रखने का आह्वान करते हुए उन्हें पता है कि
लोगों की नजर में यह 'पुनरुत्थानवादी' कार्य भी हो सकता है, खासकर उनकी नजर में नजर में जो परंपरा को सिर्फ हेय और
उच्छिष्ट दृष्टि से ही देखने के कायल हैं। वे रंग परंपरा में लिखते हैं, "इस संदर्भ में यह
बात भी महत्वपूर्ण है कि अपनी रंग परंपरा की तलाश का यह उद्देश्य अतीत की ओर लौटना
या किसी प्रकार का पुनरुत्थानवाद नहीं बल्कि, आज के जीवन के अनुभव को उसकी पूरी जटिलता और तीव्रता के साथ
उसके विविध रूपों में संप्रेषित करने के लिए रंग-परंपरा को आत्मसात करके उसका
सर्जनात्मक इस्तेमाल करना है।"8
परंपरा के सर्जनात्मक आविष्कार से उनका आशय है समकालीन, समसामयिक
आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने से है। वे मानते थे कि भारतीय रंगमंच को रचनात्मक
तरीके से समकालीन जीवन के अनुभवों से संचित करना चाहिए। जो कि पारम्परिक और
शास्त्रीय रंगमंच के प्रति गंभीरता से ही संभव है। ज्योतिष जोशी का नेमिचंद्र जैन
के बारे में मत है, “नाट्य चिंतन के क्षेत्र में उनका अवदान अप्रतिम है । पिछले
सौ-सवा सौ वर्षों की हिन्दी आलोचना, जिसका सिद्धांत और व्यवहार नाटकों की आलोचना
से विकसित हुआ, उसमें उनके जैसा आलोचक मिला, जिसने समग्रता के साथ हिन्दी रंगकर्म
की सैद्धांतिकी तो निर्मित की ही, उसकी आलोचना को भी विकसित करने का भगीरथ किया।“9 समग्रतः उनके अध्ययन की सक्रियता, कविता और आलोचना
की दुनिया के अनुशासन ने रंग समीक्षा और रंग चिंतन के क्षेत्र में शिखर तक
पहुँचाया और बीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारतीय रंग जगत को अपनी साधना और
चिंतन से समृद्ध किया।
सहायक ग्रंथ सूची-
1. हिन्दी का गद्य साहित्य, डॉ. रामचंद्र तिवारी, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी, सं.1999 पृष्ठ 104
2. रंग दर्शन, डॉ. नेमिचंद्र
जैन, अक्षर प्रकाशन, दिल्ली, सं.1967, पृष्ठ 11
3. नेमिचंद्र जैन, ज्योतिष
जोशी, विनिबंध, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, सं.2017, पृष्ठ 95
4 रंग दर्शन, डॉ. नेमिचंद्र
जैन, अक्षर प्रकाशन, दिल्ली, सं.1967, पृष्ठ 25
5 .रंगकर्म की भाषा, डॉ. नेमिचंद्र जैन, श्रीराम सेंटर, दिल्ली, सं.1999, पृष्ठ 33
6. रंगकर्म की भाषा, डॉ.
नेमिचंद्र जैन, श्रीराम सेंटर, दिल्ली, सं.1999, पृष्ठ 53
7. तारसप्तक, सं. अज्ञेय,
भारतीय ज्ञानपीठ, सं. 2002, भूमिका
8. रंग परम्परा, नेमिचंद्र
जैन, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, सं. 1996 , पृष्ठ 70
9. नेमिचंद्र जैन, ज्योतिष
जोशी, विनिबंध, साहित्य अकादेमी, नई दिल्ली, सं.2017, पृष्ठ 112
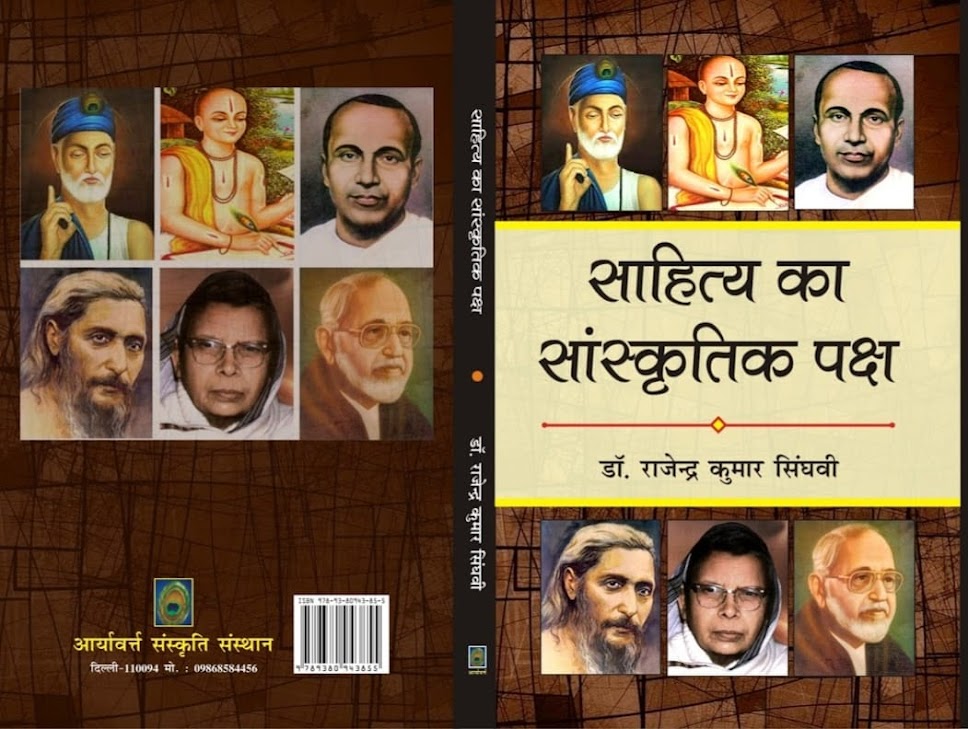
No comments:
Post a Comment