हिन्दी आलोचना : भाषा, प्रतिमान एवं विचारधारा
इक्कीसवीं सदी का हिन्दी साहित्य तीव्र गति से वैश्विक धरातल पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा है। साहित्य-रचना के मानक अब परम्परागत साँचे में नहीं है, उन पर तात्कालिकता का प्रभाव अधिक है। साहित्य अब भूमण्डलीकरण के साथ अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आलोचना भी साहित्यिक वातावरण के साथ कदमताल कर रही है, जहाँ किसी सैद्धान्तिक पैरामीटर से रचना का मूल्यांकन न करके रचनाशीलता की पहचान पर बल है। इस नवीन परिदृश्य में आलोचना का वर्तमान और भविष्य की दिशा का मूल्यांकन भाषा, विचारधारा एवं प्रतिमान की दृष्टि से किया जाना समीचीन होगा-
1. भाषा
भाषा विचार-विनिमय का साधन है, जिसके माध्यम से मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त करता है। इसके द्वारा ही वह सामाजिक संरचना का हेतु बनता है। इसलिए भाषायी संरचना को समझना आवश्यक है। भाषा स्वयमंव ऐसी प्रक्रिया है जहाँ परम्परा, परिवेश, व्यक्तित्व, विचार और अनुभव को सर्जनात्मक बनाती है। प्रसिद्ध आलोचक डॉ.रामस्वरूप चतुर्वेदी की मान्यता है कि उन्नीसवीं शती में विज्ञान के विकास ने परम्परागत धार्मिक आस्था को विघटित कर दिया था। बीसवीं शती में दो महायुद्धों ने मानवीय संवेदना को झकझोर कर रख दिया। परम्परागत सारे नैतिक-सांस्कृतिक मूल्य विघटित हो गए और व्यापक मानवतावाद की प्रतिष्ठा हुई।
वर्तमान परिदृश्य में रचना की भाषायी सर्जनशीलता का बारीकी से विश्लेषण किया जाने लगा है। नये आलोचकों की मान्यता है कि किसी विचार या अनुभव को दूसरे व्यक्ति में इस रूप में संक्रमित करना कि वहाँ उसका नया विकास संभव हो, सर्जन-प्रक्रिया का आरंभिक चरण है। इस अनुभव या विचार का संक्रमण भाषा से ही संभव है। इस हेतु भाषा और अनुभूति के अद्वैत को समझना होगा। अतः आने वाले समय में आलोचना में ‘रूप तत्त्व’ को प्रश्रय मिलता दिखाई दे रहा है। जहाँ रचना को भाषिक-संरचना के आलोक में विवेचित करने का प्रयास हो रहा है। उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद ने इस दृष्टि को और व्यापकता प्रदान की है। फलतः रचना की आलोचना में भाषा के विविध अंग- शब्द-चयन, छंद, ध्वनि-समूह, बिम्ब-विधान, प्रतीक-योजना, लय, कथन-भंगिमा, वाक्य-वक्रता, पद-विन्यास आदि के विश्लेषण पर ध्यान दिया जाने लगा है।
भाषा का स्वरूप भी आलोचना को नई धार दे रहा है। भूण्डलीकरण ने हिन्दी को वैश्विक स्वरूप प्रदान किया है। अब यह भारतीय उपमहाद्वीप के साथ मारीशस, इण्डोनेशिया, यूरोप एवं अन्य देशों में प्रवासी भारतीयों में गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। भारत में भी हिन्दी को सर्वग्राह्य मान्यता मिली है। फिल्म, टी.वी., बाजार, विज्ञापन आदि में हिन्दी का प्रचलन बढ़ गया है, जहाँ हिन्दी का शास्त्रीय रूप, तत्समनिष्ठता अथवा परिष्कृत रूप न रहकर संप्रेषणीय व्यावहारिक रूप प्रकट हुआ है। नवीन रचनाओं में नई हिन्दी का रूप दिखाई दे रहा है। आलोचक भी इसकी महत्ता को स्वीकार कर तदनुरूप मूल्यांकन कर रहा है।
उत्तर-आधुनिक चिंतन व भारतीय संवैधानिक मूल्यों के निरन्तर प्रसार से अस्मिताओं के आधार पर भाषायी-चिंतन आलोचनात्मक विमर्श के केन्द्र में आया है। स्त्री, दलित, आदिवासी, किसान आदि की सामान्य बोलचाल की शब्दावली को साहित्य में प्रश्रय मिलने लगा है, जिससे उनकी सभ्यता, परम्परा व अनुभूतिजन्य पीड़ा को अभिव्यक्ति मिल सके। आलोचना में विमर्श केन्द्रित मूल्यांकन में भाषा का मूल्यांकन भी संबंधित परिवेश के संदर्भ में किया जाने लगा है।
परम्परागत साहित्य में लोकभाषा को सदैव दूसरे दर्जे पर रखा गया, किन्तु अब लोक भाषा अपना स्वाभाविक आकार गढ़ने लगी है। आँचलिक भाषाओं का साहित्य अब रचनाशीलता में स्थान बना रहा है और परम्परागत प्रतिमानों को ध्वस्त कर रहा है। सुखद पहलू यह है कि आँचलिक भारतीय भाषाओं के साहित्यिक उदय से हिन्दी और समृद्ध हो रही है। लोकगीत, लोक नाट्य, लोक वाणी की स्वीकार्यता से स्वाभाविक प्रस्तुति हो रही है।
समकालीन साहित्य में एक तरफ लोक वृत्त उभर रहा है, वहीं दूसरी तरफ रचनाएँ वैश्विक फलक पर पाँव भी प्रसार रही है। दोनों की दिशा पृथक् होते हुए भी महत्त्व भी है। एक पक्ष अपने अस्तित्व को स्थापित कर हिन्दी को समृद्ध कर रहा है, तो दूसरा पक्ष हिन्दी को वैश्विक परिदृश्य में स्थापित कर रहा है। दोनों की शृंखला नई आलोचना का विवेच्य विषय है। आज के समय में भाषायी प्रतिमान निश्चित नहीं किए जा सकते, क्योंकि उसकी दीवारें ही गिर रही हैं।
रचना की इस भाषा के अनुरूप आलोचना की भाषा में परिवर्तन का आग्रह करते हुए नामवर सिंह लिखते हैं- “भाषा को जब तक हिन्दी आलोचना नहीं तोड़ेगी, तब तक वह एक ही जगह पर कवायद करती रहेगी। इसलिए रचनाकारों से हाथ जोड़कर मैं निवेदन करूँगा कि मित्रो, तुम लोगों ने तो अपनी भाषा तोड़ी है, हम आलोचकों को भी बताओ कि भाषा कैसे तोड़ी जाती है? जिस दिन यह भाषा तोड़कर हम नई भाषा बनाएंगे, आलोचना पढ़ने लायक होगी, अन्यथा यह चारों की या उनके गिरोहों की एक कूट भाषा बनेगी, जिसमें खग बोलेगा और खग ही सुनेगा।”
2. प्रतिमान
विगत दो दशकों से हमारे सामाजिक जीवन में भी व्यापक बदलाव आए हैं। वैश्विक समाज सूचना क्रांति से बहुत छोटा प्रतीत होने लगा है। परम्परागत विचार, प्रतिबद्धताएँ एवं मूल्य लगभग अप्रासंगिक होते गए व उन्मुक्त सोच की तरफ दुनिया बढ़ रही है। साहित्य भी इससे अलग नहीं है। आलोचना भी तात्कालिक समस्याओं के संदर्भ में होने लगी है, जिसे किसी घेरे में बन्द भी नहीं रखा जा सकता है। आज सोश्यल मीडिया पर हर व्यक्ति अपने विचार प्रकट करने के लिए स्वतंत्र है, अतः वहाँ साहित्यिक प्रतिमान स्थिर रहें, यह संभव भी नहीं है। देश-विदेश में घटित किसी भी घटना पर किसी रचना का जन्म और उस पर त्वरित प्रतिक्रियाओं से आलोचना के संदर्भ भी बदलते जा रहे हैं।
जहाँ तक आलोचना के प्रतिमानों की वस्तु-स्थिति का प्रश्न है, वे परम्परागत रूप में अब दिखाई नहीं दे रही है। आचार्य शुक्ल, राम विलास शर्मा, डॉ. नगेन्द्र अथवा आचार्य द्विवेदी की तरह उद्देश्यनिष्ठता एवं सैद्धांतिकी का स्वरूप नहीं दिखाई देता। विगत शताब्दी की आलोचनाओं में पहले उद्देश्य निर्धारित होता था, उसके बाद सिद्धान्त निर्मित किए जाते, फिर उन सिद्धांतों के आधार पर कृति की परख की जाती थी। इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर अनेक आलोचना प्रणालियों का जन्म हुआ, लेकिन विगत कुछ वर्षों से यह तकनीक भी अब स्वरूप बदल रही है। आलोचना में किसी निश्चित फलक का उपयोग दिखाई नहीं देता।
आलोचना की समकालीन परिस्थितियाँ बदलते हुए परिवेश के अनुरूप ही हैं। जहाँ ठहराव और अवकाश तो बिल्कुल भी नहीं है। अब सिद्धांतों की कसौटी पर कृति को कसने के स्थान पर सर्वप्रथम कृति के मूल कथ्य को ध्यान में रखकर सिद्धांत निर्मित किए जाते हैं, फिर एक सिरे से पुस्तक की व्याख्या या समीक्षा कर दी जाती है। सामाजिक-राजनैतिक परिस्थितियों को समझकर रचना की संपूर्णता को परखने की प्रवृत्ति अब लुप्त होती जा रही है। कतिपय आलोचनाएँ अपवाद हो सकती हैं, किन्तु यही सामान्य प्रवृत्ति दिखाई दे रही है।
आलोचना की मात्रा तो बहुत अधिक है, परन्तु उसके लेखन के प्रतिमान निश्चित नहीं हैं। रचना के तथ्यों का आलोचक वर्णन करके आगे बढ़ जाता है, जहाँ रचना की प्रशंसा तो है, परन्तु मूल्यांकन नहीं। यह कटु सत्य है कि आलोचना अब रचना केन्द्रित होने के स्थान पर रचनाकार केन्द्रित होने लगी है। आलोचक भी इसी भ्रम में हैं कि उसकी चर्चा से लेखक स्थापित हो रहे हैं और उपेक्षा से वे नगण्य, तो स्पष्टतः आलोचना के मूल्य ही विस्थापित हो रहे हैं।
एक प्रश्न उठता है कि क्या पुराने प्रतिमानों के आधार पर नई रचनाओं की समीक्षा संभव है? इस दृष्टि से तो सही उत्तर यही होगा कि पुराने प्रतिमानों के आलोक में अद्यतन रचना का मूल्यांकन संभव नहीं है। लेकिन रचना के बदलते स्वरूप के साथ आलोचना के नवीन प्रतिमान तय किए जाने अपेक्षित हैं, जो चिंता का विषय भी है। आज अनेक विमर्श केन्द्रित रचनाएँ सामने आ रही हैं, परन्तु नई आलोचना प्रणालियाँ विकसित नहीं होने से प्रतिमान भी स्थापित नहीं हो पा रहे हैं।
समकालीन रचनाओं का मूल्यांकन सम-सामयिक संदर्भों में ही किया जा सकता है और रचनाशीलता के समानांतर ही आलोचना के प्रतिमानों का निर्माण होता है। प्रत्येक समय की चुनौतियाँ होती है और उसके समाधान तात्कालिक रचनाओं में तलाशने का कार्य आलोचक का है। आलोचक ही अपनी प्रखर दृष्टि से पुराने प्रतिमानों को नया रूप दे सकता है और समय के अनुकूल प्रतिमान निर्मित भी कर सकता है। मैनेजर पांडेय ने इस संदर्भ में लिखा है- “हिन्दी में पाँच प्रकार की आलोचनाएँ प्रचलित हैं, पहली है अखबारी आलोचना, दूसरी पुस्तक समीक्षा, तीसरी अध्यापकीय आलोचना, चौथी आस्वादपरक आलोचना, जो पत्रिकाओं से लेकर व्याख्याओं तक में पायी जाती है और पाँचवीं है- पराआलोचना या साहित्य सिद्धांत। हिन्दी में जिसे साहित्य की मुख्यधारा कहा जाता है, उसमें साहित्य-सिद्धांत का पूरी तरह अकाल ही है। पहले उपनिवेशवाद के कारण और अब भूमण्डलीकरण के प्रभाव में, जैसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उधार से काम चलाने की हमारी आदत बन गई है, उसका विस्तार साहित्य की आलोचना में है और साहित्य-सिद्धांत में भी।”
हिन्दी आलोचना में आज सर्वाधिक आवश्यकता समकालीन रचनाशीलता की प्रवृत्तियों की पहचान कर आलोचना के प्रतिमान निर्मित किए जाने की है, ताकि आलोचना की भावी दिशा सही गंतव्य की ओर बढ़ सके। इससे भारतेन्दुकाल से जन्मी, शुक्ल काल में विकसित और शुक्लोत्तर काल में चरम तक पहुँची हिन्दी आलोचना वैश्विक साहित्यिक आलोचना के समकक्ष स्तर को प्राप्त कर सके। गंभीरता, अध्ययन-निष्ठता, पैनी दृष्टि और साहित्यिक वातावरण इस दृष्टि से निर्मित करना वर्तमान समय की प्रमुख आवश्यकता प्रतीत हो रही है।
3. विचारधारा
विचारधारा रचना तथा आलोचना की रीढ़ होती है, जिसके आधार पर उसकी महत्ता, उपयोगिता एवं प्रासंगिकता सिद्ध होती है। हिन्दी आलोचना अपने आरंभ से किसी न किसी आधार को लेकर चली है, चाहे वह सैद्धांतिक हो या व्यावहारिक; किसी वाद के सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में हो अथवा विमर्श केन्द्रित अवधारणाओं पर आधारित। यह क्रम बीसवीं सदी के अंतिम दशक तक किसी न किसी रूप में विधमान रहा। यहाँ तक कि आलोचक को भी किसी निश्चित पक्ष का विचारक मानकर निर्णय किया जाता रहा। नई सदी की आलोचना उत्तर-आधुनिक दौर में हैं, जहाँ विचारधाराओं से मुक्ति की बात कही जा रही है। यहाँ तक कि विचारधारा शब्द आलोचना में शत्रुता अथवा आतंक का प्रतीक समझा जाने लगा है।
समकालीन आलोचना में विचार की जगह सूचना ने ले ली है। रचना का मूल्यांकन सतही स्तर पर होने लगा है। कई बार तो आलोचना में मूल्यांकन कम विज्ञापन अधिक प्रतीत होने लगता है। सूचना के विनिमय में रचना में वर्णित घटनाओं की पृष्ठभूमि उभर नहीं पाती। इसी कारण आलोचक रचना के पक्ष अथवा विपक्ष में खड़ा होने के बजाय किसी सुरक्षित कोने की तलाश में रहता है। गंभीर आलोचना का स्थान परिचयात्मक आलोचना ने ले लिया है। विचार और इतिहास से विमुख होकर आलोचकों में समझौतावादी लेखन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है।
विचारधारा साहित्यिक कृति का आन्तरिक पक्ष है, जिससे उसका व्यक्तित्व प्रतिबिम्बित होता है। यह एक प्रकार का दृष्टिकोण भी है, जो समय और परिस्थिति के संघर्ष में जन्म लेता है। इसे लेखक की चेतना का आधार कहना समीचीन होगा। विचारधारा के अभाव में वह कृति के साथ कभी न्याय नहीं कर पाएगा। वैसे विचारधारा किसी न किसी रूप में रचना में विद्यमान रहती है, जिसका सही मूल्यांकन विचारधारा के अनुसार ही हो सकता है। लेकिन वैचारिक आग्रह की प्रबलता में लेखक को अन्य पक्ष के मतों का भी सम्मान करना चाहिए। वैचारिक आग्रह कहीं दुराग्रह के कारण अच्छी कृति का भी उपहास न उड़ाए, यह आवश्यक है। विचारधारा स्वयं की दृष्टि है, दूसरों पर थोपने का विषय नहीं।
एक समर्थ आलोचक वर्तमान की आँख से समकालीन रचना को देखता-समझता है, लेकिन अतीत की स्मृतियाँ वर्तमान को पुष्ट करती है। अतः प्रत्येक युग का दायित्व है कि वह कृति का मूल्यांकन इतिहास और समकाल के संदर्भों में करे। मैनेजर पाण्डेय लिखते हैं- “हिन्दी आलोचना का वर्तमान अगर संकटग्रस्त है तो इसके कारणों की पहचान होनी चाहिए। इस संकट का सबसे बड़ा कारण है- आलोचना में साहित्यिक को सामाजिक से अलग समझने और मानने की प्रवृत्ति। इसी प्रवृत्ति के कारण आलोचनात्मक व्यवहार के दौरान राजनीति, विचारधारा और सभ्यता के सवालों को साहित्य की आलोचना से बाहर कर दिया गया है।”
भूमण्डलीकरण में जो चुनौतियाँ साहित्यिक दृष्टि से उभर रही हैं उनमें प्रमुख हैं- मुक्त बाज़ारवाद, विकृत उपभोक्तावाद, राजनीतिक अधिनायकवाद, सांस्कृतिक परिष्करण, मूल्य-संक्रमण, हिंसक वर्चस्व, धार्मिक कट्टरता, भ्रष्ट आचरण, वैचारिक दुराग्रह आदि। समकालीन रचनाओं में इन बिन्दुओं पर बहुत कुछ लिखा भी जा रहा है। लेकिन आलोचना में अभी इन परिस्थितियों के कारकों की खोज नहीं हो पाई, जिससे रचनाएँ जन्म ले रही हैं। ऐसी स्थिति में सतही ‘पुस्तक समीक्षा’ ही आलोचना-मार्ग बनती जा रही है। हिन्दी आलोचना में अब पूर्ण गंभीरता नए परिवेश के अनुरूप आवश्यक है, जहाँ परम्परागत मूल्यों का आश्रय व विरासत के साथ नवीन प्रतिमानों का निर्धारण भी हों।
===========================
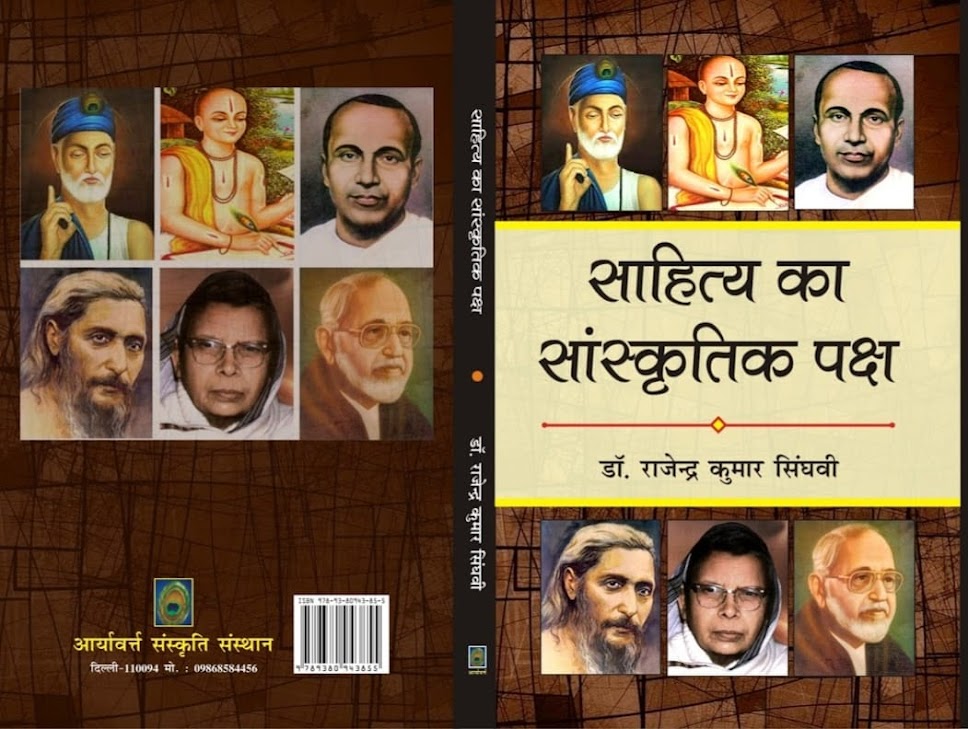
No comments:
Post a Comment