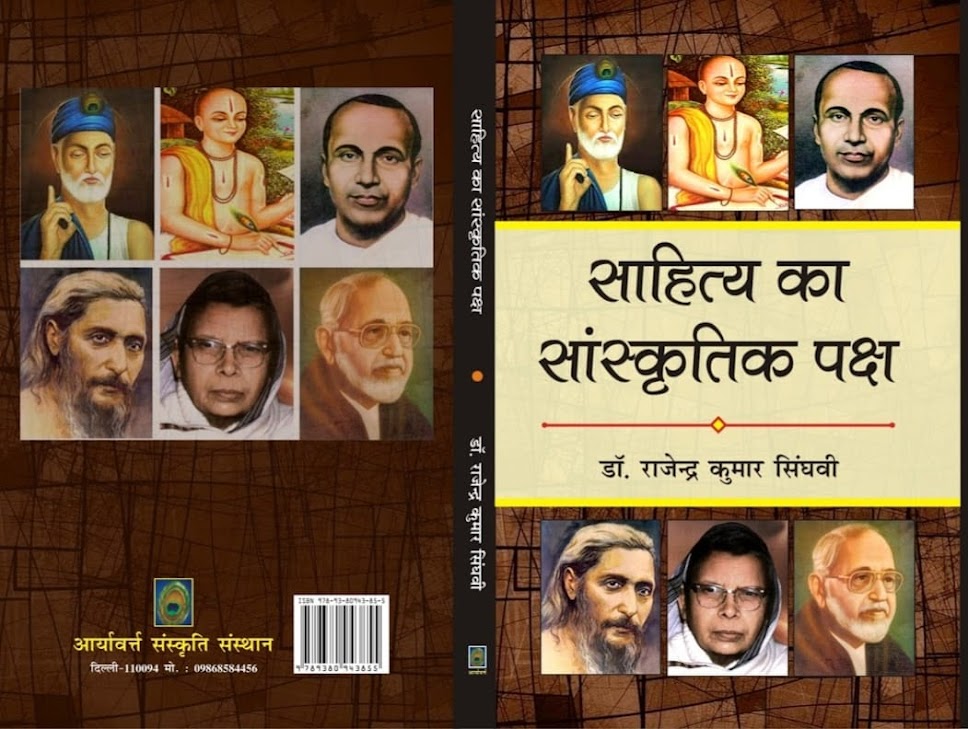हिन्दी का वैश्विक धरातल एवं विस्तार
मधुमती, सितंबर-२०२४ में प्रकाशित
भारत वर्तमान में विश्व-पटल पर सांस्कृतिक प्रभुत्त्व के साथ नेतृत्व की भूमिका में है। सामान्यतः जब कोई राष्ट्र अपने गौरव में वृद्धि करता है तो वैश्विक दृष्टि से उसकी प्रत्येक विरासत महत्त्वपूर्ण हो जाती है। परम्पराएँ, नागरिक दृष्टिकोण और भावी संभावनाओं के केन्द्र में ‘भाषा’ महत्त्वपूर्ण कारक बनकर उभरती है, क्योंकि अंततः यही संवाद का माध्यम भी है। वैश्वीकरण के दौर में संपूर्ण जीवन ‘वैश्विक ग्राम’ में सिमट कर रह गया है। भौगोलिक दूरियाँ, प्राकृतिक दुरुहता अथवा भाषायी अवरोध अब इतिहास की किवदन्तियाँ मात्र हैं। वर्तमान में राष्ट्रों की शक्तिमत्ता का आधार सैन्य शक्ति से अधिक आर्थिक संपन्नता है। ‘बाज़ार’ नई दुनिया के केन्द्र में है, इसी कारण चीन और भारत 21 वीं सदी के नेतृत्वकर्ता बन रहे हैं। इसमें भी भारत अपनी लोकतांत्रिक विशिष्टताओं, समृद्ध सांस्कृतिक परम्पराओं, उदारवादी-सर्वसमावेशी वृत्ति, प्रचुर प्राकृतिक सम्पदा, निपुण एवं प्रशिक्षित युवा-शक्ति के कारण दुनिया के आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। भारत की विश्व धरातल पर स्थापना में हिन्दी का योगदान अप्रतिम है।
वर्तमान में ‘हिन्दी’ को जो स्वरूप हमारे समक्ष विद्यमान है, उसका समय के साथ क्रमिक विकास का आधार है। हिन्दी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पालि, प्राकृत और अपभ्रंश के मार्ग से गुजरती हुई प्रारंभिक हिन्दी का रूप ग्रहण करती है। हिन्दी भाषा के विकास का विशुद्ध आरंभ ‘अपभ्रंश’ से माना जाता है, जो हमारे देश में 500 ई. से लेकर 1000 ई. के मध्य तक समृद्ध रूप में रही। अपभ्रंश से ही आधुनिक आर्य भाषाओं का भी विकास हुआ है, जिसमें शौरसेनी से पश्चिमी हिन्दी, राजस्थानी, गुजराती; अर्द्ध मागधी से पूर्वी हिन्दी; मागधी से बिहारी, उड़िया, बांग्ला, असमिया; खस से पहाड़ी; ब्राचड़ से सिंधी; पैशाची से पंजाबी; महाराष्ट्री से मराठी आदि अपभ्रंश के बाद हमारे देश में विविध भाषाओं का विकास होने लगा। इन प्रमुख भाषाओं में गुजराती, बांग्ला, उड़िया, असमिया, सिंधी, पंजाबी, मराठी के साथ हिन्दी भाषा समूह का विकास हुआ। वस्तुतः ‘हिन्दी’ शब्द भाषा विशेष का पर्याय नहीं, बल्कि भाषा-समूह का नाम है।
हिन्दी जिस भाषा समूह का नाम है, उसमें आज के हिन्दी प्रदेशों की पाँच प्रमुख उपभाषाएँ यथा-राजस्थानी हिन्दी, पश्चिमी हिन्दी, पूर्वी हिन्दी, बिहारी हिन्दी तथा पहाड़ी हिन्दी सम्मिलित हैं। इन पाँच उपभाषाओं की कुल 17 बोलियाँ इसकी संपत्ति है। पश्चिमी हिन्दी में खड़ी बोली, ब्रज, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली; पूर्वी हिन्दी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी; बिहारी हिन्दी में भोजपुरी, मैथिली, मगही; राजस्थानी हिन्दी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी; पहाड़ी हिन्दी में गढ़वाली, कुमाऊँनी आदि।
इन बोलियों की विशिष्टता है कि किसी निश्चित कालखंड में इन्होंने ‘हिन्दी’ का नेतृत्व किया है, जैसे- आदिकाल में राजस्थानी, भक्तिकाल में अवधी, ब्रज आदि, रीतिकाल में ब्रज तथा आधुनिक काल में खड़ी बोली आदि। सुखद पहलू यह है कि अन्य बोलियों ने सहजता से दूसरे का नेतृत्व स्वीकार किया। साथ ही समस्त बोलियों का फलना-फूलना जारी रहा। आज हिन्दी का विशाल साहित्य इन्हीं बोलियों में पल्लवित साहित्य का परिणाम है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक रहा कि स्वतंत्रता-संघर्ष में एकमात्र यही भाषा थी, जिसने पूरे भारत को एक सूत्र में बाँध दिया था।
हिन्दी के व्यापक प्रभाव का प्रमाण कुछ उदाहरणों से पुष्ट होता है। दिल्ली के सहायक रेजिडेंट ‘मेटकॉफ’ ने फोर्ट विलियम कॉलेज के ‘हिन्दुस्तानी’ के विभागाध्यक्ष जॉन गिलक्राइस्ट को एक पत्र लिखा- “भारत के जिस भाग में भी मुझे काम करना पड़ा है, कलकत्ता से लेकर लाहौर तक, कुमायूँ के पहाड़ों से नर्मदा तक, अफगानों, मराठों, राजपूतों, जाटों, सिक्खों और उन प्रदेशों के सभी कबीलों में जहाँ मैंने यात्रा की है, मैंने उस भाषा का आम व्यवहार देखा है, जिसकी शिक्षा आपने मुझे दी थी। मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक ........ इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत कर सकता हूँ कि मुझे हर जगह ऐसे लोग मिल जायेंगे जो हिन्दुस्तानी बोल लेते होंगे।" इसी तरह एनीबेसेंट ने कहा था, “हिन्दी जानने वाला संपूर्ण भारतवर्ष में मिल सकता है और भारत भर में यात्रा कर सकता है।”
एशियाटिक रिसर्च के लेखक एच.टी.कोलब्रुक ने लिखा- “जिस भाषा का व्यवहार भारत में प्रत्येक प्रांत के लोग करते हैं, जो पढ़े-लिखे तथा अनपढ़ दोनों की साधारण बोलचाल की भाषा है और जिसको प्रत्येक गाँव में थोड़े बहुत लोग अवश्य समझ लेते हैं, उसी का यथार्थ नाम हिन्दी है।” भारतीय भाषा विशेषज्ञ जार्ज ग्रियर्सन ने भी हिन्दी को भारत की सामान्य भाषा माना है। 1894 से 1927 तक ग्रियर्सन ने ‘लिग्विंस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया’ अर्थात् भारतीय भाषाओं के सर्वेक्षण का कार्य किया। ग्यारह बड़े-बड़े वोल्यूम में यह विशाल ग्रंथ भारत सरकार के केन्द्रीय प्रकाशन विभाग, कलकत्ता द्वारा प्रकाशित किया गया। पहला खंड बड़े महत्त्व का है, इसमें तुलनात्मक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण कार्य हुआ है। इस ग्रंथ की भूमिका में उन्होंने लिखा- “It is a comparative vocabulary of 168 selected words. In about 368 different languages and dialects. …… gramophone records are available in this country and in Paris.” इस भाग के अंत में ग्रियर्सन ने लिखा है कि भारत वस्तुतः विरोधी तत्त्वों की भूमि है और भाषाओं के संबंध में विचार करते समय तो यह तत्त्व और भी दृष्टिगोचर होते हैं। यहाँ अनेक ऐसी भाषाएँ हैं जिनके ध्वनि-संबंधी-नियमों के कारण केवल गौण और साधारण विचारों को ही प्रकट किया जा सकता है। वस्तुतः 179 भाषाओं और 544 बोलियों के इस देश में ध्वनिगत भिन्नताओं का होना कोई आश्चर्य नहीं है।
ग्रियर्सन ने इस खंड की भूमिका में देश का भाषिक प्रशिक्षण और उसकी क्षमता को भी स्वीकार किया है। इसमें भारतीय भाषाओं, उप-भाषाओं और बोलियों के उदाहरण भी संकलित हैं। तिब्बती, चीनी, बर्मी, ईरानी भाषा-परिवारों को सम्मिलित कर उन्होंने भारतीय आर्य भाषाओं के इतिहास का सबसे अधिक प्रामाणिक और क्रमबद्ध वर्णन किया। इस अथक परिश्रम का संकेत भूमिका में उल्लिखित इस टिप्पणी से मिल जाता है- “ Finish a work extending over thirty years, that after writing this Preface, the pen will be laid down …. I plead guilty to a vain boast whom I claim that what has been done in it for India has been done for no other country in the world.” ग्रियर्सन की यह मान्यता थी कि मैं इसको एक ऐसे सामग्री संग्रह के रूप में भेंट कर रहा हूँ जो नींव का काम दे सके। जिन लेखकों का नाम हम जानते तक नहीं, किन्तु वे जनता के हृदयों में जीवित वाणी बनकर बचे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जन की सत्य और सुन्दर भावना को प्रभावित किया।
भारतीय विचार-दृष्टि को समझने के लिए स्वाभाविक रूप से हिन्दी भाषा वैश्विक आकर्षण का केन्द्र बनी हैं। समग्र एवं निरपेक्ष दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि हिंदी भौगोलिक आधार पर विश्व-भाषा है, क्योंकि इसके बोलने समझने वाले संसार के सब महाद्वीपों में फैले हैं। नवीनतम सर्वेक्षण अनुसार इसकी संख्या विश्व में मंदारिन के बाद दूसरे स्थान पर है। विश्व के 132 देशों में जा बसे भारतीय मूल के लगभग दो करोड़ लोग हिंदी माध्यम से ही अपना कार्य निष्पादित करते हैं। देखा जाए तो एशियाई संस्कृति में अपनी विशिष्ट भूमिका के कारण हिंदी एशियाई भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी का किसी देशी या विदेशी भाषा से कोई विरोध नहीं रहा है। अनेक भाषाओं के शब्द हिंदी में बन गए हैं। यही कारण है कि आज हिंदी का शब्दकोश विश्व का सबसे बड़ा भाषिक शब्दकोश माना जाता है।
हिंदी स्वयं के भीतर एक अंतर्राष्ट्रीय जगत समाहित है, जिसमें आर्य, द्रविड़, अंग्रजी, स्पेनी, पुर्तगाली, जर्मन, फ्रेंच, जापानी, चीनी, फारसी, अरबी अदि सारे संसार की भाषाओं के शब्द समाहित है, जो अंतरराष्ट्रीय मैत्री और वसुदेव कुटुंबकम वाली प्रवृत्ति को उजागर करती है। हिंदी में अब अनुवाद और साहित्य लेखन भी बढ़ रहा है। गुणवत्ता की दृष्टि से इसकी वैश्विक स्वीकार्यता बढ़ रही है। प्रवासी भारतीय अपने अनेक कार्यक्रमों से हिंदी को जीवंत बनाए हुए हैं। इंटरनेट पर सर्वाधिक लोकप्रिय भाषाओं में हिंदी का अपना स्थान है। देश विदेश से प्रकाशित होने वाले पत्र-पत्रिकाएँ हिंदी को विश्व भाषा बनाने में मदद कर रहे हैं। भारतीय दूरदर्शन और आकाशवाणी और उसके साथ अनेक चैनलों ने हिंदी का प्रचार विश्वव्यापी करने में मदद की है। हिंदी की व्यापकता के कारण दुनिया के 175 देशों में हिंदी के शिक्षण और प्रशिक्षण के अनेक माध्यम केंद्र बन गए हैं। लगभग 180 विश्वविद्यालयों में हिंदी का अध्यापन हो रहा है और दिनों-दिन इसका वर्चस्व बढ़ता जा रहा है। एनसाइक्लोपीडिया के अनुसार मंदारिन के बाद सबसे बड़ी भाषा हिंदी है।
आज हिंदी 12 से अधिक देशों में बहुसंख्यक समाज की मुख्य भाषा है। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, नेपाल, मॉरीशस, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, यमन, युगांडा में भारतीयों की संख्या 2 करोड़ है। फिजी, गुयाना, सुरीनाम, टोबेगो, त्रिनिडाड तथा अरब अमीरात में भी अल्पसंख्यक भाषा के रूप में संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। भारत से बाहर जिन देशों में हिंदी का बोलने,लिखने, पढ़ने तथा अध्ययन-अध्यापन की दृष्टि से प्रयोग होता है, उन्हें हम चार वर्गों में बाँट सकते हैं-
1. जहाँ भारतीय मूल के लोग अधिक संख्या में रहते हैं, जैसे-पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका और मालदीव।
2.भारतीय संस्कृति से प्रभावित दक्षिण पूर्वी एशियाई देश, जैसे-इंडोनेशिया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, मंगोलिया, कोरिया, तथा जापान।
3. जहाँ हिंदी को विश्व के आधुनिक भाषा के रूप में पढ़ाया जाता है, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा और यूरोप के देश।
4. अरब और अन्य इस्लामी देश, जैसे संयुक्त अरब अमीरात, अफगानिस्तान, कतर, मिस्र, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान आदि।
जहाँ तक विश्व भाषा के स्तर को प्राप्त करने का प्रश्न है, तो उसके कुछ निश्चित प्रतिमान हैं। यथा-विश्व के अधिकांश भू-भाग पर भाषा का प्रयोग, साहित्य-सृजन की सुदीर्घ परम्परा, विपुल शब्द-संपदा, विज्ञान-तकनीक एवं संचार के क्षेत्र में व्यवहार, आर्थिक-विनिमय का माध्यम, वैज्ञानिक लिपि एवं मानक व्याकरण, अनुवाद की सुविधा, उच्च कोटि की पारिभाषिक शब्दावली एवं स्थानीय आग्रहों से मुक्त होना आदि। इन प्रतिमानों के आलोक में हिन्दी की विशिष्टताओं और सामर्थ्य का मूल्यांकन वर्तमान संदर्भों में समीचीन प्रतीत होता है।
भाषा के प्रयोग की दृष्टि से अवलोकन करें तो ज्ञात होता है कि आज हिन्दी का प्रयोग विश्व के सभी महाद्वीपों में प्रयोग हो रहा है। डॉ. करुणा शंकर उपाध्याय द्वारा लिखित पुस्तक ‘हिन्दी का विश्व सन्दर्भ’ में आधिकारिक तत्थ्यों के साथ स्पष्ट किया गया है कि लगभग 140 देशों में हिन्दी का प्रचलन न्यून या अधिक मात्रा में है। सन् 1999 में टोकियो विश्वविद्यालय के प्रो. होजुमि तनाका ने ‘मशीन ट्रान्सलेशन समिट’ में भाषायी आँकड़े पेश करते हुए कहा कि विश्वभर में चीनी भाषा बोलने वालों का स्थान प्रथम, हिन्दी का द्वितीय है और अंग्रेजी तीसरे क्रमांक पर पहुँच गई है। डॉ. जयन्तीप्रसाद नौटियाल ने ‘भाषा शोध अध्ययन-2005’ के आधार पर हिन्दी जानने वालों की संख्या एक अरब से अधिक बताई है। आज भारतीय नागरिक दुनिया के अधिकांश देशों में निवास कर रहे हैं और हिन्दी का व्यापक स्तर पर प्रयोग भी करते हैं, अतः यह माना जा सकता है कि अंग्रेजी के पश्चात् हिन्दी अधिकांश भू-भाग पर बोली अथवा समझी जाने वाली भाषा है।
हिन्दी में साहित्य-सृजन परम्परा एक हजार वर्ष से भी पूर्व की है। आठवीं शताब्दी से निरन्तर हिन्दी भाषा गतिमान है। पृथ्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरित मानस, कामायनी जैसे महाकाव्य अन्य भाषाओं में नहीं हैं। संस्कृत के बाद सर्वाधिक काव्य हिन्दी में ही रचा गया। हिन्दी का विपुल साहित्य भारत के अधिकांश भू-भाग पर अनेक बोलियों में विद्यमान है, लोक-साहित्य व धार्मिक साहित्य की अलग संपदा है और सबसे महत्त्वपूर्ण यह महान् सनातन संस्कृति की संवाहक भाषा है, जिससे दुनिया सदैव चमत्कृत रही है। उन्नीसवीं शती के पश्चात् आधुनिक गद्य विधाओं में रचित साहित्य दुनिया की किसी भी समृद्ध भाषा के समकक्ष माना जा सकता है। साथ ही दिनों-दिन हिन्दी का फलक विस्तारित हो रहा है, जो इसकी महत्ता को प्रमाणित करता है।
शब्द-संपदा की दृष्टि से हिन्दी में लगभग पच्चीस लाख शब्द प्रचलन में हैं। ये शब्द संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश परम्परा से विकसित, आँचलिक बोलियों में व्यवहृत, उपसर्ग-प्रत्यय, संधि-समास से निर्मित हैं, जिसका सुनिश्चित वैज्ञानिक आधार है। साथ ही विदेशी शब्दावली के अनेक शब्द जो व्यावहारिक रूप से प्रचलन में है, उनमें अंग्रेजी, फारसी, अरबी, पुर्तगाली, स्पेनिश, फ्रेंच आदि भाषाओं से गृहीत भी हैं। यह गुण हिन्दी की उदारता को रेखांकित करता है। विश्व की सबसे बड़ी कृषि विषयक शब्दावली हिन्दी के पास है, जो वैश्विक धरोहर है। दूसरी भाषाओं के साथ तादात्म्य स्थापित करने में हिन्दी की भाषिक संरचना लोकतांत्रिक है। इसकी वाक्य-संरचना में आसानी से दुनिया की किसी भी भाषा का शब्द समायोजित होकर अर्थ प्रकट कर देता है। यह विशिष्टता हिन्दी विशालता का प्रमाण है।
हिन्दी की लिपि-देवनागरी की वैज्ञानिकता सर्वमान्य है। लिपि की संरचना अनेक मानक स्तरों से परिष्कृत हुई है। यह उच्चारण पर आधारित है, जो उच्चारण-अवयवों के वैज्ञानिक क्रम- कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ आदि से निःसृत हैं। प्रत्येक ध्वनि का उच्चारण स्थल निर्धारित है और लेखन में विभ्रम की आशंकाओं से विमुक्त है। अनुच्चरित वर्णों का अभाव, द्विध्वनियों का प्रयोग, वर्णों की बनावट में जटिलता आदि कमियों से बहुत दूर है। पिछले कई दशकों से देवनागरी लिपि को आधुनिक ढंग से मानक रूप में स्थिर किया है, जिससे कम्प्यूटर, मोबाइल आदि यंत्रों पर सहज रूप से प्रयुक्त होने लगी है। स्वर-व्यंजन एवं वर्णमाला का वैज्ञानिक स्वरूप के अतिरिक्त केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा हिन्दी वर्तनी का मानकीकरण भी किया गया, जो इसकी वैश्विक ग्राह्यता के लिए महत्त्वपूर्ण कदम है।
हिन्दी में पिछले कई वर्षों से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विषयक उत्तम कोटि की पुस्तकों का अभाव था, लेकिन नई सदी में अनेक विश्वविद्यालय, केन्द्रीय संस्थाओं आदि ने इस दिशा में विशेष कार्य किया। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा मानक पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण किया, ताकि लेखन में एकरूपता रहे। आज संचार के क्षेत्र में तेजी से हिन्दी शब्दावली का प्रयोग बढ़ रहा है। यहाँ तक कि उच्चारण के आधार पर यंत्रों पर मुद्रण हिन्दी के प्रसार का लक्षण है। अभियांत्रिकी एवं चिकित्सा के क्षेत्र में हिन्दी का प्रयोग निरन्तर जारी है, अच्छा साहित्य निरन्तर प्रकाशित हो रहा है। निकट भविष्य में यह अभाव भी नहीं रहेगा, ऐसी आशा की जा सकती है।
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक संदर्भों, आर्थिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक विनिमय के क्षेत्र में हिन्दी ने भारतीय उपमहाद्वीप का नेतृत्व किया है। अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भारतीय नेताओं ने हिन्दी को समय-समय पर केन्द्र में रखा और संयुक्त राष्ट्र संघ में अब यह धारणा बनी है कि हिन्दी दुनिया की एक महत्त्वपूर्ण भाषा है। आर्थिक उन्नति की दृष्टि से भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, दुनिया के लिए एक करोड़ से अधिक का बाजार है और अपने उत्पाद के प्रचार के लिए हिन्दी भाषा उसके आर्थिक लाभ की कुंजी है, अतः विज्ञापन से लेकर आर्थिक जगत की समस्त गतिविधियों में हिन्दी को समुचित दर्जा मिला है। टेलीविजन, कम्प्यूटर, मोबाइल एवं मीडिया में हिन्दी की लोकप्रियता भविष्य के लिए अच्छे संकेत प्रदान करती है। गूगल, माइक्रोसोफ्ट एवं अन्य कंपनियों ने हिन्दी के व्यापक जनाधार को देखते हुए अनेक सॉफ्टवेयर हिन्दी की दृष्टि से तैयार किए, परिणाम स्वरूप इंटरनेट पर हिन्दी तेजी से फैल रही है।
वैश्विक स्तर पर किसी भाषा के स्तर निर्धारण में उसकी वैज्ञानिकता एवं मानकता का आधार महत्त्वपूर्ण होता है। इस दृष्टि से हिन्दी का मानक व्याकरण है। शब्द रचना की दृष्टि से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय आदि का वैज्ञानिक विवेचन है। वाक्य संरचना के निश्चित नियम है, शब्द-शिल्प प्रक्रिया का विवेचन किया गया है, साथ ही व्याकरणिक कोटियों की विशद् विवेचना की गई है। मानकता के कारण ही कम्प्यूटर आदि के लिए यह अनुकूल बन गई है। अनुवाद के लिए अच्छे सॉफ्टवेयर तैयार हो गए हैं और भाषा को समझने के लिए यह मानक व्याकरण पर्याप्त दिशा प्रदान करता है।
हिन्दी की लोकप्रियता जहाँ भारतीय उपमहाद्वीप के देश- नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश आदि में है, वहीं संपूर्ण भारत में यह प्रमुख संपर्क भाषा भी है। सुदूर इण्डोनेशिया, सूरीनाम, मलेशिया, मारीशस, सुमात्रा, जावा, बाली आदि देशों में बहुतायत में बोली जाती है। यूरोप एवं अमेरिका-कनाड़ा में हिन्दी भाषियों की तेजी से अभिवृद्धि हो रही है। मध्य एशिया में इसका सांस्कृतिक प्रभाव रहा है तो द. अफ्रीका आदि में राजनीतिक साहचर्य से यह समान रूप से लोकप्रिय हैं। यूनेस्को के अनेक कार्यक्रम हिन्दी में हैं। विश्व के अनेक क्षेत्र- मारीशस, सूरीनाम, लंदन, त्रिनिदाद, न्यूयार्क आदि में विश्व हिन्दी सम्मेलन सफलता पूर्वक आयोजित हो चुके हैं। इसी तरह भारतीय- सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा सामाजिक-सांस्कृतिक दृष्टि से हिन्दी को वैश्विक गरिमा प्रदान करने का प्रयास जारी है। महात्मा गांधी हिन्दी विश्वविद्यालय, वर्धा तथा अटल बिहारी वाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल की स्थापना भी इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। विश्व हिन्दी सम्मलेन जैसे आयोजन के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषा में हिन्दी को स्थान दिलाने का प्रयास जारी है।
अतः समग्र विवेचन उपरान्त यह स्पष्टतः कहा जा सकता है कि भाषायी संरचना शब्द-संपदा, मानकता, लिपि की वैज्ञानिकता, साहित्यिक उच्चता, सांस्कृतिक विशिष्टता, व्यापक विस्तार की दृष्टि से हिन्दी अपना एकाधिकार प्रमाणित कर चुकी है, जहाँ उसे वैश्विक भाषा का स्तर मिल सकता है। संयक्त राष्ट्र संघ की आधिकारिक भाषा अधिसूचित करने के अपने नियम हो सकते हैं, परन्तु स्वीकार्यता और भाषाई प्रतिमानों की दृष्टि से हिन्दी का धरातल अब विस्तृत हो चुका है। जिसकी उपेक्षा करना आने वाले समय में संभव नहीं होगा।
==========================================================